यह लेख अनुच्छेद 29 (Article 29) का यथारूप संकलन है। आप इसका हिन्दी और इंग्लिश दोनों अनुवाद पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें। इसकी व्याख्या इंग्लिश में भी उपलब्ध है, इसके लिए आप नीचे दिए गए लिंक का प्रयोग करें;
अपील - Bell आइकॉन पर क्लिक करके हमारे नोटिफ़िकेशन सर्विस को Allow कर दें ताकि आपको हरेक नए लेख की सूचना आसानी से प्राप्त हो जाए। साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ जाएँ और नवीनतम विचार-विमर्श का हिस्सा बनें;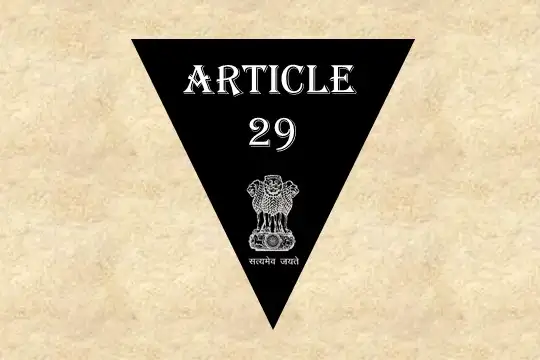
| 📌 Join YouTube | 📌 Join FB Group |
| 📌 Join Telegram | 📌 Like FB Page |
| 📖 Read in English |
📜 अनुच्छेद 29 (Article 29)
| 29. अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण – (1) भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। (2) राज्य द्वारा पोषित या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। |
| 29. Protection of interests of minorities. — (1) Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. (2) No citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the State or receiving aid out of State funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them. |
🔍 Article 29 Explanation in Hindi
संस्कृति, किसी भी सभ्यता का एक मूल तत्व होता है। ये लोगों के एक विशेष समूह की उन विशेषताओं, समूहिक व्यवहार और ज्ञान को बताता है, जिसमें भाषा, धर्म, भोजन, सामाजिक आदतें, संगीत और कला, रीति-रिवाज, परंपरा आदि शामिल होते हैं। और शिक्षा इन्ही सारी चीजों को सीखने, सिखाने एवं उसे आगे हस्तांतरित करने की एक प्रक्रिया है।
भारत एक सांस्कृतिक विविधता वाला देश है जहां ढ़ेरों अलग-अलग संस्कृतियाँ एक साथ अपनी संस्कृति को बनाए रखते हुए निवास करती है।
ऐसा इसीलिए संभव हो पाता है क्योंकि हमारा संविधान विविधता का सम्मान करती है और सभी को अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देती है (खासकर के अल्पसंख्यकों को जिसकी संस्कृतियों के लुप्त हो जाने का डर सबसे ज्यादा होता है)।
‘संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (Cultural and Educational Rights)‘ में कुल दो अनुच्छेद आते हैं (जिसे कि आप नीचे चार्ट में देख सकते हैं) इस लेख में हम इसी का पहला अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 29 (Article 29) को समझने वाले हैं।
| संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार↗️ |
|---|
| ⚫ अनुच्छेद 29 – अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण (Protection of interests of minorities) ⚫ अनुच्छेद 30 – शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उसका प्रबंधन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार (Right of minority to set up and manage educational institutions) |
| अनुच्छेद 29 – अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण
अल्पसंख्यक (Minority) कौन है?
संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं दी गई है। इस शब्द के साधारण अर्थ में इसका तात्पर्य है कोई भी ऐसा समुदाय जो राज्य की जनसंख्या के पचास प्रतिशत से कम है।
कोई समुदाय अल्पसंख्यक है या नहीं यह आपेक्षित विधान के प्रति निर्देश से सुनिश्चित किया जाएगा। भाषिक अल्पसंख्यक होने के लिए उस समुदाय की अपनी बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, भले ही लिपि न हो।
संविधान लागू होने के बाद अगर कोई संस्था अल्पसंख्यकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है तो ऐसे में अल्पसंख्यक भारत में निवासी व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन अगर संविधान लागू होने के पूर्व ही किसी अनिवासी व्यक्ति द्वारा कोई संस्था भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के फायदे के लिए स्थापित की गई है तो उसे इस अनुच्छेद का संरक्षण मिल सकता है।
अनुच्छेद 29 के दो खंड है, जिसकी व्याख्या नीचे की गई है।
अनुच्छेद 29(1) भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।
इस खंड का अर्थ ये है कि अगर कोई अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखना चाहते हैं तो राज्य उन पर कोई दूसरी संस्कृति अधिरोपित नहीं करेगा।
अगर कोई विधि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया जाता है जिसका विस्तार उस समस्त राज्यक्षेत्र में है। वहाँ उस पूरे राज्य की जनसंख्या के प्रति निर्देश से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अल्पसंख्यक कौन है।
याद रखें, भाषा को बनाए रखने के अधिकार में उस भाषा के संरक्षण के लिए आंदोलन चलाने का भी अधिकार शामिल है। और यह अधिकार राजनैतिक भी हो सकता है।
खंड (1) द्वारा प्रदत अधिकार आत्यंतिक (Absolute) है। अनुच्छेद 19(1) में उल्लिखित अधिकारों के समान इस पर युक्तियुक्त निर्बंधन नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए नागरिकों के किसी वर्ग द्वारा अपनी भाषा को बनाए रखने के लिए चलाए गए राजनैतिक आंदोलन को लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(3) के तहत “भ्रष्ट आचार” नहीं बनाया जा सकता।
कुल मिलाकर इस खंड के तहत, भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग (section) को, जिसकी अपनी विशेष बोली, भाषा, लिपि, या संस्कृति है, उसे संरक्षित करने का अधिकार है। यह व्यवस्था एक समूह के अधिकारों की रक्षा करती है।
अनुच्छेद 29(2) राज्य द्वारा पोषित या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।
जैसे कि हमने ऊपर समझा खंड (1) नागरिकों के किसी समूह के अधिकारों की रक्षा करती है। लेकिन खंड (2) नागरिकों को दिया गया एक व्यक्तिगत अधिकार है। यानी कि यह अधिकार किसी समुदाय के सदस्य के रूप में नहीं दिया गया है।
यह खंड ऐसे पीड़ित व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है जिसे उसके धर्म के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश देने से इंकार किया गया है।
⚫ याद रखिए, अगर प्रवेश पाने के इच्छुक नागरिक के पास आवश्यक क्वॉलिफ़िकेशन नहीं है तब वह ये नहीं कह सकता है कि अनुच्छेद 29(2) के अधीन उसके अधिकार का उल्लंघन हुआ है।
लेकिन अगर उसके पास आवश्यक क्वॉलिफ़िकेशन है लेकिन फिर भी उसे केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर प्रवेश देने से इंकार किया जाता है तो इस खंड के अधीन उसके अधिकारों का हनन माना जाएगा।
इसका दूसरा मतलब ये भी है कि अगर धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या लिंग से भिन्न किसी आधार पर किसी व्यक्ति को आरक्षण दिया जाता है या कुछ विशेष व्यवस्था की जाती है तो उसे इस अनुच्छेद का हनन नहीं माना जाएगा।
जैसे कि अगर संस्थान चाहे तो शारीरिक क्षमता, अनुशासन एवं प्रशिक्षण आदि को आधार बनाकर विशेष व्यवस्था तैयार कर सकती है।
यानी कि अगर आपको अनुशासन के कारण किसी कॉलेज से निकाला जाता है तो आप ये नहीं कह सकते है कि अनुच्छेद 29(2) का हनन हुआ है। [इसे आप विस्तार से आरक्षण लेख में समझ सकते हैं]
अनुच्छेद 29 के खंड (2) से संबंधित सबसे पॉपुलर मामला है चंपकम दोराईराजन का मामला 1951 जो कि बहुत से मायनों में काफी खास था। आइये इसे थोड़ा समझ लेते हैं;
चंपकम दोराइराजन बनाम मद्रास सरकार का मामला 1951
दरअसल चंपकम दोराइराजन नामक लड़की को मद्रास के एक मेडिकल कॉलेज में सिर्फ इसीलिए एड्मिशन नहीं मिला क्योंकि वहाँ सरकार के एक ऑर्डर से सीटों को समाज के अलग-अलग सेक्शन के लिए आरक्षित कर दिया गया था। जो कि कुछ इस तरह था।
हरेक 14 सीटों में से Non-Brahmin (Hindu) के लिए 6 सीटें, Backward Hindu के लिए 2 सीटें, Brahmin के लिए 2 सीटें, Harijan के लिए 2 सीटें, Anglo-Indians और Indian Christians के लिए 1 सीट और Muslims के लिए 1 सीट।
चंपकम दोराइराजन एक ब्राह्मण लड़की थी और क्वॉलिफ़िकेशन होने के बावजूद भी उसके लिए सीटें कम होने के वजह से उसका एड्मिशन नहीं हो पाया। तो उसने मद्रास उच्च न्यायालय में अपने मूल अधिकारों के हनन को लेकर एक याचिका दायर की।
चंपकम दोराइराजन का पक्ष – उन्होने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अनुच्छेद 15, 16 और अनुच्छेद 29(2) के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता है।
इस आर्ग्युमेंट के आधार पर तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि सीटों का आरक्षण गलत था। लेकिन फिर सरकार के तरफ से भी आर्गुमेंट दिया गया।
सरकार का पक्ष – सरकार ने DPSP के अनुच्छेद 46 का हवाला देते हुए कहा कि चूंकि उसके आधार पर सीटों को आरक्षित किया जा सकता है, इसीलिए किया गया। और अनुच्छेद 37 भी तो यहीं कहता है कि इसे लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।
अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट के सामने यही सवाल था कि क्या DPSP के आधार पर मूल अधिकार के हनन को जायज ठहराया जा सकता है?
सुप्रीम कोर्ट का फैसला – सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समुदाय के आधार पर दिया गया आरक्षण मूल अधिकारों का हनन करता है इसीलिए राज्य एड्मिशन के मामले में जाति या धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं कर सकता है, क्योंकि इससे अनुच्छेद 16(2) और अनुच्छेद 29(2) का हनन होता है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी बात कही कि जब भी कभी मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में टकराव होगा तो उस स्थिति में मूल अधिकार को ही प्रभावी माना जाएगा न कि DPSP को।
इस विषय को गहराई से समझें – मूल अधिकारों एवं निदेशक तत्वों में टकराव
——————————-
⚫ कुल मिलाकर खंड (1) किसी समूह से संबन्धित है जबकि खंड (2) किसी भी समूह के व्यक्ति से संबन्धित है। यहाँ पर एक बात जो याद रखने योग्य है कि अनुच्छेद 29 का शीर्षक तो अल्पसंख्यकों की बात करता है पर ये सभी नागरिकों पर लागू होता है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले की पुष्टि करते हुए कहा है कि ये सिर्फ अल्पसंख्यकों से संबन्धित नहीं है बल्कि सभी नागरिकों (यानी कि अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दोनों से) संबन्धित है।
⚫ यहाँ यह याद रखें कि अनुच्छेद 15 (1) भी विभेद के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है लेकिन वो एक साधारण संरक्षण है जबकि अनुच्छेद 29(2) के तहत जो संरक्षण की जाती है वो विशेष प्रकार के दोष के विरुद्ध संरक्षण है। और वह विशेष प्रकार का दोष है राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या वित्तपोषित शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश देने से इंकार करना।
अनुच्छेद 15(1) केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है जबकि अनुच्छेद 29(2) राज्य के साथ-साथ उन व्यक्तियों के विरुद्ध भी है जो यह अधिकार प्राप्त करने में बाधा डालता है।
तो कुल मिलाकर यही है अनुच्छेद 29 (Article 29), उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण – (1) भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।
(2) राज्य द्वारा पोषित या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।
विस्तार से समझने के लिए लेख पढ़ें;
संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं दी गई है। इस शब्द के साधारण अर्थ में इसका तात्पर्य है कोई भी ऐसा समुदाय जो राज्य की जनसंख्या के पचास प्रतिशत से कम है।
विस्तार से समझने के लिए लेख पढ़ें;
| Related Article
| ⚫ अनुच्छेद 25 ⚫ अनुच्छेद 26 ⚫ अनुच्छेद 27 ⚫ अनुच्छेद 28 ⚫ अनुच्छेद 30 |
| ⚫ Constitution ⚫ Basics of Parliament ⚫ Fundamental Rights ⚫ Judiciary in India ⚫ Executive in India |
अस्वीकरण - यहाँ प्रस्तुत अनुच्छेद और उसकी व्याख्या, मूल संविधान (नवीनतम संस्करण), संविधान पर डी डी बसु की व्याख्या (मुख्य रूप से) और संविधान के विभिन्न ज्ञाताओं (जिनके लेख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट पर ऑडियो-विजुअल्स के रूप में उपलब्ध है) पर आधारित है। हमने बस इसे रोचक और आसानी से समझने योग्य बनाने का प्रयास किया है।













