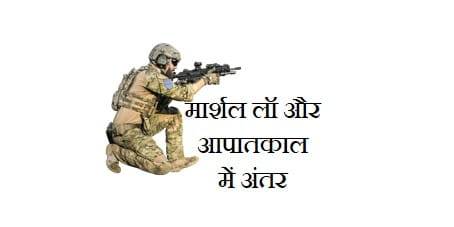चुनाव आयोग भारत के उन सबसे महत्वपूर्ण निकायों में से एक है जिसके बिना भारतीय लोकतंत्र की कल्पना करना शायद मुश्किल हो।
चुनाव के बिना लोकतंत्र अर्थहीन है और चुनाव तभी सार्थक या विश्वसनीय है जब इसे एक स्वतंत्र-स्वायत्त संस्था द्वारा करवाया जाए।
इस लेख में हम भारत के चुनाव आयोग (Election Commission of India – ECI) पर सरल और सहज चर्चा करेंगे तथा इसके सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को समझेंगे; तो भारत में चुनाव से संबन्धित सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए लेख को अंत तक जरूर पढ़ें:

| 📖 Read in English |
चुनाव आयोग क्या है?
भारतीय लोकतंत्र सफल इसीलिए है क्योंकि यहाँ एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत चुनाव कराया जाता है। और ये चुनाव इतने व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से हो पाता है क्योंकि यहाँ निर्वाचन आयोग (Election Commission) नामक एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय है।
कुल मिलाकर चुनाव आयोग लोकतंत्र को चलायमान बनाए रखने हेतु सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जिसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया था। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है।
अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयोग संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव कराता है साथ ही इसको निर्देशित और नियंत्रित भी करता है।
अत: चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि यह केंद्र व राज्य सरकारों दोनों के लिए समान है। निर्वाचन आयोग की सहायता आयोग के सचिवालय में कार्यरत सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिवों व अवर सचिवों आदि करता है।
राज्य स्तर पर, राज्य निर्वाचन आयोग की सहायता मुख्य निर्वाचन अधिकारी करते हैं, जिनकी नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त राज्य सरकारों की सलाह पर करता है। इसके नीचे जिला स्तर पर कलक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। वह जिले में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन अधिकारी व प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है।
यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि राज्यों में होने वाले पंचायतों व निगम चुनावों से चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है। इसके लिए भारत के संविधान में अलग राज्य निर्वाचन आयोगों की व्यवस्था की गई है।
चुनाव आयोग की संरचना
1950 से 15 अक्तूबर, 1989 तक चुनाव आयोग एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था यानी कि इसमें केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता था।
इससे आप समझ सकते हैं कि उस अकेले व्यक्ति पर काम का भार कितना अधिक रहता होगा। इसी भार को कम करने के उद्देश्य से 16 अक्तूबर, 1989 को राष्ट्रपति ने दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया। यानी कि उसके बाद आयोग बहुसदस्यीय संस्था के रूप में कार्य करने लगा, जिसमें तीन निर्वाचन आयुक्त था।
हालांकि 1990 में एक बार फिर दोनों अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों के पद को समाप्त कर दिया गया जिससे कि स्थिति एक बार पहले की तरह हो गई ।
लेकिन फिर से अक्तूबर 1993 में दो निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया। इसके बाद से अब तक आयोग बहुसदस्यीय संस्था के तौर पर काम कर रहा है, जिसमें तीन निर्वाचन आयुक्त है।
⚫ मुख्य निर्वाचन आयुक्त व दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों शक्तियाँ समान ही होती है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। और ये शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि किसी विषय पर विवाद की स्थिति में जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त व दो अन्य निर्वाचन आयुक्त बहुमत के आधार पर निर्णय करता है।
⚫ मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हर राज्य में एक प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त भी होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सलाह पर करता है।
⚫ चाहे केंद्र की निर्वाचन आयुक्तों की बात करें या प्रादेशिक आयुक्तों की, इन सभी की सेवा शर्तें व पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है।
⚫ निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो, तक होता है। वैसे अगर वे चाहे तो किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं या फिर उन्हे कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है लेकिन उसे उसी तरह से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है।
चुनाव आयोग कितना स्वतंत्र है?
चुनाव आयोग का स्वतंत्र होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर ये सरकार के कंट्रोल में रहा तो फिर लोकतंत्र के साख पर बट्टा लगना तय है। इसीलिए अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के स्वतंत्र व निष्पक्ष कार्य करने के लिए कुछ बहुत ही जरूरी उपबंध की व्यवस्था की गई है। जो कि निम्नलिखित है।
1. राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त को नियुक्त तो करता है पर चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद्पर्यंत काम नहीं करता। इसका मतलब ये है राष्ट्रपति उसे अपने मन से हटा नहीं सकता है। एक बात नियुक्त होने के बाद वे अपने निर्धारित पदावधि तक काम करने के लिए स्वतंत्र है।
यदि उस पर कदाचार या अक्षमता का आरोप लगता है और उसे हटाना जरूरी हो जाता है तब भी उसे उसी विधि से हटाया जाएगा जिस विधि से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है यानी कि महाभियोग के द्वारा। जिसके लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से संकल्प पारित करना पड़ता है।
2. एक बार नियुक्त हो जाने के बाद उसके सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे कि उसके वेतन की बात करें तो उसे बढ़ाया तो जा सकता है लेकिन घटाया नहीं जा सकता।
3. नया चुनाव आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफ़ारिश पर ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं।
दोष
हालांकि निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र व निष्पक्ष काम करने के लिए संविधान के तहत दिशा-निर्देश दिये गए है लेकिन इसमें कुछ दोष भी हैं: जैसे कि –
1. एक निर्वाचन आयुक्त बनने के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए इसका जिक्र सविधान में नहीं किया गया है।
2. संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि कितनी है।
3. संविधान में सेवानिवृत के बाद निर्वाचन आयुक्तों की सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है।
चुनाव आयोग के कार्य व शक्तियाँ
1. जनसंख्या बढ़ जाने से या फिर किसी अन्य राजनीतिक कारण से निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (delimitation) की आवश्यकता पड़ती रहती है। इसीलिए ये राष्ट्रपति के आदेशानुसार (संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर) समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भू-भाग का निर्धारण करता है।
2. ये समय-समय पर वोटर लिस्ट तैयार करता है और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करता है। आमतौर पर तीन तरह के मतदाता होते है
(1) सामान्य मतदाता (General voter)
(2) सेवा मतदाता (Service voters)
(3) विदेशी मतदाता (Overseas Voters)।
(1) सामान्य मतदाता (General voter) – कोई भी व्यक्ति मतदाता के रूप में खुद नामांकन करवा सकता है यदि वे:
(1) एक भारतीय नागरिक हैं।
(2) 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, (मतदाता सूची के संशोधन के वर्ष की पहली तारीख यानी 1 जनवरी को)
(3) आंशिक रूप से उस चुनाव क्षेत्र के निवासी हो जहां वे वोट डालना चाहते हैं
(4) सक्षम प्राधिकारी द्वारा वोट डालने के लिए अयोग्य न ठहराया गया हो।
अगर आप मतदाता बनना चाहते है और उसके लिए नामांकन करवाना चाहते है तो चुनाव आयोग के इस लिंक↗️ का इस्तेमाल कर सकते हैं।
(2) सेवा मतदाता (Service voters) – सेवा योग्यता रखने वाले मतदाता को सेवा मतदाता के रूप में जाना जाता है, ये हैं –
(1) भारत के सशस्त्र बल का सदस्य,
(2) सेना अधिनियम (Army act) 1950 के तहत आने वाले सभी बलों के सदस्य,
(3) किसी राज्य के सशस्त्र बल पुलिस बल जो अपने राज्य के बाहर सेवा दे रहा है,
(4) भारत सरकार के अधीन कार्यरत व्यक्ति, जो भारत से बाहर सेवा दे रहा है।
सर्विस वोटर्स कैसे चुनाव के लिए नामांकन करवा सकता है इसके लिए चुनाव आयोग के इस लिंक↗️ को विजिट कीजिये।
(3) विदेशी मतदाता (Overseas Voters) – भारत का एक नागरिक, जो रोजगार, शिक्षा आदि के कारण देश से अनुपस्थित है, और किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है, उसे प्रवासी मतदाता के रूप में जाना जाता है। वे अपने भारतीय पासपोर्ट में उल्लिखित पते पर मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के योग्य हैं। इसके लिए क्या प्रावधान है इसे जानने के लिए चुनाव आयोग के इस लिंक↗️ को फॉलो कीजिये।
3. ये निर्वाचन की तिथि और समय सारणी निर्धारित करता है एवं नामांकन पत्रों का परीक्षण करता है।
4. ये राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है तथा निर्वाचन में प्रदर्शनों के आधार पर उसे राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल का दर्जा देता है। चुनाव चिन्ह देने के मामले में हुए विवाद के समाधान के लिए न्यायालय की तरह काम करता है।
5. ये निर्वाचन के समय दलों एवं उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता (Code of conduct) का निर्माण करता है और निर्वाचन व्यवस्था से संबन्धित विवाद की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त करता है।
6. ये संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबन्धित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है और विधानमण्डल के सदस्य की निरर्हता से संबन्धित मसलों पर राज्यपाल को सलाह देता है।
7. ये समस्त भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनावी तंत्र का पर्येवक्षण करता है और मतदान केंद्र की लूट, हिंसा व अन्य अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन रद्द कर सकता है।
8. ये निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में विभिन्न हितधारकों, जैसे मतदाता, राजनीतिक दल, चुनाव अधिकारी, उम्मीदवार एवं सामान्य जनता, में जागरूकता का प्रसार करता है। इसके लिए ये विभिन्न आधुनिक माध्यमों का सहारा लेता है। जागरूकता के लिए इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टल है – SVEEP↗️, आप चाहे तो इसे विजिट कर सकते हैं।
तो कुल मिलाकर भारत का चुनाव आयोग (Election Commission of India) स्वतंत्रता, स्वायतत्ता तथा अखंडता को बनाए रखता है।
और यह हितधारकों की उपलब्धता तथा नैतिक भागीदारी को सुनिश्चित करता है। यह स्वतंत्र, दोषमुक्त तथा पारदर्शी चुनाव को संपन्न कराने के लिए उच्चतम पेशेवर मानदंडों का पालन करता है ताकि जनता का लोकतंत्र में विश्वास मजबूत हो।

![संविधान निर्माण की कहानी | संविधान कैसे बना? [UPSC Concept]](https://wonderhindi.com/wp-content/uploads/2020/05/Story-of-making-of-Constitution.jpg)
![धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार [Right to religious freedom]](https://wonderhindi.com/wp-content/uploads/2020/05/धार्मिक-स्वतंत्रता-का-अधिकार1.jpg)
![राज्य के नीति निदेशक तत्व [DPSP Explained]](https://wonderhindi.com/wp-content/uploads/2020/05/Directive-Principles-of-State-Policy1.jpg)