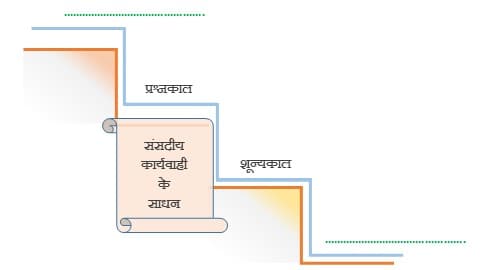जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उस समय चुनाव करवाने के लिए बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं थी;
जैसे कि मतदाता सूची एवं सीटों का आवंटन आदि। इसी को स्पष्ट करने के लिए जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 अधिनियमित किया गया।
इसे लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act 1950) भी कहा जाता है इस लेख में हम इसी पर चर्चा करेंगे।
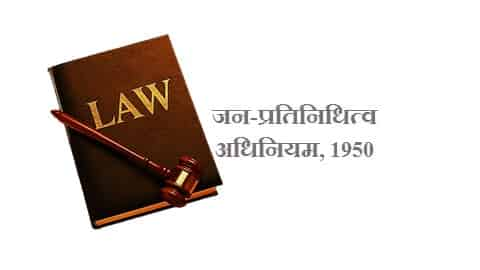
| 📖 Read in English |
जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की पृष्ठभूमि
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव किसी भी लोकतंत्र की एक मूल तत्व है। भारत में इसे सुनिश्चित करने के लिए एक सशक्त एवं स्वायत्त चुनाव आयोग की स्थापना 26 नवम्बर 1949 को की गई, जिसे कि संविधान के भाग XV के आर्टिकल 324 – 329 में वर्णित किया गया है।
भारत का चुनाव आयोग (ECI) देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए जिम्मेदार है। स्वतंत्रता के बाद, हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (Universal adult franchise) व्यवस्था को अपनाया और इसे अनुच्छेद 325 और 326 के तहत संवैधानिक मान्यता दी।
जहां अनुच्छेद 325 सार्वभौमिक मताधिकार सुनिश्चित करता है और यह प्रदान करता है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर किसी मतदाता सूची में शामिल होने का दावा करने के लिए अयोग्य नहीं होगा। और अनुच्छेद 326 में लिखा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा।
[सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सभी वयस्क नागरिकों के वोट का अधिकार है, वो भी धन, आय, लिंग, सामाजिक स्थिति, नस्ल या जातीयता की परवाह किए बिना। (केवल मामूली अपवादों को छोड़कर)]
तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग तो बन गया था लेकिन पहला चुनाव कराने से पहले उसे कई प्रकार के नीतिगत समस्याओं का सामना करना पड़ा क्योंकि इससे संबन्धित कानून स्पष्ट नहीं थे। जैसे कि लोकसभा और विधानसभाओं के लिए सीटों का आवंटन, मतदाता की अर्हता, मतदाता सूचियों का निर्माण, उम्मीदवारों की योग्यता और अयोग्यता, भ्रष्ट आचरण, आचार संहिता आदि ऐसे अनेक प्रश्न अनुत्तरित था।
इसीलिए संसद ने जन प्रतिनिधित्व कानून (Representation of the People Act 1950), और जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 (Representation of the People Act 1951) बनाया ताकि चुनावों से संबन्धित सभी प्रावधान स्पष्ट और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप हो सके और चुनाव के संचालन के लिए एक उपयुक्त कानूनी ढांचा प्रदान किया जा सके।
जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की व्याख्या
ये पूरा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 5 भागों और 7 अनुसूचियों में बंटा हुआ है, जहां अगर अनुसूचियों की बात करें तो 7 अनुसूचियों में से अंतिम 3 अनुसूची निरस्त हो चुका है। किस भाग में क्या-क्या प्रावधान है और किसी अनुसूची में क्या प्रावधान है इसे आप इस टेबल में देख सकते हैं। इसे याद रखे ताकि माइंड में एक मैप तैयार हो जाये।
जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 : एक झलक में
| भाग | विषय-वस्तु | धाराएँ |
|---|---|---|
| 1 | प्रारम्भिक | 1-2 |
| 2 | सीटों का आबंटन एवं चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन | 3-13 |
| 2A | पदाधिकारी | 13A |
| 2B | संसदीय क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची | 13D |
| 3 | विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची | 14-25A |
| 4 | परिषद क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची | 26-27 |
| 4A | राज्यों की परिषदों में सीटें भरना, संघीय प्रतिनिधियों द्वारा सीटें भरना | 27A-27K |
| 5 | सामान्य | 28-32 |
जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की अनुसूचियाँ
| अनुसूची | विषय-वस्तु |
|---|---|
| पहली अनुसूची | लोकसभा में सीटों का आवंटन |
| दूसरी अनुसूची | विधानसभाओं में कुल सीटों की संख्या |
| तीसरी अनुसूची | विधान परिषदों में सीटों का आवंटन |
| चौथी अनुसूची | विधान परिषदों के चुनाव के प्रयोजनों के लिए स्थानीय अधिकारी |
♠️ भाग 1 जिसका विषय-वस्तु प्रारम्भिक है, (इसके तहत धारा 1 और धारा 2 आता है) इसमें कुछ खास जानने को है नहीं इसीलिए उसे यहाँ डिस्कस करने का ज्यादा फायदा है नहीं। फिर भी आपको जानने का मन है तो आप दिये पीडीएफ़ को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको आगे सब भाग का मूल पीडीएफ़ दिया जाएगा ताकि विस्तार से अध्ययन करने के लिए उसे देख सकें।
भाग 2 – सीटों का आवंटन एवं चुनाव क्षेत्रों का सीमांकनpdf
अधिनियम के इस भाग में, धारा 2 से लेकर 13 तक आता है, जिसे कि पाँच शीर्षकों में विभाजित किया गया है।
पहला शीर्षक – लोक सभा
इसमें वैसे तो 3 से 6 तक धाराएँ है लेकिन धारा 3 और 4 को छोड़कर सब निरस्त हो चुका है। धारा 3 ”लोकसभा में सीटों के आवंटन” के बारे में है और धारा 4 ”लोकसभा एवं संसदीय चुनाव क्षेत्रों में सीटों की भराई” के बारे में है। आइये इसे समझ लेते हैं।
संविधान के अनुच्छेद 81 तथा अनुच्छेद 170 में संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं में अधिकतम सीटों की संख्या संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, साथ ही उन सिद्धांतों का भी उल्लेख किया गया है जिनके आधार पर लोकसभा तथा राज्यों की विधान सभाओं में सीटों का आवंटन किया जाता है लेकिन ऐसी सीटों का वास्तविक आवंटन जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 द्वारा प्रदान किया जाता है।
हम जानते हैं कि लोकसभा के लिए अधिकतम 550 सीटें आवंटित की गई है वहीं राज्यों के विधानसभा के लिए न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 (कुछ अपवादों को छोड़कर) सीटों की व्यवस्था की गई है लेकिन वास्तविक संख्या इससे हमेशा कम होती है। कहाँ कितनी सीटें होंगी ये परिसीमन आयोग की सिफ़ारिशों से तय होता है।
भाग 2 के धारा 3 में मूल रूप से यही लिखा हुआ है कि लोकसभा के लिए राज्यों में जो सीटों का आवंटन किया गया है (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों के साथ) वे वहीं होंगे जो जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुसूची 1 में लिखा है। परिसीमन आदेश 2008 के तहत अभी वर्तमान में अनुसूची 1 की स्थिति कुछ ऐसी है, जैसे कि दिये हुए पीडीएफ़↗️ में दिखाया गया है।
◾धारा 4 में यही कहा गया है कि धारा 3 के तहत जो सीटों का आवंटन किया गया है उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरे जाएँगे।
दूसरा शीर्षक – राज्यों की विधानसभाएँ
इसके तहत धारा 7 और धारा 7A आता है। धारा 7 कहता है कि राज्य विधानसभाओं के लिए जो सीटों का आवंटन होगा (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों के साथ) वो वही होगा जो अनुसूची 2 में लिखा है। अनुसूची 2 के वर्तमान स्थिति को आप दिये गए पीडीएफ़↗️ में देख सकते हैं।
धारा 7A सिक्किम विधानसभा तथा विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में सीटों की कुल संख्या के बारे में है। आपको पता होगा कि ये अधिनियम 1950 का है जबकि सिक्किम 1975 में भारत का एक राज्य बना था इसीलिए बाद में सिक्किम के लिए कुछ प्रावधान जोड़ा गया।
तीसरा शीर्षक – संसदीय एवं विधानसभा चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन आदेश
इसके अंतर्गत 3 धाराएँ हैं – 8, 8A और 9। धारा 8 ”सीमांकन आदेशों का समेकन” के बारे में है, धारा 8A ”अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर अथवा नागालैंड राज्यों में संसदीय एवं विधानसभा चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन” के बारे में है, और धारा 9 ”सीमांकन आदेश को अद्यतन (up to date) बनाए रखने की चुनाव आयोग की शक्ति” के बारे में है।
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1950 निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की व्यवस्था करता है। यानी कि लोक सभा और राज्यों की विधानसभाओं और विधान परिषदों में सीटों के आवंटन के लिए प्रावधान करता है ।
अधिनियम राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करता है कि वे चुनाव आयोग से परामर्श करके लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं एवं विधान परिषदों की सीटें भरने के लिए विभिन्न चुनाव क्षेत्रों की संख्या को पुनर्निर्धारित कर सकते हैं।
चुनाव क्षेत्र का परिसीमन
राष्ट्रपति, चुनाव आयोग से परामर्श लेने के बाद परिसीमन की व्यवस्था को संशोधित कर सकता है। चुनाव आयोग मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को निर्धारित करने की शक्ति रखता है।
पहला परिसीमन आदेश राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग के साथ और अगस्त 1951 में संसद की मंजूरी के साथ जारी किया था
सीमांकन अधिनियम, 2002
भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 तथा 170 प्रत्येक राज्य को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों (संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं विधानसभा क्षेत्रों) में बँटवारे तथा पुनर्स्थापन का प्रावधान करते हैं और इसका आधार जनगणना, 2001 है।
साथ ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 330 तथा 332 लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या का पुनर्निधारण का प्रावधान जनगणना, 2001 के आधार पर करते हैं।
हालांकि ये याद रखिए कि वर्तमान में संसदीय एवं विधानसभा क्षेत्रों का सीमांकन 1971 की जनगणना पर आधारित है। भारत के विभिन्न भागों में असमान जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ किसी एक ही राज्य में मतदाताओं का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर सतत् अप्रवास, (विशेषकर गाँवों से शहरों की ओर) का परिणाम यह हुआ है कि एक ही राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों के आकार में भारी अंतर है।
इसलिए सीमांकन अधिनियम, 2002 अधिनियमित किया गया जिसका उद्देश्य 2001 की जनगणना के आधार पर सीमांकन को प्रभावी बनाना था जिससे कि सारे निर्वाचन क्षेत्रों के आकार में एकरूपता स्थापित की जा सके।
इसके लिए 2001 में ही सीमांकन आयोग बनाया गया था इसका एक काम अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को पुनर्निर्धारित भी करना था, लेकिन 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित सीटों की कुल संख्या को बिना प्रभावित किए।
धारा 8 कुछ यही कहता है कि – अरुणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, मणिपुर और नागालैंड राज्यों के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़कर समस्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों का विस्तार ऐसा होगा जैसा परिसीमन अधिनियम 2002 के उपबंधों के अधीन परिसीमन आयोग द्वारा दिये गए आदेशों द्वारा अवधारित किया गया हो,
और साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, मणिपुर और नागालैंड राज्यों के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार ऐसा होगा जैसा परिसीमन अधिनियम 2002 की धारा 10A और धारा 10B के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आदेश 2008 में उपबंधित किया गया हो।
परिसीमन अधिनियम 2002pdf की धारा 10A और धारा 10B में ये लिखा हुआ है, आप इसे नीचे देख सकते हैं।

तो अब आप समझ रहे होंगे कि इसी प्रकार के सभी आदेशों को एकल आदेश में समेकित करने की बात धारा 8 करता है। जिसे कि परिसीमन आदेश 2008 के नाम से जाना जाता है। इसी आदेश में अपडेट करने की निर्वाचन आयोग की शक्ति के बारे में धारा 9 में बताया गया है।
चौथा शीर्षक – राज्य विधान परिषदें
धारा 10 और 11 क्रमशः विधान परिषदों में सीटों का आवंटन एंव परिषद चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन की बात करता है। अनुच्छेद 171 किसी राज्य की विधान परिषद् में अधिकतम एवं न्यूनतम सीटों का प्रावधान करता है, और उन विधियों का भी उल्लेख करता है जिनका उपयोग कर सीटें भरी जाएँगी। लेकिन यहाँ भी सीटों का वास्तविक आवंटन इस अधिनियम के धारा 10 के द्वारा प्रदान किया जाता है। और धारा 11 परिसीमन की बात करता है।
पंचम शीर्षक – चुनाव क्षेत्रों के सीमांकन आदेशों संबंधी प्रावधान
इसके तहत दो धाराएँ है धारा 12 एवं धारा 13। धारा 12 राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि धारा 11 के तहत अपने दिये गए आदेश को वह चुनाव आयोग से परामर्श करने के बाद परिवर्तित कर सकता है। और धारा 13 के तहत धारा 11 एवं 12 के अधीन दिये गए हर आदेश को यथाशीघ्र संसद के समक्ष रखा जाएगा।
भाग 2A – ऑफिसरpdf
इस भाग के अंतर्गत कुल 5 धाराएँ हैं, जो कि कि निम्नलिखित है।
⚫ धारा 13A के तहत मुख्य चुनाव अधिकारी की बात कही गई है।
⚫ धारा 13AA के तहत जिला चुनाव अधिकारी की बात कही गई है।
⚫ 13B के तहत चुनाव निबंधन पधाधिकारी,
⚫ 13C के तहत सहायक चुनाव निबंधन पधाधिकारी और
⚫ 13CC के तहत मुख्य चुनाव अधिकारी, जिला चुनाव अधिकारी आदि को चुनाव आयोग की प्रतिनियुक्ति पर माना जाना, शामिल है। इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके है आप इसके लिए चुनाव↗️ नामक लेख पढ़िये।
भाग 2B – संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियाँpdf
इसके बारे में धारा 13D में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर राज्य में या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र में जिसमें विधानसभा नहीं है, संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से भिन्न हर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली उतने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों से मिलकर गठित होगी जितने उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में समाविष्ट हैं और ऐसे किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली पृथक्त: तैयार या पुनरीक्षित करना आवश्यक नहीं होगा।
भाग 3 – विधानसभा चुनाव क्षेत्रों के लिए निर्वाचक सूचीpdf
इसके बारे में धारा 14 से लेकर 25A में बताया गया है जो कि निम्नलिखित है।
धारा 14 – परिभाषाएँ
धारा 15 – हर निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली होगी जो चुनाव आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार तैयार की जाएगी।
धारा 16 – निर्वाचक नामावली में पंजीकृत किए जाने के लिए अयोग्यताएँ
यदि कोई व्यक्ति – भारत का नागरिक नहीं है; अथवा विकृतचित है और उसके ऐसा होने की सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान है; अथवा भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से संबन्धित किसी विधि के उपबंधों के अधीन मतदान करने के लिए उस समय अयोग्य घोषित किए गए हो। ऐसे व्यक्ति व्यक्ति को निर्वाचक नामावली में नामांकन नहीं किया जाएगा।
धारा 17 – एक से अधिक निर्वाचन-क्षेत्र में किसी व्यक्ति का नाम पंजीकृत नहीं किया जाएगा।
धारा 18 – किसी निर्वाचन-क्षेत्र में कोई व्यक्ति एक से अधिक बार पंजीकृत नहीं किया जाएगा।
धारा 19 – मतदाता नामावली में पंजीकृत कराने की शर्तें।
हर व्यक्ति जो – (क) अर्हता की तारीख को 18 वर्ष से कम आयु का नहीं हैं; तथा (ख) किसी निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है, उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में पंजीकृत कराने का हकदार होगा।
धारा 20 – मामूली तौर से निवासी का अर्थ यानी कि किस प्रकार के व्यक्ति को किसी निर्वाचन क्षेत्र का मामूली निवासी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा; इसी को इस धारा में बताया गया है।
धारा 21 – निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण के बारे में इस धारा में बताया गया है।
धारा 22 – निर्वाचक नामावलियों में की गई प्रविष्टियों की शुद्धिकरण से संबन्धित है।
धारा 23 – निर्वाचक नामावलियों में नामों का सम्मिलित किया जाना जिसका नाम इसमें नहीं है। (निर्वाचक पंजीकरण ऑफिसर को आवेदन देकर)
धारा 24 – अपीलें; यानी कि ऐसे आदेश के खिलाफ जो कि किसी निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा धारा 22 या धारा 23 के अधीन दिया गया हो।
धारा 25 – आवेदनों और अपीलों के लिए जो फीस ली जाएगी वो वापस नहीं होगी।
धारा 25A – सिक्किम के संघ निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक के रूप में पंजीकरण की शर्तों के बारे में इस धारा में बताया गया है।
भाग 4 – विधानपरिषद क्षेत्रों के लिए मतदाता सूचीpdf
इसके बारे में धारा 27 में बताया गया है। इसमें विधानपरिषद निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी के बारे में बताया गया है।
भाग 4Apdf
संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले राज्य सभा में स्थानों को भरने की रीति के बारे में इस धारा में बताया गया है।
भाग 5 – सामान्य प्रावधानpdf
इस भाग में धारा 28 से लेकर 32 तक का संकलन है।
धारा 28 – नियम बनाने की शक्ति के बारे में है।
धारा 29 – स्थानीय प्राधिकारियों को आवश्यकतानुसार कर्मचारी उपलब्ध कराना।
धारा 30 – सिविल न्यायालयों की अधिकारिता वर्जित
धारा 31 – मिथ्या घोषित करना
धारा 32 – निर्वाचक नामावलियों की तैयारी आदि से संबन्धित ऑफिशियल ड्यूटी में उल्लंघन।
तो कुल मिलाकर यही था जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 (Representation of the People Act 1950), इस लेख में बहुत सारे धाराओं की विस्तार से व्याख्या नहीं की गई है, विस्तार से जानने के लिए उसके मूल पीडीएफ़↗️ को पढ़ सकते हैं।
⚫⚫⚫
जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 अभ्यास प्रश्न
⚫ Other Important Articles ⚫
https://legislative.gov.in/sites/default/files/EM_3%2528peoples%2520rep%2520act%25201950%2529.pdf

![EVM और VVPAT किसे कहते है ? [UPSC]](https://wonderhindi.com/wp-content/uploads/2021/01/evm.jpg)
![संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक [UPSC]](https://wonderhindi.com/wp-content/uploads/2020/10/संयुक्त-बैठक.jpg)
![राज्यपाल : संवैधानिक प्रावधान, नियुक्ति, इत्यादि [UPSC]](https://wonderhindi.com/wp-content/uploads/2020/08/Governor.jpg)