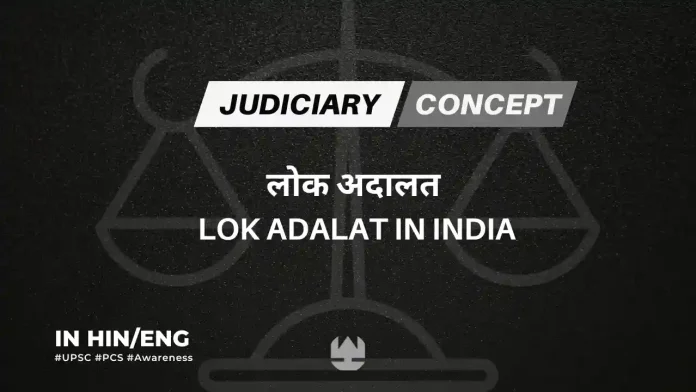लोक अदालत । Lok Adalat in India in hindi [UPSC]
अधीनस्थ या उच्च न्यायालय से न्याय प्राप्त करना बहुत माथापच्ची भरा है इसीलिए न्याय को आसान बनाने के उद्देश्य लोक अदालत का कॉन्सेप्ट लाया गया।
इस लेख में लोक अदालत (Lok Adalat) पर सरल और सहज चर्चा करेंगे एवं इसके महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने के कोशिश करेंगे, तो इस लेख को अच्छी तरह से समझने के लिए अंत तक जरूर पढ़ें।
लोक अदालत क्या है?
भारत की जो मुख्य अदालतें है उसके बारे में तो जानते ही होंगे कि वे हजारों-हज़ार लंबित मुकदमों से दबी पड़ी है। तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख होते हुए कब 10-15 साल बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और नतीजतन इंसाफ में बहुत ही ज्यादा देरी हो जाता है।
इसी को बाईपास करने के लिए एवं मुख्य न्यायालय के बोझ को कम करने के लिए और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए लोक अदालत (Lok Adalat) नामक एक फोरम का गठन किया गया।
ये अदालतें अनौपचारिक, सस्ता और सुलभ न्याय प्राप्ति के लिए एक बेहतरीन मंच प्रदान करता है। यहाँ पर बातचीत, मध्यस्थता, मान-मनौव्वल, कॉमन सेंस तथा वादियों की समस्यायों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर विशेष रूप से प्रशिक्षित एव अनुभवी विधि अभ्यासियों द्वारा मामले निपटाए जाते हैं।
निर्णय इस प्रकार दिये जाते है कि दोनों पक्ष उसे खुशी-खुशी स्वीकार करे। इसीलिए कहा जाता है कि लोक_अदालत की कार्यवाही में कोई विजयी या पराजित नहीं होता।
लोक अदालत का अधिकार क्षेत्र
इसके क्षेत्राधिकार कि बात करें तो ये विवाह संबंधी विवाद, आपराधिक मामले, भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले, श्रम विवाद, कर्मचारी क्षतिपूर्ति के मामले, बैंक बसूली के मामले, पेंशन मामले, आवास मामले, वित्त संबंधी मामले, उपभोक्ता शिकायत के मामले आदि की सुनवाई कर सकता है।
यहाँ पर दो प्रकार के मामलों की ही सुनवाई होती है
(1) ऐसे मामले जो अदालतों में लंबित है या
(2) ऐसे मामले जो अभी अदालतों तक नहीं पहुंचे है।
लोक अदालतें ऐसे मामलों की सुनवाई नहीं कर सकती जो किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है या जिस पर सुनवाई की तारीख निर्धारित हो।
दूसरी बात कि लोक अदालत उन मामलों की भी सुनवाई नहीं कर सकता है जो किसी कानून के तहत समाधान योग्य नहीं है। यानी कि ऐसे अपराध जिसका निपटारा मेन स्ट्रीम अदालत करता है। इसे गैर-समाधेय अपराध (Non Compoundable offence) कहा जाता है।
[Compoundable offences और Non Compoundable offences को विस्तार से जानें।]
वैधानिक विशेषताएँ –
1982 में लोक_अदालत गुजरात में एक प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया था लेकिन ये विवादों को निपटाने में इतनी सफल रही कि जल्द ही अन्य राज्यों में भी इसे अपनाया गया।
इसकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए लोगों ने इसे वैधानिक दर्जा देने की मांग कि फलस्वरूप 1987 में ”वैधानिक सेवाएँ प्राधिकरण अधिनियम” द्वारा इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। इसकी वैधानिक विशेषताएं कुछ इस प्रकार है-
1. राज्य वैधानिक सेवाएँ प्राधिकरण (SLSA) या जिला वैधानिक सेवाएँ प्राधिकरण (DLSA) या सर्वोच्च न्यायालय वैधानिक सेवाएँ प्राधिकरण (SCLSA) या फिर उच्च न्यायालय वैधानिक सेवाएँ प्राधिकरण (HCLSA) लोक अदालतों का आयोजन कर सकता है और वहाँ पर आयोजन कर सकता है जहां पर वो उपयुक्त समझता है।
आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऊपर बताए गए ये वैधानिक सेवाएँ प्राधिकरण है क्या? ये एक अलग टॉपिक है जो न्याय व्यवस्था से तो जुड़ा ही हुआ है साथ ही राज्य के नीति निदेशक तत्व से भी जुड़ा हुआ है। तो इसे समझने के लिए –राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण↗️ पढ़ सकते हैं।
2. लोक_अदालत में सुनवाई करने वाले कितने सदस्य होंगे इसका निर्धारण इसका आयोजन करने वाले करते हैं। साधारणत: एक लोक अदालत में अध्यक्ष के रूप में एक न्यायिक अधिकारी तथा एक वकील व सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों के रूप में होते है।
3. अदालत के समक्ष लंबित किसी मामले को लोक_अदालत सुनवाई के लिए लाया जा सकता है यदि:
(1) यदि दोनों पक्ष विवाद का समाधान लोक अदालत में करना चाहते हैं, या
(2) कोई एक पक्ष उस मामले को लोक अदालत में भेज देने के लिए आवेदन देता है, या
(3) यदि न्यायालय संतुष्ट है कि मामला लोक अदालत के संज्ञान में लाये जाने के उपयुक्त है।
4. लोक अदालतों की शक्तियों के बारे में बात करें तो, इसे वही शक्तियाँ प्राप्त होती है जो कि सिविल कोर्ट को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर (1908) के अंतर्गत प्राप्त होती है।
इस प्रकार लोक अदालत में चली कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860 में निर्धारित अर्थों में अदालती कार्यवाही माना जाएगा तथा प्रत्येक लोक अदालत को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) (1973) के उद्देश्य से एक सिविल कोर्ट माना जाएगा।
6. लोक_अदालत का निर्णय सिविल कोर्ट के हुकुमनामे अथवा किसी भी अन्य अदालत के किसी भी आदेश की तरह मान्य होगा। लोक अदालत द्वारा दिया गया फैसला अंतिम तथा सभी पक्षों पर बध्याकारी होगा और लोक अदालत के फैसले के विरुद्ध किसी अदालत में कोई अपील नहीं होगी।
लोक अदालत के लाभ
1. यहाँ कोई अदालती फीस नहीं लगती और अगर किसी पक्ष द्वारा अदालती फीस का भुगतान कर दिया गया हो तो लोक अदालत में मामला निपटने के बाद राशि लौटा दी जाएगी। इसके अलावा इसमें समय भी कम लगता है और ये नियमित न्यायालयों के तकनीकी उलझनों से मुक्त होता है।
2. यहाँ सभी पक्ष अपने वकीलों के माध्यम से न्यायाधीश से सीधे संवाद कर सकते है, जो की नियमित न्यायालयों में संभव नहीं है साथ ही यहाँ सम्बद्ध पक्ष अपने मतभेदों पर खुलकर चर्चा कर सकते है जो कि विवाद सुलझाने में सहायक सिद्ध होती है।
3. यहाँ विवादों का समाधान शीघ्र, नि:शुल्क तथा सौहार्दपूर्ण ढंग से हो जाता है और यहाँ कोई विजयी या पराजित नहीं होता।
स्थायी लोक अदालत क्या है?
हमने ऊपर ही पढ़ा कि लोक अदालतों को विभिन्न न्यायिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित करवाया जाता है। यानी कि ये विधि मान्य तो हो गया था लेकिन स्थायी नहीं हुआ था।
इसीलिए ‘कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987‘ को 2012 में संशोधित कर सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं से जुड़े मामलों के लिए स्थायी लोक अदालतों का प्रावधान किया गया।
स्थायी लोक अदालत की विशेषताएँ
लोक अदालत के मुक़ाबले स्थायी लोक अदालत में जो प्रमुख बदलाव लाये गए वो कुछ इस प्रकार है –
1. स्थायी लोक अदालत का अध्यक्ष वो होगा जो कि जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रहा हो अथवा जो जिला न्यायाधीश से भी उच्चतर श्रेणी की न्यायिक सेवा में रहा हो। इसके साथ ही दो अन्य व्यक्ति होंगे जिन्हे सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त अनुभव हो।
2. स्थायी लोक अदालत के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अधिक जनोपयोगी सेवाएँ होंगी, जैसे, यात्री अथवा माल परिवहन, टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवाएँ, किसी संस्थान द्वारा जनता को बिजली, प्रकाश या पानी की आपूर्ति, अस्पतालों में सेवाएँ, बीमा सेवाएँ आदि।
3. स्थायी लोक अदालत का गैर-समाधेय (Non Compoundable) मामलों में कोई कोई क्षेत्राधिकार नहीं होगा।
4. आवेदन स्थायी लोक अदालत को प्रस्तुत करने के बाद उस आवेदन का कोई भी पक्ष उसी वाद में किसी न्यायालय मे समाधान के लिए नहीं जाएगा।
5. जब कभी स्थायी अदालत को ऐसा प्रतीत हो कि किसी वाद में समाधान के तत्व मौदूद है जो संबन्धित पक्षों को स्वीकार्य हो सकते है तब वह संभावित समाधान को एक सूत्र दे सकती है और उसे पक्षों के समक्ष रख सकती है ताकि वे भी उसे देख ले समझ ले।
यदि इसके बाद वादी (complainant) एक समाधान तक पहुंच जाते है तो लोक अदालत इस आशय का फैसला सुना सकती है। यदि वादी समझौते के लिए तैयार नहीं हो पाते तब लोक अदालत बाद के गुणदोष के आधार पर फैसला सुना सकती है।
7. स्थायी लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक न्याय निर्णय अंतिम होगा और वादियों एवं समस्त पक्षों पर बाध्यकारी होगा। (लोक अदालत के गठन में शामिल व्यक्तियों के बहुमत के आधार पर फैसला पारित होगा)
लोक_अदालत की खामी-
लोक अदालतों की सबसे बड़ी खामी ये है कि इसकी व्यवस्था प्रमुखत: समझौता अथवा पक्षों के बीच समाधान पर आधारित है।
यदि दोनों पक्ष किसी समझौते या समाधान तक नहीं पहुँच पाते तब मामला या तो न्यायालय को वापस भेज दिया जाता है जहां से वह यहाँ भेजा गया था या दोनों पक्षों को सलाह दी जाती है की वे अपने विवाद को न्यायालयी प्रक्रिया द्वारा सुलझाएँ। इससे न्याय प्राप्त मे अनावश्यक देरी होती है।
कुल मिलाकर यही है लोक_अदालत। इस लेख को अच्छे से समझने के लिए राष्ट्रीय वैधानिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा को एक बार अवश्य पढ़ लें, लिंक नीचे भी है