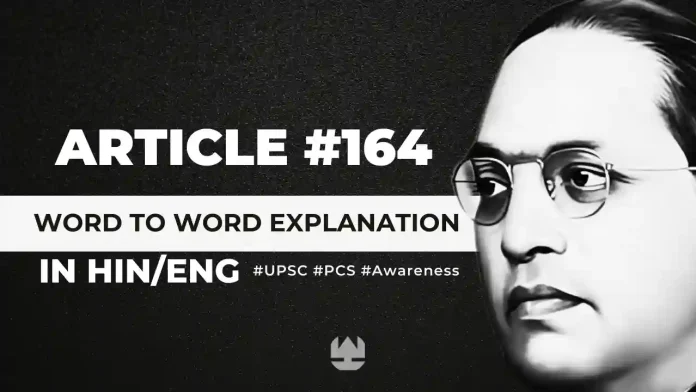Article 164 of the Constitution | अनुच्छेद 164 व्याख्या
यह लेख Article 164 (अनुच्छेद 164) का यथारूप संकलन है। आप इस मूल अनुच्छेद का हिन्दी और इंग्लिश दोनों संस्करण पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें, और MCQs भी सॉल्व करें।
अनुच्छेद 164 (Article 164) – Original
| भाग 6 “राज्य” 164. मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध — (1) मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री, राज्यपाल के प्रसादपर्यत अपने पद धारण करेंगे। परंतु 1 मध्य प्रदेश और 2 राज्यों में जनजातियों के कल्याण का भारसाधक एक मंत्री होगा जो साथ ही अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण का या किसी अन्य कार्य का भी भारसाधक हो सकेगा। 3 (2) मंत्रि-परिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। (3) किसी मंत्री द्वारा अपना पद्ग्रहण करने से पहले, राज्यपाल तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूपों के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। (4) कोई मंत्री, जो निरंतर छह मास की किसी अवधि तक राज्य के विधान-मंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। (5) मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगेहों गेजो उस राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, समय-समय पर अवधारित करे और जब तक उस राज्य का विधान-मंडल इस प्रकार अवधारित नहीं करता है तब तक ऐसे होंगेहों गेजो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। ================== 1. संविधान (चौरानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 2 द्वारा (12-6-2006 से) “बिहार” के स्थान पर प्रतिस्थापित। 2. उड़ीसा (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2011 (2011 का 15) की धारा 4 द्वारा (1-11-2011 से) “उड़ीसा” के स्थान पर प्रतिस्थापित। 3. संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 3 द्वारा (1-1-2004 से) अंतः स्थापित। 4. देखिए अधिसूचना सं. का.आ. 21(अ), तारीख 7-1-2004। |
अनुच्छेद 164 हिन्दी संस्करण
Article 164 English Version
�� Article 164 Explanation in Hindi
भारतीय संविधान का भाग 6, अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक कुल 6 अध्यायों (Chapters) में विस्तारित है (जिसे कि आप नीचे टेबल में देख सकते हैं)।
| Chapters I | Title साधारण (General) | Articles Article 152 |
| II | कार्यपालिका (The Executive) | Article 153 – 167 |
| III | राज्य का विधान मंडल (The State Legislature) | Article 168 – 212 |
| IV | राज्यपाल की विधायी शक्ति (Legislative Power of the Governor) | Article 213 |
| V | राज्यों के उच्च न्यायालय (The High Courts in the States) | Article 214 – 232 |
| VI | अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Courts) | Article 233 – 237 |
जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, इस भाग के अध्याय 2 का नाम है “कार्यपालिका (The Executive) और इसका विस्तार अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 167 तक है।
इस अध्याय को तीन उप–अध्यायों में बांटा गया है – राज्यपाल (The Governor), मंत्रि–परिषद (Council of Ministers), राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General of the States) और सरकारी कार्य का संचालन (Conduct of Government Business)।
इस लेख में हम मंत्रि–परिषद (Council of Ministers) के तहत आने वाले अनुच्छेद 164 को समझने वाले हैं। आइये समझें;
⚫ अनुच्छेद 152- भारतीय संविधान
Just Previous to this Article
| अनुच्छेद 164 – मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध (Other Provisions As To Ministers)
भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है यानी कि यहाँ केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार भी होता है और राज्य सरकार की अपनी कार्यपालिका होती है।
राज्य कार्यपालिका के मुख्यतः चार भाग होते है: राज्यपाल (Governor), मुख्यमंत्री (Chief Minister), मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) और राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General of the state)।
प्रधानमंत्री की तरह ही मुख्यमंत्री के लिए भी संविधान में अलग से कोई अनुच्छेद नहीं है। बल्कि अनुच्छेद 163 और 164 से ही यह अपना अस्तित्व रखता है।
राज्यपाल चूंकि संवैधानिक कार्यपालिका होता है और उसी के नाम से सारे कार्यपालक काम किए जाते हैं, ऐसे में अनुच्छेद 163 के तहत उसे सलाह और सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है।
अनुच्छेद 164 अपने पहले वाले अनुच्छेद का ही विस्तार है। यह मंत्रियों से संबंधित कुछ प्रावधान और कॉन्सेप्ट को विस्तार देता है और उसमें स्पष्टता लाता है। अनुच्छेद 164 में कुल 5 खंड है; आइये समझें;
| Article 164(1) Explanation
अनुच्छेद 164(1) के तहत मुख्य रूप से छह बातें कही गई है;
पहली बात) मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा।
मुख्यमंत्री कौन होता है? अनुच्छेद 163 के तहत हमने समझा था कि राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है, उसी का मुखिया होता है मुख्यमंत्री (Chief Minister)।
दूसरी बात) मुख्यमंत्री के अलावे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करेगा लेकिन मुख्यमंत्री के सलाह पर।
तीसरी बात) सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद्पर्यंत अपना पद धारण करते हैं।
Q. राज्यपाल के प्रसाद्पर्यंत (During the Pleasure of the Governor) का क्या मतलब है?
शब्द “राज्यपाल के प्रसाद्पर्यंत” एक कानूनी शब्द है जिसका अर्थ है कि किसी पदाधिकारी को राज्यपाल द्वारा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय पद से हटाया जा सकता है।
इस शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कई संदर्भों में किया जाता है, जिसमें किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति और किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति शामिल है।
“राज्यपाल के प्रसाद्पर्यंत” शब्द का प्रयोग राज्यपाल को इन कार्यालयधारकों पर बहुत अधिक शक्ति प्रदान करता है। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह शक्ति पूर्ण (Absolute) नहीं है।
राज्यपाल बिना किसी कारण के किसी पदाधिकारी को नहीं हटा सकते। राज्यपाल के पास हटाने का वैध कारण होना चाहिए, और निष्कासन कानून के अनुसार होना चाहिए।
चौथी बात) छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्यों में जनजातियों के कल्याण हेतु अलग से एक भारसाधक मंत्री (minister in charge) की व्यवस्था की गई है। जो कि अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण का या किसी अन्य कार्य का भी भारसाधक हो सकेगा।
पहले बिहार राज्य भी इस सूची में हुआ करता था लेकिन साल 2006 में संविधान (चौरानवेवां संशोधन) अधिनियम द्वारा इसे हटा दिया गया।
Q. भारसाधक मंत्री या प्रभारी मंत्री (Minister in Charge) का क्या मतलब है?
शब्द “भारसाधक मंत्री या प्रभारी मंत्री” का उपयोग भारतीय संदर्भ में एक ऐसे मंत्री को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जो सरकार के एक विशेष विभाग के लिए जिम्मेदार होता है।
प्रभारी मंत्री विभाग के समग्र प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है, जिसमें नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन, संसाधनों का आवंटन और अधिकारियों की नियुक्ति शामिल है।
प्रभारी मंत्री आमतौर पर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सत्तारूढ़ दल का सदस्य होता है। मंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सिफारिश पर, जैसा भी मामला हो, राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
प्रभारी मंत्री को विभाग के सचिव, अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव सहित अधिकारियों की एक टीम द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। प्रभारी मंत्री विभाग के कामकाज के लिए विधायिका के प्रति भी जिम्मेदार होता है।
भारतीय संविधान में “प्रभारी मंत्री” शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। हालाँकि, यह एक ऐसा शब्द है जो आमतौर पर भारत सरकार और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों में उपयोग किया जाता है।
प्रभारी मंत्री की भूमिका उस विभाग के आधार पर भिन्न हो सकती है जिसके लिए वह जिम्मेदार है। हालाँकि, प्रभारी मंत्री हमेशा सरकार में एक प्रमुख व्यक्ति होता है और नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
पाँचवी बात) किसी राज्य की मंत्रि-परिषद् में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या बारह से कम नहीं होगी।
उदाहरण के लिए अगर बिहार राज्य को लें तो वहाँ 243 विधान सभा की सीटें है, तो ऐसे में वहाँ पर मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या अधिकतम 36 हो सकती है। और न्यूनतम 12। मूल संविधान में यह शर्तें नहीं थी बल्कि संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा इसे जोड़ा गया है।
विस्तार से समझने के लिए पढ़ें – 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003
छठी बात) इसे अनुच्छेद 164(1B) के तहत रखा गया है। और इसके तहत मंत्रियों या सदस्यों के लिए दल-बदल की स्थिति में अयोग्यता संबंधी कुछ प्रावधान जोड़े गए है।
यह भाग हमेशा से संविधान का हिस्सा नहीं था बल्कि 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसे जोड़ा गया है। यहाँ दो बातें समझने वाली है;
अनुसूची 10 के पैरा 2 के तहत दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता (disqualification) का प्रावधान किया गया है। इसके तहत बताया गया है कि संसद अथवा किसी राज्य विधानमंडल का कोई निर्वाचित सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुआ है, दल-परिवर्तन के आधार पर अयोग्य होगा –
यदि वह स्वेच्छा से उस राजनैतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है, या
यदि वह उस सदन में मतदान के दौरान अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मत देता है या फिर मत देता ही नहीं है, और इसके लिए वह राजनीतिक दल से पंद्रह दिनों के भीतर क्षमादान भी न पाता हो।
संसद या राज्य विधानमंडल का कोई निर्दलीय सदस्य किसी सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाएगा यदि वह उस चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है।
संसद अथवा राज्य विधानमंडल का कोई मनोनीत सदस्य, जो अपने मनोनीत होने के समय किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं है और जो अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से छह माह की अवधि समाप्त होने से पूर्व किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य बना है, उस सदन की सदस्यता के अयोग्य हो जाएगा यदि वह उस सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के छह माह बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है।
राज्य विधानमंडल का सदस्य या विधान परिषद का सदस्य (अगर हो तो) जो कि किसी राजनीतिक दल से संबंध रखता है अगर वो ऊपर बताए गए किसी व्यवस्था के तहत अयोग्य घोषित किया जाता है तो वह मंत्री नहीं बन सकता है। और तब तक नहीं बन सकता है जब तक उसकी पदावधि समाप्त नहीं हो जाती है।
दल–बदल यानि कि Anti-defection को विस्तार से समझने के लिए पढ़ें – दल–बदल कानून (Anti-defection Law) क्या है?
| Article 164(2) Explanation
अनुच्छेद 164(2) के तहत कहा गया है कि मंत्रि-परिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। कहने का अर्थ है कि मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री सीधे जनता के प्रति उत्तरदायी होता है।
Q. सामूहिक रूप से उत्तरदायी (Collectively responsible) होने का क्या मतलब है?
सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective Responsibility) सरकार की संसदीय प्रणाली का एक सिद्धांत है जिसके तहत संपूर्ण कैबिनेट अपने व्यक्तिगत सदस्यों के कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जिम्मेदार होता है।
इसका मतलब यह है कि यदि कोई मंत्री कानून या सरकार की नीतियों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो पूरा मंत्रिमंडल जिम्मेदार है और उसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा सकता है।
सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) और अनुच्छेद 164(2) में निहित है, जिसमें कहा गया है कि “मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा और राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी”।
सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कई कारणों से महत्वपूर्ण है।
◾ सबसे पहले, यह सुनिश्चित करता है कि सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है।
◾ दूसरा, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत सरकार में स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद करता है। यदि व्यक्तिगत मंत्री अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, तो उनके जोखिम लेने या अलोकप्रिय निर्णय लेने की अधिक संभावना हो सकती है।
◾ तीसरा, सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि सरकार एकजुट है।
| Article 164(3) Explanation
अनुच्छेद 164(3) के तहत बताया गया है कि किसी मंत्री द्वारा अपना पदहण करने से पहले, राज्यपाल तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूपों के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा।
जब कोई कोई मंत्री अपना पद ग्रहण करता है तो उससे पहले उसे दो शपथ (पद और गोपनियता) लेनी पड़ती है। यह शपथ राज्यपाल द्वारा दिलवाई जाती है। शपथ में क्या कहा जाएगा यह अनुसूची 3 में लिखा हुआ है;
अनुसूची 3 के अनुसार राज्य के मंत्री के लिए पद की शपथ:
“मैं, …………….. ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं …………….. राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अन्तःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। “
“I, …….., do swear in the name of God/solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the State of ……….and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favour, affection or ill-will.”
अनुसूची 3 के अनुसार राज्य के मंत्री के लिए गोपनीयता की शपथ:
“मैं, …………….. ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय ………….राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।”
“I, …….., do swear in the name of God/solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the State of ………………..except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister.”
| Article 164(4) Explanation
अनुच्छेद 164(4) के तहत बताया गया है कि कोई मंत्री, जो निरंतर छह मास की किसी अवधि तक राज्य के विधान-मंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा।
कहने का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति बिना सदन का सदस्य बने छह माह तक मुख्यमंत्री या मंत्री बना रह सकता है। अगर उसे आगे भी मंत्री बने रहना है तो छह माह के अंदर विधानमंडल का सदस्य बनना पड़ेगा। अगर नहीं बनता है तो उसकी पद समाप्त हो जाएगी।
| Article 164(5) Explanation
अनुच्छेद 164(5) के तहत कहा गया है कि मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगेहों गेजो उस राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, समय-समय पर अवधारित करे और जब तक उस राज्य का विधान-मंडल इस प्रकार अवधारित नहीं करता है तब तक ऐसे होंगेहों गेजो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।
कहने का अर्थ यह है कि राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्ते क्या होंगेहों गेइसका निर्धारण राज्य विधानमंडल को ही विधि बनाकर करना है। सभी राज्यों ने ऐसा कानून बना रखा है जिसके तहत वो अपने मंत्रियों को वेतन और भत्ता देता है।
Important Facts Related to Article 163 and 164
◾ संविधान में मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएँ स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई हैं। अनुच्छेद 164 के अनुसार, राज्यपाल ही मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्ति करने का प्रभारी होगा।
हालांकि इसका यह मतलब नहीं होता है कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर देगा। राज्यपाल, आम चुनाव में बहुमत प्राप्त दल के स्वीकार्य नेता को ही मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है।
◾ अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि किसी मंत्री का कार्यकाल राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर होता है। यानि कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद्पर्यंत काम करता है।
हालांकि इसका यह मतलब नहीं होता है कि राज्यपाल जब चाहे किसी मंत्री को निकाल सकता है सरकार गिरा सकता है। राज्यपाल ऐसा तभी करता है जब कोई दल बहुमत खो देता है या फिर मुख्यमंत्री ऐसा करने को कहता है।
◾ Har Sharan Verma vs. Tribhuvan Narain Singh मामले में यह स्पष्ट हुआ था कि एक मुख्यमंत्री छह महीने की अवधि तक सेवा कर सकता है, भले ही वह राज्य विधायिका (state legislature) का सदस्य न हों।हों
आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को सुवेन्दु अधिकारी से हारने के बावजूद भी मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। और छह माह का समय दिया गया। और ममता बनर्जी छह महीने के अंदर चुनाव जीत कर पूरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बन गई।
◾ अनुच्छेद 164 और 75 को आप एक साथ पढ़ सकते हैं क्योंकिक्यों अनुच्छेद सेम यही बात संघ के लिए कहती है। हालांकि वहाँ मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री होता है।
तो यही है अनुच्छेद 164, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
◾ राज्यों के मुख्यमंत्री (Chief Minister of States)
◾ प्रधानमंत्री (Prime minister)
◾ केन्द्रीय मंत्रिपरिषद (Council of Ministers)
◾ राज्यों के राज्य मंत्रिपरिषद (State Council of Minister)
Must Read
सवाल–जवाब के लिए टेलीग्राम जॉइन करें; टेलीग्राम पर जाकर सर्च करे – @upscandpcsofficial
MCQs with Explanation
Q. What does Article 164 of the Indian Constitution deal with?
The appointment of the chief minister of a State.
The powers of the Governor to grant pardons, reprieves, and remissions of punishment. The Council of Ministers to aid and advise the Governor.
The qualifications for appointment as the Governor of a State.
Explanation: The correct answer is (a). Article 164 of the Indian Constitution deals with the appointment of the chief minister of a State.
Q. Who is the head of the Council of Ministers in a State?
The Governor.
The Chief Minister.
The Prime Minister.
The Speaker of the Legislative Assembly.
Explanation: The correct answer is (b). The Chief Minister is the head of the Council of Ministers in a State.
Q. How many ministers can be appointed in the Council of Ministers in a State? There is no limit on the number of ministers that can be appointed in the Council of Ministers in a State.
The total number of Ministers, including the Chief Minister, in the Council of Ministers in a State shall not exceed fifteen per cent of the total number of members of the Legislative Assembly of that State
The number of ministers that can be appointed in the Council of Ministers in a State is determined by the Chief Minister.
The number of ministers that can be appointed in the Council of Ministers in a State is determined by the Legislative Assembly.
Explanation: The correct answer is (b). The total number of Ministers, including the Chief Minister, in the Council of Ministers in a State shall not exceed fifteen per cent of the total number of members of the Legislative Assembly of that State
Q. What happens if the Council of Ministers loses the confidence of the Legislative Assembly in a State?
The Council of Ministers has to resign.
The Governor can dissolve the Legislative Assembly.
The President can dismiss the Governor.
The Chief Minister can ask the President to impose President’s Rule in the State.
Explanation: The correct answer is (a). if the Council of Ministers loses the confidence of the Legislative Assembly in a State, the Council of Ministers has to resign.
Q. How is the Chief Minister appointed according to Article 164?
A) By the President of India
B) By the Governor of the State
C) By the Prime Minister
D) By the Chief Justice of India
Explanation: Correct Answer: B) By the Governor of the State
According to Article 164, the Chief Minister of a State is appointed by the Governor of the State. The Governor usually appoints the leader of the political party or coalition that has the majority of seats in the State Legislative Assembly.
| Related Article
⚫ अनुच्छेद 165 – भारतीय संविधान
⚫ अनुच्छेद 163 – भारतीय संविधान
Related to Article 160
अस्वीकरण – यहाँ प्रस्तुत अनुच्छेद और उसकी व्याख्या, मूल संविधान (उपलब्ध संस्करण), संविधान पर डी डी बसु की व्याख्या (मुख्य रूप से), प्रमुख पुस्तकें (एम. लक्ष्मीकान्त, सुभाष कश्यप, विद्यु त चक्रवर्ती, प्रमोद अग्रवाल इत्यादि) एनसाइक्लोपीडिया, संबंधित मूल अधिनियम और संविधान के विभिन्न ज्ञाताओं (जिनके लेख समाचार पत्रों,त्रों पत्रिकाओं एवं इंटरनेट पर ऑडियो-विजुअल्स के रूप में उपलब्ध है) पर आधारित है। हमने बस इसे रोचक और आसानी से समझने योग्य बनाने का प्रयास किया है।