भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के साथ-साथ भारत के महान्यायवादी भी कार्यपालिका (executive) होते हैं।
इस लेख में हम भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India) पर सरल और सहज चर्चा करेंगे एवं इसके विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को समझेंगे,
तो अच्छी तरह से समझने के लिए लेख को अंत तक जरूर पढ़ें, साथ ही संबंधित अन्य लेख भी पढ़ें। Link is given below;
| Central Council of Ministers | Click Here |
| Cabinet Committee | Click Here |
| Chief Minister of Indian States | Click Here |
| Governor | Click Here |

| 📖 Read in English |
भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India)
संघ के स्तर पर मुख्यतः 5 कार्यपालिका होते हैं। राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केन्द्रीय मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India)।
दरअसल जब भी लॉ डिग्रीधारी अधिवक्ता (Advocate) बन जाता है यानी कि किसी की तरफ से केस लड़ने के योग्य हो जाता है तो फिर आगे वो व्यक्ति इस क्षेत्र में बहुत कुछ बन सकता है; जैसे कि यदि वो न्यायालय में राज्य की तरफ से किसी पीड़ित का पक्ष लेता है तो उसे लोक अभियोजक (Public prosecutor) कहा जाता है।
यदि वो व्यक्ति न्यायालय में न्यायालय में राज्य सरकार की तरफ से खड़ा होता है तो उसे राज्य का महाधिवक्ता (Advocate General of State)↗️ कहा जाता है।
यदि वो व्यक्ति न्यायालय में केंद्र सरकार की तरफ से खड़ा होता है तो उसे महान्यायवादी (Attorney General) कहा जाता है। (इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं।)
इसी महान्यायवादी के सहायक (Assistant) के रूप में काम करने वाले को अधिकारी को महा याचक/ महा न्यायभिकर्ता (solicitor general) कहते हैं।
भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India) दरअसल देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। संविधान में अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है। यानी कि ये एक संवैधानिक पद है।
भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति एवं कार्यकाल
अनुच्छेद 76(1) के अनुसार भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India) की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो।
दूसरे शब्दों में कहें तो भारत के महान्यायवादी में उन योग्यताओं का होना आवश्यक होता है जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होता है; यानी कि
(1) वह भारत का नागरिक हो,
(2) उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का पाँच वर्षों का अनुभव हो या किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव हो, या
(3) राष्ट्रपति के नज़र वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो।
महान्यायवादी का कार्यकाल
◼ संविधान में महान्यायवादी के कार्यकाल को लेकर कोई निश्चित व्यवस्था नहीं किया गया है। इसके साथ ही संविधान में उसको हटाने को लेकर भी कोई मूल व्यवस्था नहीं दी गई है। हालांकि अनुच्छेद 76(4) में ये बताया गया है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद्पर्यंत पद धारण करेगा इसके साथ ही वेतन और भत्ते भी वही प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति तय करेगा।
इसका तात्पर्य यह है कि महान्यायवादी को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। या फिर वो खुद भी चाहे तो राष्ट्रपति को कभी भी अपना त्यागपत्र सौंपकर पदमुक्त हो सकता है।
वैसे परंपरा ये है कि जब सरकार त्यागपत्र दे दे या फिर वो गिर जाये तो उसे त्यागपत्र देना होता है क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सिफ़ारिश से ही होती है। फिर जब नया सरकार बनेगा तब वो जो सिफ़ारिश करेगा वो भारत का महान्यायवादी बनेगा।
महान्यायवादी की कार्य एवं शक्तियाँ
भारत सरकार के मुख्य कानून अधिकारी के रूप में महान्यायवादी के निम्नलिखित कर्तव्य हैं:-
1. भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौपे गए हो
2. संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करें।
राष्ट्रपति भी महान्यायवादी को कार्य सौंपता है जैसे कि –
1. भारत सरकार से संबन्धित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना।
2. संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत, राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना।
3. सरकार से संबन्धित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार।
◼ भारत के किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों मे बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। हालांकि वो वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। एक संसद सदस्य की तरह महान्यायवादी को भी सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार मिलते है।
भारत के महान्यायवादी की सीमाएं
महान्यायवादी की निम्नलिखित सीमाएं भी है ताकि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं उसके बीच स्पष्ट अंतर रहे।
1. वह भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता
2. जिस मामले में उसे भारत की ओर से पेश होना है, उस पर वह कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है
3. बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है
4. बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी परिषद या कंपनी के निदेशक का पद ग्रहण नहीं कर सकता है।
महान्यायवादी से जुड़े अन्य तथ्य
महान्यायवादी के अतिरिक्त भी भारत सरकार के अन्य कानूनी अधिकारी होते हैं। इसमें एक Solicitor General of India एवं 4 Additional Solicitors General for India होते हैं। ये लोग महान्यायवादी को उसकी ज़िम्मेदारी पूरी करने में सहायता करते हैं।
यहाँ एक बात ध्यान में रखिए कि महान्यायवादी का पद एक संवैधानिक पद है जिसका कि अनुच्छेद 76 में उल्लेख किया गया है। वहीं Solicitor General of India एवं Additional Solicitors General for India की बात करें तो संविधान में उसकी चर्चा नहीं की गयी है।
◼ कहने को तो इसे कार्यपालक की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है। सरकारी स्तर पर विधिक मामलों को देखने के लिय केन्द्रीय कैबिनेट (cabinet) में एक अलग से विधि मंत्री (Law minister) होता है। जबकि अमेरिका के महान्यायवादी को कार्यकारी प्राधिकार भी होता है।
महान्यायवादियों की सूची
| महान्यायवादी | कार्यकाल | उस समय के प्रधानमंत्री |
|---|---|---|
| एम सी सीतलवाड | 28 Jan 1950 – 1 Mar 1963 | जवाहरलाल नेहरू |
| सी के दफतरी | 2 Mar 1963 – 30 Oct 1968 | जवाहरलाल नेहरू; लाल बहादुर शास्त्री |
| नीरेन डे | 1 Nov 1968 – 31 Mar 1977 | इन्दिरा गांधी |
| एस वी गुप्ते | 1 Apr 1977 – 8 Aug 1979 | मोरारजी देशाई |
| एल एन सिन्हा | 9 Aug 1979 – 8 Aug 1983 | इन्दिरा गांधी |
| के परासरण | 9 Aug 1983 – 8 Dec 1989 | इन्दिरा गांधी; राजीव गांधी |
| सोली सोराबजी | 9 Dec 1989 – 2 Dec 1990 | वी पी सिंह ; चन्द्रशेखर |
| जी रामास्वामी | 3 Dec 1990 – 23 Nov 1992 | चन्द्रशेखर; पी वी नरसिम्हाराव |
| मिलन के बनर्जी | 21 Nov 1992 – 8 July 1996 | पी वी नरसिम्हा राव |
| अशोक देशाई | 9 July 1996 – 6 April 1998 | एच डी देवगौड़ा; इंद्र कुमार गुजराल |
| सोली सोराबजी | 7 April 1998 – 4 June 2004 | अटल बिहारी बाजपेयी |
| मिलन के बनर्जी | 5 June 2004 – 7 June 2009 | मनमोहन सिंह |
| गूलम इस्साजी वेहनवती | 8 June 2009 – 11 June 2014 | मनमोहन सिंह |
| मुकुल रोहतगी | 19 June 2014 – 18 June 2017 | नरेंद्र मोदी |
| के के वेणुगोपाल | 1 July 2017 – 30 Sep 2022 | नरेंद्र मोदी |
| आर वेंकटरमन | 1 Oct 2022 – Incumbent | नरेंद्र मोदी |
कुल मिलाकर यही है भारत के महान्यायवादी (Attorney-General for India), उम्मीद है समझ में आया होगा। नीचे अन्य लेखों का लिंक है उसे भी अवश्य पढ़ें।
भारत के महान्यायवादी प्रैक्टिस क्विज यूपीएससी
◼◼◼
Vice President of india explained in hindi
Central Council of Ministers explained in hindi

![Lok Sabha : UPSC Concept [लोकसभा बेसिक कॉन्सेप्ट]](https://wonderhindi.com/wp-content/uploads/2020/10/लोकसभा.jpg)
![संसदीय समितियां (भाग 2) । स्थायी समितियां [UPSC]](https://wonderhindi.com/wp-content/uploads/2020/10/स्थायी-समितियां.jpg)
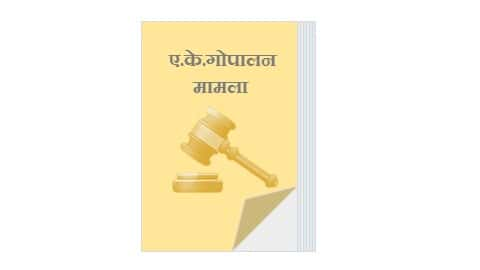
![राज्यपाल : संवैधानिक प्रावधान, नियुक्ति, इत्यादि [UPSC]](https://wonderhindi.com/wp-content/uploads/2020/08/Governor.jpg)