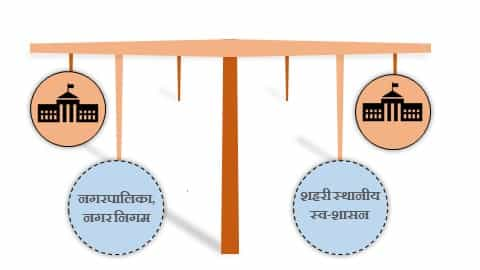जब हम संसद की बात करते हैं तो उसका मतलब ही होता है लोकसभा (Lok Sabha), राज्यसभा (Rajya Sabha)और राष्ट्रपति (President)। यानी कि यही तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं,
इसीलिए संसद को समझने के लिए इन तीनों को समझना जरूरी है। तीनों को अलग-अलग लेख में कवर किया गया है, सभी को पढ़ें।
इस लेख में हम लोकसभा (Lok Sabha) पर सरल और सहज चर्चा करेंगे, एवं इसके विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे।

| 📌 Join YouTube | 📌 Join FB Group |
| 📌 Join Telegram | 📌 Like FB Page |
| 📖 Read in English |
लोकसभा (Lok Sabha) क्या है?
लोकसभा आम जनों की एक सभा है जहां प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं। प्रत्येक प्रतिनिधि किसी खास भौगोलिक क्षेत्र से चुनकर आते हैं जिसे निर्वाचन क्षेत्र (constituency) कहा जाता है।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जनसंख्या के आधार पर आवंटित किया गया एक खास भौगोलिक क्षेत्र है। जीते हुए उम्मीदवार किसी खास निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और संसद में बैठकर विधायी या कार्यकारी प्रक्रिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
प्रत्येक सदस्य को सांसद (Member of Parliament) कहा जाता है (जिसकी संख्या वर्तमान में 543 है) और ये सारे सांसद मिलकर विधायिका (legislature) कहलाते हैं।
इन्ही सांसदों में से किसी एक व्यक्ति का चुनाव करके लोकसभा अध्यक्ष (speaker) बना दिया जाता है, जो कि लोकसभा व उसके प्रतिनिधियों का मुखिया होता है और लोकसभा के कार्य संचालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
आम चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त दल वाले राजनैतिक पार्टी के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री अपनी पार्टी से कुछ सांसदों का चुनाव करके उसे विभिन्न मंत्रालयों का कार्य-भार सौंप देते है।
इन मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद (council of ministers) कहा जाता है और यही होते है वास्तविक कार्यपालिका (Real executive) या सरकार।
लोकसभा की संरचना (Composition of Lok Sabha):
लोकसभा की संरचना से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 81 में मिलता है। लोकसभा (जिसे कि निचला सदन भी कहा जाता है) का गठन वयस्क मतदान के आधार पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने गए के प्रतिनिधियों से होता है।
संविधान में लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है जिसमें से 530 प्रतिनिधि राज्यों के लिए और 20 प्रतिनिधि केंद्रशासित प्रदेशों के लिए है। इसके साथ ही 2 एंग्लो-इंडियन समुदाय के सदस्य की भी व्यवस्था की गई थी।
जनवरी 2020 तक की स्थिति को देखें तो लोकसभा में 545 सदस्य हुआ करता था। जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से चुन कर आते थे और राज्यों से चुनकर आने वाले सदस्यों का कोटा भी 530 ही है, 13 सदस्य केंद्रशासित प्रदेशों से चुनकर आते थे लेकिन केंद्रशासित प्रदेशों से चुनकर आने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या 20 है यानी कि 7 सदस्य अभी चुनकर नहीं आते थे। और दो सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित या नाम निर्देशित एंग्लो-इंडियन समुदाय से आते थे।
? एंग्लो-इंडियन का कॉन्सेप्ट को जनवरी 2020 में 104th संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा खत्म दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अब राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो-इंडियन को नामित नहीं किया जाएगा। [एंग्लो-इंडियन को समझें]
अभी कि बात करें तो 530 सदस्य राज्यों से चुनकर पहले की तरह ही आते हैं, और 20 केंद्रशासित प्रदेशों की सीटों में से 13 सदस्य पहले की ही तरह चुनकर आते हैं, तो अभी कुल 543 सीटें लोकसभा में हैं यानी कि 543 सदस्य अभी लोकसभा में हैं।
[आपके मन में सवाल आ सकता है कि अब तो जम्मू-कश्मीर भी केंद्रशासित प्रदेश हो गया है तो इसको कैसे मैनेज किया जाएगा? तो इस पर अभी के लिए कोई स्पष्टता नहीं है, अभी वहाँ पर परिसीमन का काम भी चल रहा है तो आने वाले समय में जरूर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा।]
| लोकसभा की संरचना को गहराई से समझने के लिए पढ़ें – Article 81 (अनुच्छेद 81)
लोकसभा की विशेषता (Features of Lok Sabha):
लोकसभा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये जनता कि सभा है यानी जनता प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करके यहाँ भेजते हैं।
भारत के हर नागरिक को जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और जिसे संविधान या किसी विधि के उपबंधों के मुताबिक अयोग्य नहीं ठहराया गया हो, मत देने का अधिकार प्राप्त है।
1988 से पहले तक वोट देने की उम्र 21 वर्ष हुआ करता था पर 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा मत देने की आयु सीमा को 18 वर्ष कर दिया गया।
इसके अलावे भी इसकी कई विशेषताएँ हैं जो कि निम्नलिखित है:
लोकसभा की चुनाव प्रणाली
लोकसभा चुनाव प्रणाली से संबन्धित विभिन्न पहलू इस प्रकार है:
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र – जैसा कि ऊपर भी बताया है कि लोकसभा के प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कैसे विभाजित किया गया है; इस संबंध में संविधान में दो उपबंध हैं जो कि अनुच्छेद 81(2) में वर्णित है।
(क). लोकसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य को ऐसी रीति से किया जाएगा कि सीटों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथा साध्य एक ही हो।
इसका मतलब ये है कि अगर बिहार में 40 सीटें है तो उसकी एक सीट लगभग उतने ही लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जितना कि उत्तर-प्रदेश का (जहां पर 80 सीटें है)।
आप चाहे तो इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जनसंख्या 1971 वाली लेनी है और 2026 तक यही काम करेगा।
पहले तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्यों को लोकसभा में सीटों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन को वर्ष 2000 तक 1971 के जनगणना के आधार पर फिक्स कर दिया गया।
इस प्रतिबंध को 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा 25 वर्ष और बढ़ाकर 2026 तक फिक्स कर दिया गया। यानी कि 2026 तक जिस राज्य कि अभी जो स्थिति है वही रहेगी, और 1971 वाला जनसंख्या के आधार पर ही चलेगा।
(यहाँ पर एक बात याद रखिए कि यह उपबंध उन राज्यों पर लागू नहीं होता जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है।)
◾ 1971 वाला जनसंख्या क्यों लिया जाता है, वर्तमान वाला क्यों नहीं इसे राष्ट्रपति चुनाव वाले लेख में अच्छे से समझाया है, आप उसे जरूर पढ़ें।
(ख). प्रत्येक राज्य को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में इस तरह से विभाजित किया गया है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसके लिए आवंटित सीटों की संख्या के बीच का अनुपात पूरे राज्य में यथा साध्य एक ही हो। (एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक ही सीट का आवंटन होता है)
नोट- साल 2000 तक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए भी 1971 के जनगणना का ही प्रयोग किया जाता था। (42वें संविधान संशोधन के कारण) लेकिन 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इसे 1991 की जनगणना पर शिफ्ट कर दिया गया। पुनः 2003 में 87वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसे 2001 के जनगणना पर शिफ्ट कर दिया गया।
इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हो सकता है कि 1971 के बाद किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या दूसरे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के तुलना में बढ़ गया हो या घट गया हो।
तो ऐसी स्थिति में राज्य के अंदर ही उन सभी निर्वाचन क्षेत्रों को 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित किया जा सकता है, ताकि सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या यथासाध्य एक ही हो जाए।
| अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो यह लेख पढ़ें – Article 81 (अनुच्छेद 81)
आनुपातिक प्रतिनिधित्व न अपनाना
राज्यसभा की बात करें तो वहाँ निर्वाचन के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाया गया लेकिन इस प्रणाली को लोकसभा में नहीं अपनाया गया। बल्कि इसकी जगह, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (territorial representation system) को निर्वाचन का आधार बनाया गया।
प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत, कई निर्वाचन क्षेत्र होते है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है। कई प्रत्याशी उस क्षेत्र के लिए चुनाव लड़ते हैं, जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक मत प्राप्त होता हैं, उसे विजयी घोषित किया जाता है।
इस पद्धति की कई खामियाँ भी है। जैसे कि अगर 9 प्रत्याशी है और मान लें कि कुल 100 वोट है। अगर 8 को 11-11 वोट मिले हो और 9वें व्यक्ति को 12 वोट तब भी विजेता वही कहलाएगा, इसका मतलब ये हुआ 100 लोगों में से सिर्फ 12 लोग 9वें व्यक्ति को पसंद करता है फिर भी वह पूरे 100 का प्रतिनिधित्व करेगा।
इसके अलावा इस व्यवस्था में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की कोई गारंटी नहीं होती है जबकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में कम से कम ये समस्याएं नहीं है।
इस व्यवस्था के तहत लोगों के सभी वर्गों को अपनी संख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलता है। यहाँ तक की अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व भी यहाँ सुरक्षित होता है।
फिर सवाल आता है कि हमने आनुपातिक प्रतिनिधित्व को क्यों नहीं अपनाया? दरअसल संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने लोकसभा सदस्यों के चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की ही वकालत की थी लेकिन इसे मूलतः दो कारणों से नहीं अपनाया गया।
1. आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बहुत ही जटिल प्रणाली है और उस समय देश में साक्षरता दर भी कम था तो लोग इस प्रणाली को समझ ही नहीं पाते कि कैसे क्या होता है? आज भी पढे-लिखे लोग भी इसे ठीक से समझ नहीं पाते हैं।
2. बहुदलीय व्यवस्था के कारण संसद की अस्थिरता का खतरा उत्पन्न हो सकता था।
इसके अलावा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के कई दोष भी है :-
1. यह काफी खर्चीली व्यवस्था है और यहाँ उप-चुनाव कोई गुंजाइश बचती नहीं है,
2. यह मतदाताओं एवं प्रतिनिधियों के बीच आत्मीयता को कम करती है,
3. यह पार्टी व्यवस्था के महत्व को तो बढ़ावा देती है लेकिन मतदाताओं के महत्व को कम करती है।
अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण –
अभी हमने ऊपर पढ़ा कि प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली में अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है इसी को खत्म करने के लिए जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई है।
हालांकि अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई है लेकिन उनका निर्वाचन, निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं दारा किया जाता है। अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों को सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने का अधिकार हैं।
84वें संशोधन अधिनियम, 2001 में आरक्षित सीटों को 1991 की जनगणना के आधार पर पुनः नियत किया गया (सामान्य सीटों की तरह)। 87वें संशोधन अधिनियम 2003 में आरक्षित सीटों को 1991 की बजाय 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः नियत किया गया।
लोकसभा की अवधि
राज्यसभा से अलग, लोकसभा जारी रहने वाली संस्था नहीं है। सामान्य तौर पर इसकी अवधि आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से पाँच वर्ष के लिए होती है, इसके बाद यह खुद विघटित हो जाती है।
हालांकि राष्ट्रपति को पाँच साल से पहले किसी भी समय इसे विघटित करने का अधिकार है। इसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती ।
इसके अलावा लोकसभा की अवधि आपात की स्थिति में एक बार में एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। लेकिन इसका विस्तार किसी भी दशा में आपातकाल खत्म होने के बाद छह महीने की अवधि से अधिक नहीं हो सकता।
समापन टिप्पणी
लोकसभा भारतीय संसदीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण संस्था है। यह लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करने, कानूनों को शुरू करने और पारित करने, बजट को मंजूरी देने और सरकार को उसकी नीतियों और कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए जिम्मेदार है।
लोकसभा में कई अनूठी विशेषताएं हैं, जैसे अध्यक्ष, कोरम, मतदान प्रक्रिया और समितियां। प्रश्नकाल और वाद-विवाद सहित इसकी कार्यवाही, सांसदों को चिंताओं को उठाने और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करती है।
अध्यक्ष (Speaker) : लोकसभा का अध्यक्ष सदन का पीठासीन अधिकारी होता है और सदस्यों द्वारा चुना जाता है। वह सदन में व्यवस्था बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि सदन का काम निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से संचालित हो। [विस्तार से समझने लिए पढ़ें – लोकसभा अध्यक्ष: शक्ति व कार्य]
कोरम (Quorum): लोकसभा की एक बैठक के लिए कोरम सदन की कुल सदस्यता का दसवां हिस्सा है, जो वर्तमान में 55 सदस्य हैं।
मतदान (voting): लोकसभा में अधिकांश निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा लिए जाते हैं। हालाँकि, कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत। [विस्तार से समझें; संसद में मतदान की प्रक्रिया]
मुख्य भूमिका (Main Role): लोकसभा देश की विधायी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके पास बिलों को शुरू करने और पारित करने, बजट को मंजूरी देने और अपनी नीतियों और कार्यों के लिए सरकार को जवाबदेह ठहराने की शक्ति है। [विस्तार से समझें; संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया]
प्रश्नकाल (Question Hour): प्रत्येक लोकसभा सत्र का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए आरक्षित होता है, जिसके दौरान संसद सदस्य (सांसद) सरकार और उसके मंत्रियों से नीतियों, कार्यक्रमों और निर्णयों के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। [विस्तार से समझें; प्रश्नकाल एवं शून्यकाल]
समितियाँ (Committees): लोकसभा में कई समितियाँ हैं, जिनमें स्थायी समितियाँ शामिल हैं, जो विभिन्न सरकारी मंत्रालयों के बजट और नीतियों की जाँच करती हैं, और संसदीय समितियाँ, जो विशिष्ट मुद्दों की जाँच करती हैं और सदन को सिफारिशें देती हैं। [विस्तार से समझें: संसदीय समितियां (अर्थ, प्रकार, समझ)]
कुल मिलाकर, लोकसभा देश के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि सरकार अपने नागरिकों के सर्वोत्तम हित में काम करती है।
इस लेख के माध्यम से लोकसभा (Lok Sabha) की बेसिक्स को क्लियर करने की कोशिश की गई है। लोकसभा अध्यक्ष और इसके साथ ही संसद से जुड़े अन्य लेखों का लिंक नीचे और ऊपर दिया गया है, अच्छी समझ के लिए उसे भी पढ़ें।

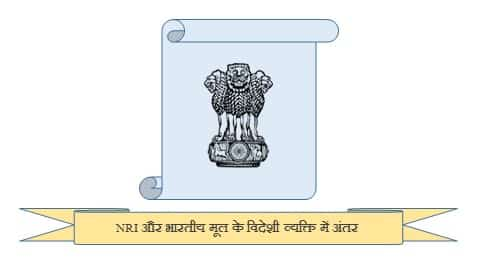
![Powers of Governor in Hindi [राज्यपाल की शक्तियां]](https://wonderhindi.com/wp-content/uploads/2020/08/राज्यपाल-शक्तियाँ.jpg)
![शहरी स्थानीय शासन के प्रकार एवं अन्य तथ्य [UPSC]](https://wonderhindi.com/wp-content/uploads/2021/02/शहरी-स्थानीय-शासन-के-प्रकार-.jpg)