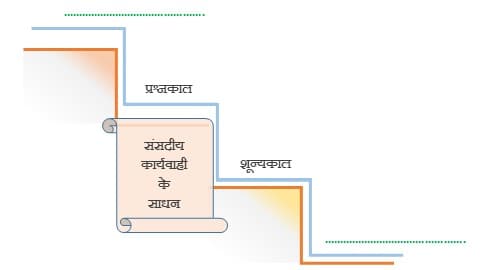इस लेख में पेसा अधिनियम 1996 (PESA Act 1996) पर सरल और सहज चर्चा करेंगे, एवं इसके विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे।
ये लेख पंचायती राज व्यवस्था (Panchayati Raj system) का ही एक भाग है, इसे समझने से पहले उस पंचायती व्यवस्था को जरूर समझ लें।
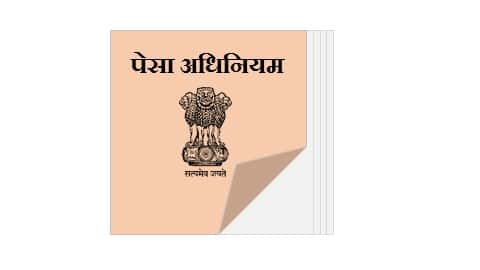
| 📖 Read in English |
पेसा अधिनियम 1996 की पृष्ठभूमि
1992 में भारतीय संसद ने संविधान में ऐतिहासिक 73वां संशोधन अधिनियम पारित किया जिसके अंतर्गत प्रतिनिधि शासन का तीसरा स्तर बनाया गया था।
प्रतिनिधि शासन का दो रूप केंद्र और राज्य पहले से मौजूद था, इस संविधान संशोधन के माध्यम से एक तीसरा स्तर जोड़ा गया जिसे पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। इसके कार्यकारी क्षेत्र आदि को जगह देने के लिए संविधान में एक नई ग्यारहवीं अनुसूची भी बनाया गया।
पर सवाल ये था कि इन सब व्यवस्थाओं से जनजातियों या आदिवासियों का क्या होगा? क्योंकि पंचायतों से संबन्धित संविधान का जो भाग 9 है वो संविधान के पाँचवी अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है।
भारत में चल रही आधुनिक विकास की परिकल्पना ने अगर किसी समुदाय को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है तो वह इस देश का आदिवासी या जनजातीय समाज है। अपने जल-जंगल-जमीन से लगातार बेदखली ने आदिवासियों के जीवन के संकट को उतरोत्तर बढ़ाया है।
आदिवासियों के साथ हो रहे इस अन्याय व अत्याचार से बढ़ते जन असंतोष और सरकार पर बन रहे दबाव के चलते संसद ने दिसम्बर 1996 में पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम पारित किया और जनजातियों की विशेष स्थिति एवं आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन एवं अपवाद के साथ संविधान के भाग 9 को पाँचवी अनुसूची के अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित कर दिया। इसलिए इसे विस्तार अधिनियम भी कहा जाता है।
तो कुल मिलाकर पेसा अधिनियम 1996 (PESA Act 1996) आदिवासियों के रीति-रिवाजों, परंपराओं और जीवन-शैली को कायम रखते हुए सत्ता और विकास की बागडोर उसी के हाथ में सौंप दिया।
आदिवासी इलाके आजादी के पहले भी स्वतंत्र थे। वहाँ, अंग्रेजों का शासन-प्रशासन नहीं था। तब इन इलाकों को बहिष्कृत और आंशिक बहिष्कृत की श्रेणी में रखा गया। 1947 में आजादी के बाद जब 1950 में संविधान लागू हुआ तो इन क्षेत्रों को 5वीं और छठी अनुसूची में वर्गीकृत किया गया।
जो पूर्णतः बहिष्कृत क्षेत्र थे उन्हे छठी अनुसूची में डाला गया। जिसमें पूर्वोत्तर के चार राज्य हैं – त्रिपुरा, मेघालय, असम और मिज़ोरम। और जो आंशिक बहिष्कृत क्षेत्र थे, अंग्रेजों ने वहाँ भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया, उन्ही क्षेत्रों को 5वीं अनुसूचित में डाला गया। इसमें दस राज्य शामिल हैं, मध्य प्रदेश, छतीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश।
वर्तमान में इन्ही 10 राज्यों (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और राजस्थान) में यह अधिनियम लागू होता है।
पेसा अधिनियम 1996 के उद्देश्य
1. संविधान के भाग 9 (जो कि पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है) को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करना तथा जनजातियों की स्वायत्तता के बिंदु स्पष्ट करना, जिनका उल्लंघन करने की शक्ति राज्यों के पास न हो।
2. जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना, पारंपरिक परिपाटियों की सुसंगता (Compatibility) में उपयुक्त प्रशासनिक ढाँचा विकसित करना तथा ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केंद्र बनाना।
3. जनजातीय लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त स्तरों पर पंचायतों को विशिष्ट शक्तियों से युक्त करना एवं उच्च स्तर के पंचायतों को निचले स्तर की ग्राम सभा की शक्तियों एवं अधिकारों को छिनने से रोकना।
पेसा अधिनियम की विशेषताएँ
1. आदिवासी या जनजातीय क्षेत्रों में पंचायतों पर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून वहाँ के प्रथागत क़ानूनों, रीति-रिवाजों, धार्मिक प्रचलनों आदि के अनुरूप होगा।
2. यहाँ गाँव का मतलब अपनी परंपराओं एवं रिवाजों के अनुसार जीवनयापन कर कर रहे एक समुदाय का वास स्थल अथवा वास स्थलों का एक समूह या फिर एक टोला अथवा टोलों का समूह होगा।
3. प्रत्येक गाँव में एक ग्राम सभा होगी जिसमें ऐसे लोग होंगे जिनके नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए निर्वाचक सूची में दर्ज हो।
4. प्रत्येक ग्राम सभा अपने और अपने लोगों की परम्पराओं एवं प्रथाओं, सामाजिक- सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधन तथा विवाद निवारण के परंपरागत तरीकों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए सक्षम होगी।
5. सामाजिक एवं आर्थिक विकास के कार्यक्रमों एवं परियोजना को ग्राम पंचायत द्वारा क्रियान्वित करने से पहले, ग्राम सभा से स्वीकृति लेनी होगी।
6. संविधान के भाग 9 के अंतर्गत जिन समुदायों के संबंध में आरक्षण के प्रावधान हैं, उन्हें अनुसूचित क्षेत्रों के प्रत्येक पंचायत में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन साथ में यह शर्त भी है कि अनुसूचित जनजातियों (scheduled tribes) का आरक्षण कुल स्थानों के 50% से कम नहीं होगा तथा पंचायतों के सभी स्तरों पर अध्यक्षों के पद अनुसूचित जनजाति (scheduled tribe) के लिये आरक्षित रहेंगे।
7. जिन अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व मध्यवर्ती स्तर की पंचायत या जिला स्तर की पंचायत में नहीं है उन्हे सरकार द्वारा नामित (nominated) किया जाएगा। लेकिन नामित सदस्यों की संख्या पंचायत में निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या के 1/10 वें भाग से अधिक नहीं होगी।
8. इन क्षेत्रों में विकास परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के पहले ग्राम सभा अथवा उपयुक्त स्तर की पंचायत से सलाह की जाएगी। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में इन परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के पहले भी ग्राम सभा अथवा उपयुक्त स्तर की पंचायत से सलाह की जाएगी।
9. इन क्षेत्रों में लघु जल स्रोतों के लिए आयोजना एवं प्रबंधन की ज़िम्मेदारी उपयुक्त स्तर के पंचायत को दी जाएगी।
10. अधिसूचित क्षेत्रों मे छोटे स्तर पर खनिजों का खनन संबंधी लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए ग्राम सभा अथवा उपयुक्त स्तर की पंचायत की अनुशंसा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
11. अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत स्वशासन संस्थाओं के तौर पर कार्य कर सके इसके लिये राज्यों के विधानमंडल यह सुनिश्चित करेंगे कि उपयुक्त स्तर पर पंचायत तथा ग्राम सभा को –
(a) किसी भी मादक पदार्थ की बिक्री या उपभोग को प्रतिबंधित या नियमित करने का अधिकार होगा।
(b) छोटे स्तर पर वन उपज पर स्वामित्व होगा।
(c) गाँवों के हाट-बाज़ारों के प्रबंधन की शक्ति होगी।
(d) अनुसूचित जनजातियों को पैसा उधार दिये जाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने की शक्ति होगी।
(e) सभी सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं एवं पदाधिकारियों पर नियंत्रण रखने की शक्ति होगी।
12. राज्य विधानमंडल ऐसी व्यवस्था बनाएगी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्च स्तर की पंचायतें निचले स्तर की किसी पंचायत या ग्राम सभा के अधिकारों का हनन नहीं कर सके।
13. अनुसूचित क्षेत्रो में जिला स्तर पर प्रशासकीय व्यवस्था बनाते समय राज्य विधानमंडल संविधान की छठी अनुसूची को फॉलो करेगी।
अधिनियम से जुड़ी समस्याएँ
◾पेसा अधिनियम के तहत प्रत्येक गाँव में एक ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है, जबकि हम जानते है कि कई स्थितियों में एक ग्राम पंचायत एक से अधिक ग्राम सभाओं द्वारा चुनी जाती है। ऐसे में अगर किसी विषय पर अलग-अलग ग्राम सभाओं का मत अलग-अलग हो तो अंतिम निर्णय कैसे निकाला जाएगा।
◾लघु वन उत्पादों के सम्बन्ध में जो ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है वो भी सीमित है क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा यह व्यवस्था दी गई है कि कोई ग्राम सभा उतने ही वन क्षेत्र के उत्पादों पर अपने अधिकार का दावा कर सकती है जो उसकी राजस्व सीमाओं के भीतर आता है।
◾जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है कि ये अधिनियम सिर्फ उन्ही क्षेत्रों पर लागू होती है जिसका वर्णन अनुसूची 5 में है, ऐसे में दूसरे राज्यों की अनुसूचित जनजातियाँ जो कि संख्या में कम है; इस कानून का लाभ नहीं उठा सकते।
◾इसके अलावा ऐसे क्षेत्रों में नक्शलवाद आदि की समस्याएँ भी देखने को मिलती है जो कि विकास की गति में बाधा पहुंचाते हैं।
हालांकि पेसा अधिनियम की खामियों को ढूंढकर उसे सही बनाने के लिए 2013 में भी इसमें संशोधन की कोशिश हुई, लेकिन वो सफल नहीं हुआ।
पेसा अधिनियम 1996 प्रैक्टिस क्विज
तो कुल मिलाकर यही है पेसा अधिनियम 1996 (PESA Act 1996), उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। संबन्धित अन्य लेखों को भी अवश्य पढ़ें।
???

![Indian Parliament (भारतीय संसद की बेसिक्स) [UPSC]](https://wonderhindi.com/wp-content/uploads/2020/10/भारतीय-संसद.jpg)
![बहुमत के प्रकार । Types of Majority in Hindi [UPSC]](https://wonderhindi.com/wp-content/uploads/2020/07/happy-woman-chatting-with-friends-online_74855-14073-440x264.webp)
![जनहित याचिका (PIL): अर्थ, उद्देश्य, लाभ आदि [UPSC]](https://wonderhindi.com/wp-content/uploads/2021/01/pil.jpg)