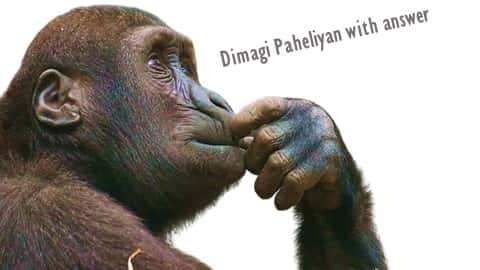भारत का संविधान निर्माण कैसे हुआ? जिस देश का संविधान इतना बड़ा हो और लगभग 3 साल उसे बनाने में लग जाये उसकी कहानी तो दिलचस्प होगी ही।
भारतीय संविधान को बनाना आसान काम नहीं था, इसे कई चरणों में पूरा किया गया है, कई देशों की संविधान की मदद ली गई है एवं कई विद्वानों ने इसमें भाग लिया है।
इस लेख में हम संविधान निर्माण की कहानी को जानेंगे और इसी के माध्यम से इसके महत्वपूर्ण पक्षों को भी एक्सप्लोर करेंगे। इस दिलचस्प लेख को अंत तक पढ़ें और हमारे सोशल मीडिया हैंडल से अवश्य जुड़ जाएँ।
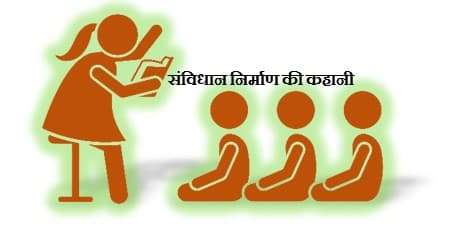
संविधान निर्माण (Making of the Constitution): पृष्ठभूमि
भारतीय संविधान और संविधान निर्माण की कहानी अपने आप में विलक्षण है; जहां कई देशों को कई बार अपना संविधान बनाना पड़ा, कई देशों को संविधान बनाने के बाद जनमत संग्रह (referendum) करवाना पड़ा ये देखने के लिए कि लोग इसे स्वीकार कर रहें हैं या नहीं।
पर भारतीय संविधान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि पहली बात तो भारतीय संविधान (Indian Constitution) को जिन लोगों ने बनाया उनमें समाज का पहले से ही अटूट विश्वास था।
दूसरी बात ये कि संविधान निर्माण के समय किसी प्रावधान को संविधान का हिस्सा बनाने के लिए वोटिंग का सहारा नहीं लिया गया बल्कि आपसी सहमति से इस प्रकार के समस्याओं को सुलझाया गया।
और आपसी सहमति बनाना कितना मुश्किल रहा होगा ये बात आप इससे समझ सकते हैं कि संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण सदस्यों के बीच आपस में बनती तक नहीं थी।
जैसे कि डॉ. भीमराव अंबेडकर को काँग्रेस पसंद नहीं था, वहीं पंडित नेहरू और डॉ. राजेंद्र प्रसाद की एक-दूसरे से बनती नहीं थी। पर ये काबिले तारीफ ही थी कि इस सब के बावजूद भी सहमति बना ली जाती थी।
वैसे भी जिस संविधान को बनने में लगभग 3 साल लग गये हो, उस संविधान के बनने की कहानी दिलचस्प तो होगी ही; है कि नहीं।
संविधान निर्माण की कहानी को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि संविधान होता क्या है? आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है? किसी देश के लिए संविधान जरूरी ही क्यों होता है?
आइये पहले संविधान के बेसिक्स को समझ लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में संविधान की अहमियत और उसकी प्रासंगिकता स्पष्ट हो सकें।
संविधान क्या है? (What is constitution?)
संविधान यानी कि श्रेष्ठ विधान; ये एक ऐसा दस्तावेज़ है जो व्यक्ति और राज्य के बीच सम्बन्धों को स्पष्ट करता है।
दूसरे शब्दों में, एक लोकतांत्रिक देश में व्यक्ति स्वतंत्रता का प्रतीक होता है या यूं कहें कि लोकतंत्र की अवधारणा ही इसी बात पर टिकी हुई है कि व्यक्ति स्वतंत्र रहें।
वहीं दूसरी ओर राज्य शक्ति का प्रतीक होता है यानी कि देश को चलाने के लिए सारी की सारी आवश्यक शक्तियाँ राज्य के पास होती है।
ऐसे में राज्य अपनी शक्तियों का गलत उपयोग न करें और व्यक्ति अपनी आजादी का गलत उपयोग न करें, इन्ही दोनों में संतुलन स्थापित करने के लिए जो दस्तावेज़ बनाए जाते हैं, वही संविधान है।
संविधान का उद्देश्य (Purpose of constitution)
संविधान के उद्देश्य को कुछ बेसिक प्रश्नों के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे कि –
- राज्य की संरचना कैसी होगी,
- सरकार की प्रकृति कैसी होगी,
- शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा,
- सरकार के अधिकार और कार्य तथा व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता क्या होगी,
- व्यक्ति और सरकार के बीच संबंध कैसा होगा,
- हम किस प्रकार के राज्य की स्थापना करना चाहते हैं इत्यादि।
इन्ही प्रश्नों का एक सर्वमान्य एवं व्यवस्थित उत्तर स्थापित करना संविधान का प्रमुख उद्देश्य होता है।
अब आते हैं संविधान निर्माण पर कि संविधान कैसे अस्तित्व में आया? संविधान निर्माण को समझने की दृष्टि से पाँच भागों में बाँट सकते हैं।
संविधान निर्माण के पाँच चरण (Five steps of making of Constitution)
1. संविधान सभा गठन के पूर्व की स्थिति
2. प्रारम्भिक संविधान सभा का गठन
3. गुलाम भारत के संविधान सभा की पहली कार्यवाही
4. संविधान निर्माण और पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव
5. आजाद भारत का संविधान सभा
1.संविधान सभा गठन के पूर्व की स्थिति
संविधान निर्माण के लिए 1946 में एक संविधान सभा (Constituent Assembly) का गठन किया गया था। इसी संविधान सभा ने संविधान निर्माण को उसकी परिणति तक पहुंचाया था।
पर संविधान सभा का गठन कैसे हुआ ये समझने के लिए पहले के उन महत्वपूर्ण घटनाओं को समझना जरूरी है जिसके फलस्वरूप संविधान सभा अस्तित्व में आया। तो आइये देखते है वो क्या हैं।
◾ 1764 ई. से 1857 तक के लगभग 100 साल के कंपनी शासन को देखें या फिर 1858 से 1947 तक के ताज के शासन को देखें तो इस दरम्यान ढेरों विधि-विधान बनाए गए।
हालांकि वो सब थे तो अंतत: ब्रिटिश हितों के पक्ष में ही लेकिन विधि-विधान की इस परंपरा ने भारतीयों को एक तरह से तैयार किया जो कि संविधान निर्माण के वक़्त काफी काम आया। इसे उदाहरण से समझते हैं –
जैसे कि आज हमारे संसद में दो सदन है राज्य सभा और लोक सभा। पर ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है बल्कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में पहली बार ये व्यवस्था किया गया था।
यहाँ तक कि प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था भी इसी अधिनियम में किया गया था। इसी प्रकार अगर हम संघीय व्यवस्था, संघीय न्यायालय आदि की बात करें तो इसका प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था।
लेकिन इन्ही अधिनियमों का गुलाम भारत में बहिष्कार किया गया था इसका कारण ये था कि इन अधिनियमों से भारतीय हित कम सधता था जबकि ब्रिटिश हित ज्यादा।
शायद इसीलिए 1922 में, महात्मा गांधी ने ये विचार रखा था कि भारतीयों के लिए एक संविधान होनी चाहिए। गांधीजी का इस मामले में कहना था कि – “स्वराज ब्रिटिश संसद का उपहार नहीं है, वह भारत की पूर्ण आत्माभिव्यक्ति की घोषणा होगी।”
- साल 1922 में एनिबेसेंट के प्रयासों से केन्द्रीय विधानमंडलों के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक शिमला में आयोजित की गई, जिसमें संविधान सभा की मांग की गई।
- फिर फरवरी 1923 में दिल्ली में एक अन्य सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों द्वारा संविधान के आवश्यक तत्वों की एक रूपरेखा तैयार की गई, जिसके तहत भारत को अन्य स्व-शासित राज्यों के बराबरी का दर्जा दिया गया था।
- अप्रैल, 1924 में तेजबहादुर सपूर की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कॉमनवैल्थ ऑफ इंडिया बिल का ड्राफ्ट तैयार किया गया।
- इसमें जरूरी संशोधनों के साथ, 1925 में हुई दिल्ली में हुई सर्वदलीय सम्मेलन में फिर से इसे रखा गया। महात्मा गांधी इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे।
- यहाँ से पास होने के बाद बिल को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। आम चुनाव में लेबर पार्टी की सरकार हार गई और यह बिल भी उसी के साथ खत्म हो गया।
◾ साइमन कमीशन की घोषणा के पूर्व भारतीय मामलों के सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने उस समय के भारतीय नेताओं को एक सर्वमान्य संविधान बनाने की चुनौती थी। लॉर्ड बर्कनहेड इस बात को लेकर आश्वस्त थे कांग्रेस द्वारा बनाए गए संविधान को मुस्लिम लीग के जिन्ना एवं अन्य नेता मान्यता ही नहीं देंगे।
कांग्रेस ने बर्कनहेड की इस चुनौती को स्वीकार किया और फ़रवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया। फिर मई 1928 में बंबई में सर्वदलीय बैठक हुई।
इसी अधिवेशन के दौरान पंडित मोतीलाल नेहरू ने केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्यों तथा अन्य नेताओं के परामर्श से भारत के लिए एक संविधान तैयार करने संबंधी प्रस्ताव रखा, जिसे कि स्वीकार भी कर लिया गया।
संविधान के सिद्धांत निर्धारित करने के लिए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। जिसने कि अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसे ही “नेहरू रिपोर्ट” के नाम से जाना जाता है।
नेहरू रिपोर्ट में भारत के संविधान की पूरी रूपरेखा शामिल थी, लेकिन उस वक्त भी संविधान अस्तित्व में न आ पाया। क्योंकि इस रिपोर्ट को भारत के मुस्लिम नेतृत्व, विशेषकर मुहम्मद अली जिन्ना ने खारिज कर दिया।
साथ ही राष्ट्रवादियों ने भी इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया क्योंकि पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की गई थी, बल्कि डोमिनियन की बात की गई थी।
| Important Facts |
|---|
| नेहरू समिति की रिपोर्ट ने सांप्रदायिकता को भी मान्यता प्रदान करने का काम किया था। इस समिति ने बंबई से सिंध को काटकर एक अलग मुस्लिम बहुल प्रांत बनाना स्वीकार किया था। इस मांग को मुसलमान काफी समय से कर रहे थे। कहा जाता है इसी निर्णय से मुसलमानों के अंदर विभाजन को लेकर आत्मविश्वास जागा था और इस संबंध में उसकी महत्वाकांक्षाएं आसामन छूने लगी। |
◾ साल 1934 में एक साम्यवादी नेता एम.एन. रॉय ने पहली बार एक संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की बात कही।
हालांकि ब्रिटिश सरकार ने 1935 में भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत एक ऐसी विस्तृत दस्तावेज़ पेश किया जो बिलकुल संविधान जैसा था। इसमें 321 धाराएँ और 10 अनुसूचियाँ थी। पर वहीं बात कि ये एक स्वतंत्र भारत का संविधान नहीं था। इसीलिए इस अधिनियम को कॉंग्रेस ने अप्रैल 1936 के लखनऊ अधिवेशन और दिसम्बर 1936 के फैजपुर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित करके इसे पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया।
इसके बाद 19-20 मार्च को काँग्रेस के विधानमंडल के सदस्यों ने राष्ट्रीय सम्मेलन में और 14 सितंबर 1939 को अपने ऐतिहासिक प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग दोहराई। नवम्बर 1939 में कॉंग्रेस कार्यकारिणी समिति ने फिर से एक प्रस्ताव पारित करने हुए भारत के लिए संविधान सभा की स्थापना पर जोर दिया।
अगस्त प्रस्ताव – इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और में जर्मनी की असाधारण सफलता ने ब्रिटेन की स्थिति अत्यन्त नाजुक कर दी थी। ऐसी स्थिति में भारतीयों का सहयोग पाने के लिये ब्रिटेन ने समझौतावादी दृष्टिकोण की नीति अपनाई।
और कॉंग्रेस की मांग को ध्यान में रखते हुए 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो ने भारतीयों के लिये एक प्रस्ताव की घोषणा की जिसे ‘अगस्त प्रस्ताव’ के नाम से जाना जाता है।
इस प्रस्ताव के मुख्य प्रावधान कुछ ऐसे थे, (i) भारत को डोमिनियन स्टेट्स देने का प्रस्ताव, (ii) द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत संविधान सभा गठन किए जाने का प्रस्ताव,
हालांकि इस अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा के गठन की बात कही गई थी लेकिन फिर भी काँग्रेस द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि इसमें एक स्वतंत्र-संप्रभु देश के बजाय डोमिनियन दर्जा देने की बात कही गई थी और दूसरी बात ये कि इसमें कहा गया था कि बिना अल्पसंख्यकों की स्वीकृति के सरकार कोई भी संवैधानिक परिवर्तन लागू नहीँ कर सकती है। यानी कि एक तरह से मुस्लिम लीग को वीटो पावर मिल रहा था।
क्रिप्स मिशन – उपरोक्त प्रस्ताव के असफल हो जाने के बाद ब्रिटिश सरकार ने संविधान निर्माण का एक प्रारूप तैयार किया और सन 1942 में उसे स्टाफोर्ड क्रिप्स के हाथों भारत भेजा। दरअसल क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए किया गया एक असफल प्रयास था।
इस मिशन ने युद्ध में सहयोग करने के बदले, युद्ध समाप्त होने के बाद चुनाव कराने, डोमिनियन स्टेटस देने और संविधान निर्माण की बात कही। इसे काँग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकृत कर दिया। और काँग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू कर दिया।
इससे हुआ ये कि ब्रिटिश सरकार ने सभी प्रमुख काँग्रेस नेताओं को जेल में बंद कर दिया। इससे एक व्यापक गतिरोध की शुरुआत हुई और स्थिति स्थिति धीरे-धीरे बिगड़ती चली गई।
वेवेल योजना – इसी गतिरोध को दूर करने के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने जून 1945 में एक योजना प्रस्तुत की जिसे कि वेवेल योजना कहा गया।
इस योजना की मुख्य बाते कुछ ऐसी थी – (1) वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या सवर्ण हिन्दुओं के बराबर होगी। (2) युद्ध समाप्त होने के उपरान्त भारतीय स्वयं ही संविधान बनायेंगे। (3) कांग्रेस के नेता रिहा किये जायेंगे तथा शीघ्र ही शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जायेगा। शिमला में सम्मेलन बुलाया भी गया लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की जिद के कारण ये योजना भी निरस्त हो गया।
मुस्लिम लीग भारत का विभाजन चाहते थे और अपनी बात पर अड़े थे कि भारत को दो स्वायत हिस्सों में बांटा जाना चाहिए जिसका कि अपना-अपना एक संविधान सभा होगा।
कैबिनेट मिशन – स्थिति इतनी बिगड़ गया कि अंतत: अंग्रेजों को झुकना ही पड़ा और सत्ता हस्तांतरण के लिए बाध्य होना ही पड़ा। इसके लिए वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लिमेंट एटली ने भारत में एक तीन सदस्यीय उच्च-स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की।
इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिये गये थे तथा इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिये, उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना था। इसे कैबिनेट मिशन कहा गया जो कि 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा।
काफी बहस और जद्दोजहद के बाद इन्होंने मुस्लिम लीग को किसी तरह से समझा बुझा लिया और इस तरह से एक अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा बनने का रास्ता साफ हो गया।
2. प्रारम्भिक संविधान सभा का गठन
संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा (Constituent Assembly) का होना जरूरी था। और ये संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गये तरीकों के आधार पर होना था। जो कि कुछ ऐसा था –
◾संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 आवंटित किया गया। जिसमें से 93 सीटें देशी रियासतों (Princely states) और 296 सीटें ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों के लिए आवंटित किए गए थे।
◾ये सीटें जनसंख्या के अनुपात में आवंटित की जानी थी मोटे तौर पर प्रत्येक 10 लाख लोगों पर 1 सीट की व्यवस्था की गयी थी।
◾संविधान सभा लिए के ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों से सदस्यों का चुनाव उसी के समुदाय द्वारा उसी के प्रांतीय असेंबेली में किया जाना था और देशी रियासतों के प्रतिनिधि का चुनाव रियासत प्रमुखों द्वारा किया जाना था।
तो कुल मिलाकर ये सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय होने वाली थी।
संविधान सभा के लिए चुनाव – 1946 के जुलाई-अगस्त में संविधान सभा के लिए चुनाव सम्पन्न हुआ। और ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों के लिए आवंटित 296 सीटों में से 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस को, 73 सीटें मुस्लिम लीग को और और बची सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों को मिला।
लेकिन देशी रियासतों को जो 93 सीटें मिला था उसने इसका बहिष्कार कर दिया और इसमें हिस्सा नहीं लिया यानी कि अपने प्रतिनिधि को उनलोगों ने संविधान सभा में नहीं भेजा।
3. गुलाम भारत के संविधान सभा की पहली कार्यवाही
इसे गुलाम भारत के संविधान सभा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय देश आजाद नहीं हुआ था। तो कुल मिलाकर देशी रियासतों ने तो संविधान सभा का पहले ही बहिष्कार कर रखा था और अब मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलने के बावजूद भी उसने इसका बहिष्कार कर दिया। अब ये स्पष्ट हो चुका था कि विभाजन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है और वही हुआ भी।
यही कारण था कि जब 9 दिसम्बर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो इसमें मात्र 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इसके बावजूद भी संविधान सभा ने उसी सदस्यों के साथ बैठक की और डॉ. राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया। इस तरह से संविधान निर्माण की आधारशिला रख दी गई।
4. संविधान निर्माण और पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव
इसके ठीक चार दिन बाद 13 दिसम्बर 1946 को पंडित नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ा। ये एक प्रस्तावना की तरह ही था।
ग़ौरतलब कि आज के प्रस्तावना में बहुत सारी बातों को उसी में से लिया गया है। इस उद्देश्य प्रस्ताव में इस बात को रेखांकित किया गया कि हमारा भावी संविधान कैसा होगा और उस से संचालित देश कैसा होगा।
इसमें कही गयी कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि –
◾यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य घोषित करती है और अपने भविष्य के प्रशासन के लिए संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। (हालांकि उस समय तक भारत आजाद नहीं हुआ था।)
◾ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत के बाहर के कोई क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे वे इस संघ का हिस्सा होंगे। संघ में निहित शक्तियों को छोड़कर सभी शक्तियाँ राज्यों को प्राप्त होंगी।
◾इस स्वतंत्र एवं संप्रभु भारत के सभी शक्तियों का स्रोत इसकी जनता होंगी। यानी कि जनता सर्वोपरि होगी।
◾भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक स्वतंत्रता; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाएगी। (इसे आप मौलिक अधिकार में भी पढ़ेंगे और प्रस्तावना में भी)
◾अल्पसंख्यकों एवं पिछड़े वर्गों तथा जनजातियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
◾विधि के अनुरूप सभी काम होंगे तथा भारत को विश्व में उसका उचित स्थान और अधिकार दिलाया जाएगा।
ये थी उद्देश्य प्रस्ताव की कुछ मूल बातें, जिसे कि 26 जनवरी 1947 को इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया।
उसके कुछ समय बाद ही माउण्टबेटन ने 3 जून 1947 को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ऐसा घोषणा किए जाने के बाद धीरे-धीरे लगभग सभी रियासतें (जिन्होने अब तक संविधान सभा का बहिष्कार कर रखा था) इस सभा में शामिल हो गया।
(कुछ को छोड़ कर जैसे कि – जम्मू और कश्मीर, हैदराबाद, और जूनागढ़ जिसे बाद में शामिल करा लिया गया। ये कैसे किया गया इसके लिए इस लेख↗️ को पढ़ें)
5. आजाद भारत का संविधान सभा
जैसा कि हम जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और संविधान सभा एक स्वतंत्र निकाय बन गया जिसे अब किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। इससे हुआ ये कि अब संविधान सभा अपनी पूरी क्षमता और गति के साथ काम करने लगे।
[चूंकि अब देश भी चलाना था इसीलिए सभा दो रूपों मे काम करने लगी। एक संविधान बनाने का काम और दूसरा सामान्य विधि बनाने का काम जिससे की तत्कालीन प्रशासन को चलाया जा सकें।]
[मुस्लिम लीग चूंकि अब अलग होकर एक नया राज्य पाकिस्तान बना चुका था इसीलिए संविधान सभा में सीटों की संख्या कम हो गयी और अब केवल 299 सीटें ही रह गयी थी जिसमें से 70 देशी रियासतों के लिए और बाकी ब्रिटिश प्रांत के लिए।]
संविधान निर्माण, व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से हो इसके लिए विभिन्न बड़ी और छोटी समितियों का गठन किया गया और सभी समितियों को उसके विशेषज्ञता और क्षमता के अनुसार कार्य सौप दिया गया।
आइये जान लेते है कि वो कौन-कौन समितियां (Committees) थी।
संविधान निर्माण के लिए निर्मित बड़ी समितियां
1. संघ शक्ति समिति – जवाहर लाल नेहरू
2. संघीय संविधान समिति – जवाहर लाल नेहरू
3. प्रांतीय संविधान समिति – सरदार पटेल
4. प्रारूप समिति – डॉ बी आर अंबेडकर
5. मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों एवं सीमांत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति – सरदार पटेल
6. प्रक्रिया नियम समिति – डॉ राजेंद्र प्रसाद
7. राज्यों के लिए समिति – जवाहर लाल नेहरू
8. संचालन समिति – डॉ राजेंद्र प्रसाद
9. झंडा समिति – जे बी कृपलानी
10. परामर्श समिति – सरदार पटेल
इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हैं प्रारूप समिति (Drafting committee)। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संविधान के प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेवारी इसी की थी।
सब कुछ ड्राफ्ट पर ही टिका था क्योंकि ड्राफ्ट तैयार होने के बाद ही इस पर बहस होता, इसमें संशोधन होता और अंतिम रूप से संविधान अस्तित्व में आ पाता।
प्रारूप समिति
प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष डॉ. बी.आर. अंबेडकर थे।
इसके अलावा और छह सदस्य क्रमशः एन गोपालस्वमी आयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एम माधव राव (इन्होंने बाद में बी एल मित्र की जगह ली।) टी टी कृष्णमचारी (इन्होंने डी पी खेतान की जगह ली।)
संविधान का प्रभाव में आना (Constitution comes into effect)
प्रारूप समिति द्वारा संविधान का पहला प्रारूप फ़रवरी 1948 में पेश किया गया। और इस में संशोधन कराने के लिए लोगों को 8 महीने का वक़्त दिया गया।
जितने भी संशोधन के मांग आये। जरूरत अनुसार उसमें संशोधन करके आठ महीने बाद अक्तूबर 1948 में इसे फिर से प्रकाशित किया गया।
4 नवम्बर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया गया। इस पर पाँच दिनों तक चर्चा हुई और 15 नवम्बर 1948 से इस पर खंडवार विचार और उस पर संविधान सभा में बहस होना शुरू हुआ। बहस इस कदर हुई कि कहा जाता है कि सार्वभौमिक मताधिकार ही एक ऐसा प्रावधान था जो कि बिना बहस के पास हो पाया।
17 अक्तूबर 1949 तक इस पर विचार और बहस चला और उसके बाद 14 नवम्बर 1949 से इस पर तीसरे दौर का विचार होना शुरू हुआ।
डॉ. अंबेडकर ने ‘The Constitution Age Settled by the Assembly be Passed’ नामक प्रस्ताव पेश किया और 26 नवम्बर 1949 को इसे पारित घोषित कर दिया गया।
जब ये बनकर तैयार हो गया तो इस संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और एक प्रस्तावना थी।
हालांकि जिस दिन ये पारित हुआ उस दिन सभी सदस्य नहीं आए थे केवल 284 सदस्य ही उपलब्ध थे तो उन्होने ही इस पर हस्ताक्षर किए। (आप इस लिंक के माध्यम से उस समय की कुछ तस्वीरें देख सकते हैं – संविधान निर्माण की तस्वीरें↗️)
और एक बात और याद रखने वाली है कि 26 नवम्बर 1949 को संविधान के सिर्फ कुछ ही प्रावधानों को लागू किया गया था जैसे कि नागरिकता, चुनाव आदि। जबकि सम्पूर्ण संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। जिस दिन हम गणतन्त्र दिवस (Republic Day) मनाते है।
इस दिन के पीछे कारण ये है कि इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित एक संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था।
संविधान निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण डॉ.अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता से संबोधित किया जाता है।
◾24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और 26 जनवरी 1950 से इस संविधान सभा ने तब तक अन्तरिम संसद के रूप में काम किया जब तक कि 1951-52 में आम चुनाव नहीं हो गया।
संविधान निर्माण तथ्य (Facts of making of Constitution)
◾संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। इस के दौरान संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई लगभग 60 देशों के संविधान को खंगाला गया। कहा जाता है कि उस समय इसमें लगभग 64 लाख रुपए खर्च आया। उस समय के हिसाब से ये काफी ज्यादा रकम था।
◾22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया।
◾मूल संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा इटैलिक शैली में लिखा गया, तथा इसका सौंदर्यीकरण शांतिनिकेतन के कलाकार द्वारा हुआ। (इन कलाकारों में नन्दलाल बोस और बिउहर राममनोहर सिन्हा शामिल थे)
◾मूल प्रस्तावना, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया तथा सौंदर्यीकरण राम मनोहर सिन्हा द्वारा हुआ।
◾मूल संविधान के हिन्दी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया जिसे कि नंदलाल बोस द्वारा सौंदर्यीकरण किया गया।
संविधान निर्माण की कहानी Practice Quiz
भारतीय राज्यों के बनने की कहानी
प्रस्तावना : अर्थ, महत्व, जरूरत, उद्देश्य
नागरिकता क्या है?
विदेशी भारतीय नागरिकता
मौलिक अधिकार
References,
Wikipedia – Constitution of India↗️
आधुनिक भारत का इतिहास – विपिन चंद्र↗️
भारत का संविधान – कक्षा 11 राजनीति विज्ञान↗️
इतिहास के कुछ विषय – कक्षा 12 इतिहास पार्ट 3↗️
भारत का संविधान – प्रमोद कुमार अग्रवाल
एम लक्ष्मीकान्त – भारत की राजव्यवस्था
स्पेक्ट्रम – आधुनिक भारत का इतिहास
न्यूज़पेपर के कुछ अंश;

![पंचायती राज व्यवस्था : स्वतंत्र भारत में पंचायत [UPSC]](https://wonderhindi.com/wp-content/uploads/2021/02/पंचायती-राज.jpg)
![Same Sex Marriage (समलैंगिक विवाह): Case Study [UPSC]](https://wonderhindi.com/wp-content/uploads/2023/10/young-beautiful-woman-dress-up-local-culture-southern-region-with-rainbow-flag_24797-1309-440x264.webp)