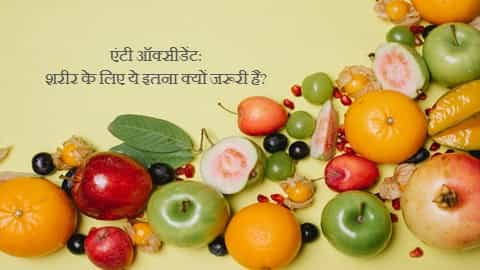इस लेख में हम मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) का एक परिचयात्मक अध्ययन करेंगे एवं संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आने वाले दो शुरुआती अनुच्छेद (अनुच्छेद 12 और 13) पर सरल और सहज चर्चा करेंगे,
तो मौलिक अधिकारों की आधारभूत समझ के लिए इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें, और साथ ही इस टॉपिक से संबंधित अन्य लेखों को भी पढ़ें। [मौलिक अधिकारों पर लेख]

| 📖 Read in English |
मौलिक अधिकार की आधारभूत समझ
18वीं सदी की जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट के विचार में ”हर चीज़ की या तो कीमत होती है या गरिमा” जिसकी कीमत होती है उसके जगह कोई अन्य समतुल्य वस्तुएँ रखी जा सकती है पर इसके इत्तर जिसकी कोई कीमत न हो या जो सभी कीमतों से ऊपर हो; वो है किसी व्यक्ति की गरिमा।
व्यक्ति की ये गरिमा कुछ मूलभूत अधिकारों एवं दायित्वों पर टिका होता है। कांट ने इन विचारों के जरिये अधिकार की एक नैतिक अवधारणा प्रस्तुत की। पहला, हम अधिकारों की प्राप्ति के लिए इतने स्वार्थी न हो जाये कि दूसरों का नुकसान कर बैठें। दूसरा, हम दूसरों के साथ वैसा ही आचरण करें जो हम अपने लिए सामने वाले से अपेक्षा रखते हैं।
मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है और समय के साथ उन्होने एक ऐसा जटिल सामाजिक संरचना विकसित की है जहां लोगों को अपनी इच्छाओं एवं जरूरतों के हिसाब से जीने के लिए कुछ अधिकार होते है।
समाज में किसी के पास बहुत ही ज्यादा अधिकार होते हैं तो किसी के पास बहुत ही कम पर सभी के पास कुछ न कुछ अधिकार जरूर होते हैं। दरअसल ये अधिकार बोध प्राकृतिक तौर पर हमारे अंदर विद्यमान होता है।
अधिकार क्या है? (What is right?)
अधिकार वो हक़ या मांग या दावे है जो हमें मिलता है, या तो राज्य से, समाज से, परिवार से, खुद से या फिर प्रकृति से।
17वीं एवं 18वीं शताब्दी के राजनैतिक चिंतकों का अधिकार के बारे में तर्क यही होता था कि ये प्रकृति या ईश्वर प्रदत है और कोई व्यक्ति या शासक उसे हमसे छीन नहीं सकता है। उस समय इस तरह के तीन प्राकृतिक अधिकार चिन्हित किए गए थे – जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार एवं संपत्ति का अधिकार।
उस समय की यही अवधारणा हाल के वर्षों में मानवाधिकार (Human Rights) के रूप में प्रचलित हुआ है। ज्यों-ज्यों लोगों के अंदर तार्किक चेतना घर करने लग गया, वे ईश्वर केन्द्रित से स्वकेंद्रित होने लग गया और इस तरह से इन्सानों ने समय के साथ कई ऐसे अधिकारों की खोज की जो उसके लिए उपयुक्त था।
मानवाधिकार क्या है? (What is Human Rights?)
मानव अधिकारों के पीछे का मूल तर्क ये है कि सिर्फ मनुष्य होने मात्र से हम कुछ चीजों को पाने के अधिकारी हो जाते हैं। इसका दूसरा मतलब ये है कि आंतरिक दृष्टि से सभी मनुष्य समान है इसीलिए उन्हे स्वतंत्र रहने तथा अपनी पूरी संभावनाओं को साकार करने का समान अवसर मिलना ही चाहिए।
तो कुल मिलाकर वे सभी अधिकार जो कम से कम एक इंसान होने के नाते हमें मिलनी ही चाहिए, मानवाधिकार है। उदाहरण के लिए- जीने का अधिकार, इसके तहत ढेरों संबन्धित अधिकार आ सकते हैं जैसे कि खाने का अधिकार, कपड़े पहनने का अधिकार, घर में रहने का अधिकार आदि।
अब ऐसा तो नहीं हो सकता है न कि कोई देश इसे दे और कोई न दे। इसीलिए मानवाधिकार किसी राज्य की सीमाओं से नहीं बंधी होती है बल्कि ये पूरी मानवजाति के लिए होती है। इस विचार का इस्तेमाल समाज में व्याप्त नस्ल, जाति, धर्म और लिंग पर आधारित मौजूदा असमानताओं को खत्म करने या चुनौती देने के लिए किया जाता है।
यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स (UDHR) मानवाधिकारों के इतिहास में एक मील का पत्थर दस्तावेज़ है। इसे 10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने स्वीकार किया और लागू किया।
मानवाधिकार की पैरवी करने वाले ढेरों देश और संस्थाएं आज भी इस दस्तावेज़ से प्रेरणा लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, इसे आप खुद ही देख सकते हैं; UDHR
मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR)
| चूंकि, मानव परिवार के सभी सदस्यों के जन्मजात गौरव और सम्मान तथा अविच्छिन अधिकार की स्वीकृति ही विश्व-शांति, न्याय और स्वतंत्रता की बुनियाद है, चूंकि, मानव अधिकारों के प्रति उपेक्षा और घृणा के फलस्वरूप ही ऐसे बर्बर कार्य हुए जिनसे मनुष्य की आत्मा पर अत्याचार किया गया, इसीलिए यह अनिवार्य है कि ऐसे विश्व की स्थापना हो जिसमें सभी मनुष्य भाषण तथा विश्वास की स्वतंत्रता हासिल तथा भय तथा अभाव से मुक्ति प्राप्त कर सकें, जो मानव समुदाय की सबसे महत्वपूर्ण अभिलाषा है। चूंकि, यह आवश्यक है कि मनुष्य को अत्याचार तथा दमन के विरुद्ध अंतिम अस्त्र के रूप में विद्रोह न करना पड़े, इसीलिए विधि के शासन के द्वारा मनवाधिकारों की रक्षा हो, चूंकि, राष्ट्रों के मध्य मित्रतापूर्ण संबन्धों की स्थापना को प्रोत्साहित करना आवश्यक है, चूंकि, संयुक्त राष्ट्रसंघ के देशों ने घोषणा पत्र में मूलभूत मानवाधिकारों, मनुष्य की गरिमा तथा महत्व तथा पुरुषों तथा महिलाओं के समान अधिकारों के प्रति अपना विश्वास पुनः व्यक्त किया तथा व्यापक स्वतंत्रता की उपलब्धि हेतु उत्तम जीवन स्तर तथा सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया है, चूंकि, सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के सहयोग से मानव अधिकारों तथा मूल स्वतंत्रताओं के विश्व स्तर पर सम्मान तथा अनुपालन को प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया है, चूंकि, उक्त संकल्पों की पूर्ण उपलब्धि हेतु इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सार्वदेशिक अवधारणा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अतः आज संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा, मनवाधिकारों के विश्वजनीन घोषणा पत्र को सभी सभ्यताओं तथा देशों के लिए उपलब्धि के सर्वमान्य मानदंड के रूप में एतदर्थ घोषित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति तथा समाज का प्रत्येक अंग इस घोषणा पत्र का सदा विचार रखते हुए इन अधिकारों तथा स्वतंत्रता, स्वतंत्रताओं की मर्यादा को अध्यापन तथा शिक्षा के माध्यमों द्वारा प्रोत्साहित करेगा तथा विकासोन्मुख राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय साधनों द्वारा इनकी सार्वदेशिक तथा सशक्त स्वीकृति एवं अनुपालन को आपस में, सदस्य देशों की जनता के बीच तथा उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले प्रदेशों की जनता के बीच स्थापित करेगा। |
तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अधिकारों के संबंध में यहाँ ढ़ेरों बातें की गई है, जैसे कि भाषण एवं विश्वास की स्वतंत्रता, विधि का शासन, मनुष्य की गरिमा एवं महिलाओं के समान अधिकार इत्यादि। ये समझना इसीलिए जरूरी है ताकि जब आप भारतीय संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के बारे में समझें तो ये समझ पाएँ कि भारतीय संविधान ने इन सभी बातों को अपने में सम्मिलित किया है। हालांकि इससे संबन्धित भारत में मानवाधिकारों की स्थिति↗️ पर एक अलग से लेख साइट पर उपलब्ध है, उसे जरूर पढ़ें।
◾ अधिकारों की बातें करने भर से तो ये लागू हो नहीं जाएगा इसे उचित उचित संवैधानिक संरक्षण भी देना पड़ता है। भारत का संविधान इस मामले में अग्रणी है क्योंकि ये न्यायोचित मूल अधिकारों की एक लंबी एवं विस्तृत सूची उपलब्ध कराता है जो कि कानूनी रूप से प्रवर्तनीय भी है। मुख्य रूप से यहाँ दो टर्म आता है – संवैधानिक अधिकार (Constitutional right) एवं मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)।
संवैधानिक अधिकार क्या है? (What is constitutional right?)
जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है ये वो अधिकार है जो संविधान हमें देता है। एक सवाल यहाँ आता है कि मौलिक अधिकार भी तो संविधान द्वारा ही दिया जाता है।
हाँ, पर एक बात याद रखने वाली है कि मौलिक अधिकार केवल वो है जिसे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत दिया गया है जबकि संवैधानिक अधिकार वे सभी हैं जो पूरे संविधान में उल्लेखित है।
यानी कि सभी मौलिक अधिकार संवैधानिक अधिकार है लेकिन सभी संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। जैसे कि संपत्ति के अधिकार को ही ले लें तो ये एक संवैधानिक अधिकार तो है पर एक मौलिक अधिकार नहीं है।
मौलिक अधिकार क्या है? (What is a Fundamental Right?)
मौलिक अधिकार वो न्यूनतम अधिकार है जो किसी व्यक्ति के चहुंमुखी विकास यानी कि बौद्धिक, नैतिक, भौतिक, एवं आध्यात्मिक विकास के लिए चाहिए ही चाहिए। इसके लिए ”राजनीतिक अधिकार (Political rights)” शब्द का भी प्रयोग किया जाता है।
भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) की चर्चा की गयी है। और हम इस लेख में हम अनुच्छेद 12 एवं अनुच्छेद 13 को समझेंगे।
◾ संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्नाकार्टा कहा जाता है। इसे मैग्नाकार्टा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इंग्लैंड में सर्वप्रथम 1215 में एक दस्तावेज़ बनाया गया जिसमें जनता को कुछ मूलभूत अधिकारों की गारंटी दी गयी जिसे मैग्नाकार्टा कहा गया। भारत के संविधान का भाग 3 भी चूंकि मूलभूत अधिकारों की गारंटी देती है इसीलिए इसे भारत का मैग्नाकार्टा कहा जाता है।
मूल संविधान के 7 मौलिक अधिकार
मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार दिये गए थे जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात याद रखने योग्य है कि संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संसोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है। इसीलिए अब सिर्फ 6 मूल अधिकार ही है।
| मौलिक अधिकार |
| 1. समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 – 18 2. स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 – 22 3. शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 – 24 4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 – 28 5. शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 – 30 ❌ 6. संपत्ति का अधिकार – अनुच्छेद 31 6. संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32 |
अनुच्छेद 12 – परिभाषा
दरअसल मूल अधिकारों के कुछ उपबंधो को छोड़कर सारे के सारे उपबंध राज्य (State) के मनमाने रवैये के खिलाफ है मतलब ये की अगर राज्य द्वारा आपके मूल अधिकारों का हनन किया जाता है, तो आप सीधे उच्चतम या उच्च न्यायालय जा सकते हैं क्योंकि मूल अधिकारों की सुरक्षा और प्रवर्तन का ज़िम्मा अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट पर है।
अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि हम राज्य माने किसे क्योंकि यहाँ तो स्टेट को भी राज्य कहा जाता है और देश को भी।
अनुच्छेद 12 में इसी राज्य को परिभाषित किया गया है। तो आइये देखते हैं संविधान के अनुसार राज्य क्या है?
राज्य क्या है? (What is the state?)
▪️ इसके अनुसार कार्यकारी एवं विधायी अंगों को केंद्रीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद, राज्य है।
▪️ उसी प्रकार, कार्यकारी एवं विधायी अंगों को राज्य में क्रियान्वित करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल, राज्य हैं।
▪️ सभी स्थानीय निकाय जैसे की नगरपालिका, पंचायत, जिला बोर्ड आदि, राज्य हैं।
▪️ भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी, जैसे- एलआईसी, ओएनजीसी आदि भी राज्य हैं। सोसाइटी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड सोसाइटी भी राज्य है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी राज्य है।
इसका मतलब समझ गए न कि इन में से अगर किसी के द्वारा भी मूल अधिकारों का हनन किया जाता है तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यहाँ यह याद रखिए कि राज्य की यह जो परिभाषा है वो केवल संविधान के भाग 3 और भाग 4 के लिए है। संविधान के दूसरे भागों के लिए इसके मायने अलग भी हो सकते हैं।
यहाँ यह याद रखिए कि निम्नलिखित निकाय अनुच्छेद 12 के तहत राज्य नहीं माना जाता है;
- ऐसा असंवैधानिक निकाय जो कानूनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है। जैसे कि कोई कंपनी जो कि सरकार का अधिकरण न हो।
- प्राइवेट निकाय जिसे कोई कोई कानूनी शक्ति हासिल नहीं है। या फिर जिसे किसी राज्य अधिनियम से समर्थन प्राप्त नहीं होता है।
अनुच्छेद 13 – मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ
ये अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है संविधान निर्माण के बाद से जितने भी विवाद मूल अधिकारों को लेकर हुआ है उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 13 उसमें रहा ही है।
ये बात आप तब समझेंगे जब गोलकनाथ मामला, केशवानन्द भारती आदि जैसे मामलों के बारे में जानेंगे। खैर इसकी चर्चा तो आगे करेंगे अभी जान लेते हैं कि अनुच्छेद 13 कहता क्या है?
अनुच्छेद 13 – (1) इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले भारत के राज्यक्षेत्र में लागू सभी विधियाँ उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत है।
कहने का ये मतलब है कि हमारा संविधान लागू होने से पहले जितने कानून चल रहे थे, संविधान लागू होने के बाद उसका उतना हिस्सा रद्द हो जाएंगी जो संविधान के भाग 3 में बताए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।
(2) राज्य ऐसी कोई विधि (law) नहीं बना सकती है जो संविधान के इस भाग में वर्णित मूल अधिकारों को छीनती है या उसे कम करती है। लेकिन अगर राज्य ऐसा करता है तो वो विधि उतनी मात्रा तक शून्य हो जाएंगी जो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा होगा।
अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लगता है की किसी विधि के द्वारा मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रह है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट उस विधि को असंवैधानिक भी घोषित कर सकती है। इस संबंध में बहुत सारे सवाल उठते हैं, उसका उत्तर समझने के लिए नीचे दिए गए FAQs पढ़ें।
अब यहाँ भी एक सवाल है कि विधि क्या होता है या फिर हम विधि किसको माने। इसका जवाब इस अनुच्छेद के बिन्दु (3) के तहत दिया गया है –
विधि क्या है?(What is the law?)
अनुच्छेद 13 के अनुसार निम्नलिखित बातें विधि मानी जाएंगी।
1. संसद या राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विधियाँ
2. राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश (Ordinance)
3. प्रत्यायोजित विधान (Delegated statement) जैसे कि – (आदेश order), उप-विधि (Bye law), नियम (Rule), विनियम (Regulations) या अधिसूचना (Notification)।
4. विधि के गैर-विधायी स्रोत जैसे कि – किसी विधि का बल रखने वाली रूढ़ि या प्रथा (Custom or practice)।
नोट – संविधान संशोधन (Constitutional amendment) एक विधि है कि नहीं इसकी चर्चा यहाँ नहीं की गई है इसीलिए लंबे समय तक ये माना जाता रहा कि चूंकि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है इसीलिए उसे न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकती है।
लेकिन 1973 के केशवानन्द भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकार के हनन के आधार पर संविधान संशोधन को भी चुनौती दी जा सकती है और मूल अधिकारों से असंगत पाये जाने पर उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है।
मौलिक अधिकार का महत्व
⚫ मौलिक अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ है। ये अधिकार राज्य को कुछ खास तरीकों से कार्य करने के लिए वैधानिक दायित्व सौंपते हैं। प्रत्येक अधिकार निर्देशित करता है कि राज्य के लिए क्या करने योग्य है और क्या नहीं। जैसे कि अगर कोई मेरे जीने के अधिकार को क्षति पहुंचाता है तो राज्य का ये दायित्व बनता है कि वे ऐसे कानून बनाए जिससे की कोई मेरे जीने के अधिकार को क्षति न पहुंचा पाये।
⚫ ये व्यक्ति की भौतिक एवं नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थिति उत्पन्न करता है एवं व्यक्तिगत सम्मान को बनाए रखता है।
⚫ ये सरकार के पूर्णता पर नियंत्रण लाता है और व्यक्तिगत एवं सामूहिक अधिकारों को बढ़ावा देता है। इसीलिए इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षक कहा जाता है।
⚫ ये अल्पसंख्यकों एवं समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हुए लोगों को राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रणाली में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है।
⚫ ये देश में विधि के शासन को संरक्षित करता है एवं सामाजिक समानता एवं सामूहिक न्याय को सुदृढ़ करता है।
अधिकार एवं कर्तव्य (Rights and Duties)
जब भी हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये मानकर चलना चाहिए कि कर्तव्य भाव भी उसी में निहित है। ये न सिर्फ राज्यों के लिए है बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए है।
जैसे कि हमें व्यवसाय करने का अधिकार प्राप्त है तो हमने ऐसे व्यवसाय चलाने शुरू कर दिये जिससे जल, जमीन, वायु सभी प्रदूषित हो रहे हैं। ऐसे में हमारा दायित्व या कर्तव्य बनता है कि नए वृक्ष लगाकर, जंगलों की कटाई को रोककर, जल को प्रदूषित होने से रोककर, पारिस्थितिकीय संतुलन कायम रखने में अपनी भूमिका को सुनिश्चित करें।
वैसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान में एक नया भाग 4’क’ जोड़कर प्रत्येक नागरिक के लिए मौलिक कर्तव्यों (Fundamental duties) को सुनिश्चित किया गया है।
मूल अधिकारों की विशेषताएँ
⚫ भाग 3 के अंतर्गत जितने भी मूल अधिकारों की चर्चा की गई है उसमें से कुछ सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है जैसे कि अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 एवं 30। बाद बाकी अन्य सभी व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध है। इसकी चर्चा हमने नागरिकता (Citizenship) वाले लेख में भी किया है।
⚫ ये अधिकार असीमित नहीं होते हैं, यानी कि राज्य इस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध (Reasonable restriction) लगा सकता है। उदाहरण के लिए अभिव्यक्ति की आजादी के तहत किसी को भी तस्वीरे खींचने की आजादी है लेकिन अगर वो किसी की नहाते हुए तस्वीर खींच लेता है तो ये उसकी निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा, और ऐसे अधिकार तो किसी को हरगिज़ नहीं दी जा सकती।
⚫ ये अधिकार स्थायी नहीं है, यानी कि संसद इसमें कटौती या कुछ जोड़ सकता है। हाँ, लेकिन शर्त ये है कि इस तरह के संशोधन से संविधान के मूल ढांचे को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। जैसे कि अगर संसद ये चाहे कि जीने के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया जाये तो वे ऐसा नहीं कर सकते।
हालांकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, लेकिन चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट की नजर में संविधान का मूल ढांचा नहीं था इसीलिए इसे हटाये जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा।
⚫ ये प्रवर्तनीय (Enforceable) होते हैं एवं इन्हे उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है। मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है और उच्चतम न्यायालय उसे सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है।
FAQs
Q. मूल अधिकार से असंगत होने पर क्या उच्चतम न्यायालय सम्पूर्ण विधि को शून्य कर देगा?
आमतौर पर न्यायालय पृथक्करण के सिद्धांत (principle of separation) को अपनाता है। यानी कि उच्चतम न्यायालय यह देखता है कि अगर किसी विधि का कोई ऐसा प्रावधान मूल अधिकारों से असंगत है जिसे कि उस विधि/अधिनियम से पृथक किया जा सकता है तो केवल वह प्रावधान ही शून्य घोषित किया जाएगा, सम्पूर्ण विधि नहीं।
अगर कानून इस तरह से बना हो कि इस तरह के असंगत प्रावधान को उससे अलग करना नामुमकिन हो तो फिर न्यायालय पूरे कानून को शून्य करने के बारे में विचार करता है।
Q. मूल अधिकारों के हनन के मामले में उच्चतम न्यायालय के अधिकार एवं कर्तव्य क्या है?
उच्चतम न्यायालय विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियमों का सम्मान करता है और आमतौर पर ये मान के चलता है कि विधानमंडल ने बनाया है तो सही ही बनाया होगा।
लेकिन एक बार जब उच्चतम न्यायालय को यह लग जाता है कि किसी याची (petitioner) के मूल अधिकारों का उल्लंघन राज्य के क़ानूनों से हुआ है तो उच्चतम न्यायालय का ये कर्तव्य होता है कि उस मामले में वह हस्तक्षेप करें, और मूल अधिकारों को लागू करें।
Q. उच्चतम न्यायालय किसी विधि के संवैधानिकता पर कब विचार करता है?
उच्चतम न्यायालय किसी विधि के संवैधानिकता पर विचार करने से पहले सामान्यतः दो चीज़ें देखती है। पहला यह कि विधि सामान्य विधि बनाने की प्रक्रिया का पालन करके बनाया गया है कि नहीं और दूसरा ये कि वह विधि या उसका कोई हिस्सा मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है या नहीं।
याद रखें – न्यायालय यह मान कर चलता है कि विधि संवैधानिक है और यह सिद्ध करने का भार कि विधि मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, उस व्यक्ति पर होता है जिसने अपील की है।
यह भी याद रखिए कि अगर किसी कानून का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उसकी संवैधानिकता पर विचार नहीं करता।
Q. विधि की संवैधानिकता पर कौन सवाल उठा सकता है और कौन नहीं?
जिसपर उस विधि का सीधा प्रभाव पड़ता है। उसे न्यायालय के समक्ष यह बतानी होगी कि उस विधि से उसे क्या क्षति हुई है। अगर कोई व्यक्ति मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है तो वह किसी विधि की विधिमान्यता पर आक्षेप नहीं कर सकता है।
Q. क्या मौलिक अधिकार का त्याग किया जा सकता है?
इस मामले में आम मत ये है कि कोई नागरिक ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि यह मौलिक अधिकार उस व्यक्ति के लाभ के लिए बनाए गए है।
Q. क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक या शून्य घोषित कर दिए जाने पर संसद या विधानमंडल फिर से उसी कानून को पारित कर सकती है?
नहीं, विधानमंडल या संसद फिर से नया कानून बना सकती है जो कि असंवैधानिक तत्वों से मुक्त हो।
इस लेख में बस इतना ही, संक्षिप्त में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को समेटने की कोशिश की गई है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगले लेख में हम समता का अधिकार (Right to Equality) यानी कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक की चर्चा करेंगे उसे पढ़ने के लिए क्लिक करें।
मौलिक अधिकार अभ्यास प्रश्न
References,
मूल संविधान भाग 3↗️
NCERT कक्षा 11A राजनीति विज्ञान↗️
UN – UDHR↗️
डी डी बसु एवं एनसाइक्लोपीडिया इत्यादि


![क्षमादान की शक्ति : राष्ट्रपति एवं राज्यपाल [UPSC Concept]](https://wonderhindi.com/wp-content/uploads/2020/07/cute-couple-barista-apron-feeling-sorry-apologize-cartoon-character-illustration_56104-416-440x264.webp)