इस लेख में हम अध्यादेश (Ordinance) के बारे में सरल और सहज चर्चा करेंगे, एवं इसके विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए लेख को अंत तक जरूर पढ़ें और साथ ही संबन्धित अन्य लेखों को भी पढ़ें।
| पाठकों से अपील 🙏 |
| Bell आइकॉन पर क्लिक करके हमारे नोटिफ़िकेशन सर्विस को Allow कर दें ताकि आपको हरेक नए लेख की सूचना आसानी से प्राप्त हो जाए। साथ ही नीचे दिए गए हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ जाएँ और नवीनतम विचार-विमर्श का हिस्सा बनें; |
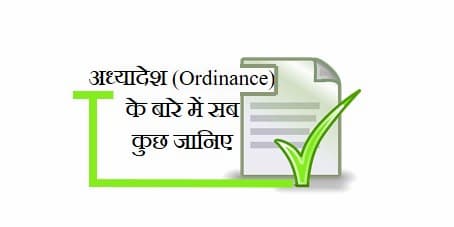
अगर टेलीग्राम लिंक काम न करे तो सीधे टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें – @upscandpcsofficial
| 📖 Read in English |
एक कहावत है – ‘सब दिन होत न एक समान’। ये कहावत राजनीति में भी ज्यादा चरितार्थ हो जाता है, चूंकि सब दिन संसद चल नहीं सकता है। आखिर उसे भी रेस्ट की जरूरत पड़ती ही है। फिर ऐसे में विधि बनाने का काम कौन करेगा?
अध्यादेश क्या है? (What is an ordinance?)
क्या हो अगर संसद का सत्रावसान हो गया हो या फिर कहें कि वो छुट्टी पर हो और राजनीतिक स्थिति कुछ इस तरह से बदल जाए कि किसी कानून की सख्त जरूरत आन परे तो ऐसी ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा?
इसी स्थिति को ध्यान में रखकर संविधान ने अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया है कि वो अध्यादेश (Ordinance) जारी कर सकता है।
यहीं स्थिति किसी राज्य में भी तो हो सकता है इसीलिए संविधान ने अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को भी ये अधिकार दिया है कि वो राज्य में अध्यादेश(Ordinance) जारी कर सकता है।
अब तक आप समझ ही गए होंगे कि अध्यादेश कुछ और नहीं बल्कि एक कानून ही है जो तब बनाया जाता है जब संसद कार्य न कर रहा हो। या फिर राज्य की बात करें तो जब राज्य विधानमंडल काम न कर रहा हो।
दूसरे शब्दों में कहें तो अध्यादेश कुछ और नहीं बल्कि कानून की दुनिया में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है। जिसे कि जरूरत के वक्त एंट्री कारवाई जाती है।
इन अध्यादेशों का प्रभाव व शक्तियाँ, संसद और विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून की तरह ही होता है परंतु ये प्रकृति से अल्पकालीन होते हैं। यानी कि ये कानून संसद और विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून की तरह हमेशा के लिए नहीं होता है। बल्कि इसकी कुछ सीमाएं निर्धारित कर दी गयी है।
डॉ. भीमराव अंबेडकर
अध्यादेश जारी करने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को उस परिस्थिति से निपटने में योग्य बनाती है जो आकस्मिक व अचानक उत्पन्न होती है और संसद के सत्र कार्यरत नहीं होते है।
अध्यादेश जारी करना केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल की एक विधायी शक्ति है। [राष्ट्रपति के समस्त विधायी शक्ति (Legislative power) के बारे में हम एक अलग लेख में बात कर चुके है।]
कुछ प्रावधानों को छोड़ दे तो राष्ट्रपति और राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति बराबर ही है। जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। उसी तरह से राज्य में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। इस लेख में हम दोनों की चर्चा करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए।
राष्ट्रपति और राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की सीमाएं
राष्ट्रपति अध्यादेश केवल तीन स्थितियों में जारी कर सकता है।
1. जब संसद के दोनों सदन का सत्र न चल रहा हो।
2. जब लोकसभा का सत्रावसान हो गया हो लेकिन राज्यसभा चल रहा हो।
3. जब लोकसभा चल रहा हो लेकिन राज्य सभा का सत्रावसान हो गया हो।
यानी कि अध्यादेश उस समय भी जारी किया जा सकता है जब संसद में केवल एक सदन का सत्र चल रहा हो क्योंकि जाहिर है कोई भी विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना होता है न की केवल एक सदन द्वारा।
इससे एक बात और समझ सकते हैं कि जब संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो उस समय अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है।
▶ एक और महत्वपूर्ण बात याद रख लीजिए कि अगर लोकसभा भंग हो गया हो, यानी कि सरकार गिर गया हो तो फिर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। किसी राज्य पर भी यही लागू होता है।
ये सीमाएं तो केंद्र का था। सवाल ये है कि राज्य में क्या होगा?
किसी राज्य में राज्यपाल की भी यही स्थिति होती है। ये जो अभी तीन सीमाएं राष्ट्रपति की बताई गयी है, यही सीमाएं हूबहू राज्यपाल पर भी लागू होती है।
लेकिन बस इतना ध्यान रखिए कि कुछ राज्य में विधानमंडल द्विसदनीय होता है। यानी कि वहाँ विधानसभा के साथ-साथ विधानपरिषद भी होता है। तो ऐसे जितने भी राज्य हैं वहाँ तो ऊपर वाला तीनों कंडिशन हूबहू लागू हो जाएगा।
जहां विधानमंडल एक सदनीय वहाँ सिर्फ पहले नंबर वाले कंडिशन से ही काम चल जाएगा। यानी कि उस सदन के सत्र का न चलना।
▶ अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल जानबूझकर संसद या विधानमंडल को स्थगित करके अध्यादेश लाता है तो याद रखिए उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
? राष्ट्रपति कोई अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब वह इस बात संतुष्ट हो कि मौजूदा परिस्थिति ऐसी है कि उसके लिए तत्काल कारवाई करना आवश्यक है।
राज्यपाल के मामले में भी बिल्कुल यही स्थिति है। तो इसको अलग से लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है।
अध्यादेश की समयावधि और उसके तीन महत्वपूर्ण पक्ष
1. अध्यादेश केवल उन्ही मुद्दों पर जारी जा सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है। यानी कि किसी ऐसे मुद्दे पर अध्यादेश नहीं लाया जा सकता है जिस मुद्दे पर किसी भी कारण से संसद भी कानून नहीं बना सकती हो।
2. अध्यादेश की वही संवैधानिक सीमाएं होती है, जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून की होती हैं। अतः एक अध्यादेश_ किसी भी मौलिक अधिकार का लघुकरण अथवा उसको छीन नहीं सकता।
अगर ऐसा होता है तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और न्यायालय उस अध्यादेश का उसी तरह से समीक्षा कर सकती है जैसे कि वो नॉर्मल कानून का करती है।
3. जैसा कि हम जानते है, अध्यादेश_ तभी जारी किया जाता है जब संसद सत्र न चल रहा हो। संसद में जब भी सत्रावसान होता है तो नियम ये है कि दो सत्रावसानों के बीच अधिकतम 6 महीने से ज्यादा का गैप न हो। आमतौर पर होता भी नहीं है।
इसीलिए अध्यादेश_ की अधिकतम अवधि 6 महीने तक है। क्योंकि जाहिर है इन 6 महीनों के अंदर संसद का सत्र चालू हो ही जाएगा।
संसद का सत्र जैसे ही चालू हो जाएगा उसके 6 सप्ताह के भीतर उस अध्यादेश को दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
यदि संसद के दोनों सदन उस अध्यादेश_ को पारित कर देती है तो वह कानून का रूप धारण कर लेता है। और अगर उस अध्यादेश को संसद अस्वीकृत कर दें तो वह अध्यादेश_वही समाप्त हो जाता है।
अगर उसे संसद में पेश नहीं किया जाएगा तो बैठक शुरू होने के 6 सप्ताह के बाद वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। और अगर बैठक शुरू नहीं होता है तो अधिकतम 6 महीने तक वो अध्यादेश वैध रह सकता है।
▶ याद रखिए यदि कोई अध्यादेश संसद के सभापटल पर रखने से पूर्व ही समाप्त हो जाता है तो इस अध्यादेश के अंतर्गत किए गए कार्य तब भी वैध व प्रभावी रहेंगे।
एक बात और याद रखिए कि यदि संसद का दोनों सदन अलग-अलग तिथियों पर शुरू होता है। तो 6 सप्ताह की गणना; जो सदन सबसे बाद में जो शुरू हुआ होगा, वहाँ से होगा।
ये तो केंद्र का मामला था। राज्य में क्या होगा?
जो भी रामकहानी अभी ऊपर पढ़ें है राज्य के मामले में भी वहीं लागू होता है, कोई अलग प्रावधान नहीं है। बस जिस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है, वहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं क्योंकि वो तो सेम टु सेम वैसे ही लागू हो जाएगा।
लेकिन जहां पर एक सदनीय व्यवस्था है, वहाँ पर केंद्र में जो प्रावधान राज्यसभा के लिए है उसे हटा दीजिए बस। जैसे कि, अगर वहाँ पर दोनों संदनो में पेश किया जाएगा तो यहाँ पर बस एक ही सदन में पेश किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक ही सदन तो है।
✅ राष्ट्रपति किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस ले सकता है। लेकिन वो अपने मन से ऐसा नहीं कर सकता है।
वह किसी भी अध्यादेश को प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सलाह पर ही जारी करता है और उसी की सलाह पर खत्म भी कर सकता है।
जो स्थिति केंद्र में राष्ट्रपति की है वहीं राज्य में राज्यपाल की है मतलब ये कि वे भी इस तरह का निर्णय मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सलाह पर ही ले सकता है।
राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने के संबंध में विशेष प्रावधान
ये एक अकेला ऐसा मामला है जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने के संबंध में अंतर दर्शाता है। दरअसल जब राष्ट्रपति अध्यादेश_ जारी करता है, तब उसे किसी की निर्देश की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन राज्यपाल के मामले में ऐसा नहीं होता है। राज्यपाल को कुछ मामलों में अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति से निर्देश लेना पड़ता है।
? तीन प्रकार की स्थितियाँ है जब राज्यपाल को राष्ट्रपति से निर्देश लेना पड़ता है।
1. ऐसा कोई विधेयक जिसे राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति से आज्ञा लेना जरूरी होता है। इस तरह के मुद्दे पर अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है, जब राष्ट्रपति से आज्ञा ले लिया गया हो।
2. ऐसा को कोई विधेयक जिसे कि राज्य विधानमंडल से पास करवाने के बाद राष्ट्रपति से स्वीकृति लेना पड़ता है। ऐसे मुद्दे पर जब अध्यादेश जारी किया जाएगा तो वह लागू तभी हो पाएगा जब उस अध्यादेश को राष्ट्रपति स्वीकृति दे दे।
3. यदि राज्यपाल को ऐसा लगे कि किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजा जाना चाहिए। यानी कि जहां आज्ञा के साथ-साथ स्वीकृति की भी जरूरत हो। तो ऐसे मामलों में भी राज्यपाल राष्ट्रपति से निर्देश लेता है।
अध्यादेश से जुड़े कुछ तथ्य
✅ एक विधेयक (Bill) की भांति एक अध्यादेश_ भी पूर्ववर्ती (Retrospective) हो सकता है अर्थात इसे पिछली तिथि से प्रभावी (लागू) किया जा सकता है।
✅ चूंकि अध्यादेश एक सामान्य कानून की भांति ही काम करता है इससे वो लगभग वो सब कुछ किया जा सकता है जो किसी सामान्य कानून से किया जा सकता है। पर अध्यादेश_ संविधान संशोधन नहीं कर सकता है।
✅ भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश_जारी करने की शक्ति अनोखी है। ये अनोखी इसलिए है क्योंकि अमेरिका जैसे देश में भी राष्ट्रपति को ये अधिकार नहीं मिला है।
✅ लोकसभा के नियम के अनुसार जब कोई विधेयक किसी अध्यादेश का स्थान लेने के लिए सदन में प्रस्तुत किया जाता है, उस समय अध्यादेश जारी करने के कारण व परिस्थितियों को भी सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
राष्ट्रपति और राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण शक्तियों की तुलना
| राष्ट्रपति | राज्यपाल |
|---|---|
| 1. वह किसी अध्यादेश को केवल तभी प्रख्यापित कर सकता है जब संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में न हो। यानी कि अगर कोई एक सदन भी सत्र में न हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि कोई भी विधि दोनों सदनों द्वारा पारित की जानी होती है न कि एक सदन द्वारा । | 1. वह किसी अध्यादेश को तभी प्रख्यापित कर सकता है, जब विधानमंडल के सदन सत्र में न हो। लेकिन अगर विधानपरिषद भी हो तब अगर कोई एक सदन भी सत्र में न हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। |
| 2. राष्ट्रपति किसी अध्यादेश को तभी प्रख्यापित कर सकता है, जब वह देखे कि ऐसी परिस्थितियाँ बन गयी कि त्वरित कदम उठाना आवश्यक है। | 2. जब वह इस बात से संतुष्ट हो कि अब ऐसी परिस्थितियाँ आ गयी है कि तुरंत कदम उठाया जाना जरूरी है तो वह अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। |
| 3. राष्ट्रपति केवल उन्ही विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है, जिस विषय पर संसद विधि बनाती है। नहीं तो जारी अध्यादेश अवैध हो सकता है, यदि वह संसद द्वारा बना सकने योग्य न हो। | 3. राज्यपाल उन्ही मुद्दों पर अध्यादेश जारी कर सकता है, जिन पर विधानमण्डल को विधि बनाने का अधिकार है। नहीं तो जारी अध्यादेश अवैध हो सकता है, यदि वह विधानमंडल द्वारा बना सकने योग्य न हो। |
| 4. उसके द्वारा जारी कोई अध्यादेश उसी तरह प्रभावी है, जैसे संसद द्वारा निर्मित कोई अधिनियम। | 4. उसके द्वारा अध्यादेश की मान्यता राज्य विधानमंडल के अधिनियम के बराबर ही होता है। |
| 5. वह एक अध्यादेश को किसी भी समय वापस कर सकता है। | 5. वह एक अध्यादेश को किसी भी समय वापस कर सकता है। |
| 6. उसकी अध्यादेश निर्माण की शक्ति स्वैच्छिक नहीं है, इसका मतलब वह कोई विधि बनाने या किसी अध्यादेश को वापस लेने का काम केवल प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही कर सकता है। | 6. उसकी अध्यादेश निर्माण की शक्ति स्वैच्छिक नहीं है इसका मतलब वह कोई विधि बनाने या किसी अध्यादेश को वापस लेने का काम केवल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है। |
| 7. उसके द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखा जाना चाहिए | 7. उसके द्वारा जारी अध्यादेश को विधानमंडल के पटल पर रखा जाना चाहिए। |
| 8. उसके द्वारा जारी अध्यादेश संसद का सत्र प्रारम्भ होने के छह सप्ताह उपरांत समाप्त हो जाता है। यह उस स्थिति में पहले भी समाप्त हो जाता है, जब संसद के दोनों सदन इसे अस्वीकृत करने का संकल्प पारित करें। | 8. उसके द्वारा जारी अध्यादेश राज्य विधानसभा का सत्र प्रारम्भ होने के छह सप्ताह उपरांत समाप्त हो जाता है। यह इससे पहले भी समाप्त हो सकता है, यदि राज्य विधान सभा इसे अस्वीकृति को सहमति प्रदान करें। |
| 9. उस अध्यादेश बनाने में किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं होती। | 9. यह बिना राष्ट्रपति से निर्देश के निम्न तीन मामलों में अध्यादेश नहीं बना सकता यदि – (1) राज्य विधानमंडल में इसकी प्रस्तुति के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, (2) यदि राज्यपाल समान उपबंधों वाले विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आवश्यक माने। (3) यदि राज्य विधानमंडल का अधिनियम ऐसा हो कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना यह अवैध हो जाये। |
अध्यादेश से जुड़े कुछ न्यायिक मामले
38वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा ये व्यवस्था कर दी गयी थी कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश_ को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया था।
एके रॉय बनाम भारत संघ मामला – 1982
इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति के द्वारा लाये गए अध्यादेश न्यायिक पुनर्निरीक्षण के दायरे से बाहर नहीं है।
टी वेंकट रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामला – 1985
इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्यायालय सिर्फ अध्यादेश लाने की प्रक्रिया का न्यायिक पुनर्निरीक्षण कर सकती है। उस अध्यादेश में निहित तत्व का नहीं और अध्यादेश से जुड़े उद्देश्य का नहीं।
डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य मामला – 1987
इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अध्यादेश_(Ordinance) असाधारण परिस्थितियों में उपयोग किया जाने वाला विधायी शक्ति है न कि इसे जब चाहे तब लागू कर दो। क्योंकि अगर अध्यादेश से ही काम चलाया जाने लगा तो फिर सामान्य कानून की जरूरत ही क्या रह जाएगी।
दरअसल हुआ ये था कि 1967-1981 के बीच बिहार के राज्यपाल द्वारा एक अध्यादेश को पुनः जारी कर-कर के चौदह वर्ष तक लगभग 256 अध्यादेश जारी किया गया था।
उम्मीद है आप को राष्ट्रपति और राज्यपाल की अध्यादेश_जारी करने की शक्ति समझ में आया होगा। बेहतर समझ के लिए संबन्धित अन्य लेखों को भी पढ़ें।
अध्यादेश Practice quiz for upsc
⏫राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में जानिए – यहाँ क्लिक करें।
⏫राष्ट्रपति की वीटो पावर को समझिए – यहाँ क्लिक करें।
| 📌 Join YouTube | 📌 Join FB Group |
| 📌 Join Telegram | 📌 Like FB Page |
मूल संविधान↗️
Ordinance making powers of the Executive in India Pinterest पीडीएफ़


![Money bill & Finance bill [धन विधेयक और वित्त विधेयक]](https://wonderhindi.com/wp-content/uploads/2020/10/धन-विधेयक-और-वित्त-विधेयक.jpg)
![राष्ट्रपति शासन : क्यों, क्या, कब और कैसे [बोम्मई मामला सहित]](https://wonderhindi.com/wp-content/uploads/2020/07/President’s-rule.jpg)
![केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध [Concept] #UPSC](https://wonderhindi.com/wp-content/uploads/2020/07/Center-State-Financial-Relations1.jpg)









