इस लेख में हम उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार (Jurisdictions of High Court) एवं शक्तियों पर सरल और सहज चर्चा करेंगे।
भारतीय एकीकृत न्यायिक व्यवस्था में शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद राज्यों के उच्च न्यायालयों का स्थान आता है। किसी राज्य के अंदर ये सबसे बड़ी न्यायालय होती है।
यहाँ तक कि कुछ स्थितियों में दो राज्यों के लिए भी एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है ऐसे में इसका न्यायक्षेत्र या क्षेत्राधिकार काफी व्यापक हो जाता है।

| 📖 Read in English |
उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार
हमने उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के बारे में समझा, कुल मिलाकर वहाँ हमने देखा कि एक लोकतंत्र के हिसाब से हर जरूरी स्वतंत्रता उच्च न्यायालय को दी गई है।
कोई संस्था स्वतंत्र है इसमें अपने आप में निहित है कि उसका अपना एक क्षेत्र होगा जहां वह अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करता होगा या फिर अपनी शक्तियों का अनुप्रयोग करता होगा।
चूंकि हमारी न्यायिक व्यवस्था एकीकृत व्यवस्था पर आधारित है जहां उच्च न्यायालय का स्थान उच्चतम न्यायालय के बाद आता है, उस हिसाब से उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, उच्चतम न्यायालय से थोड़ा सीमित जरूर है पर एक राज्य क्षेत्र के हिसाब से ठीक ही है।
एक उच्च न्यायालय राज्य में अपील करने का सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक होता है इसके पास भी संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होता है। इसके अलावा इसकी पर्यवेक्षक एवं सलाहकार की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है।
हालांकि उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन संविधान में विस्तार से किया गया है लेकिन उच्च न्यायालय के मामले में ऐसा नहीं है। इसमें उस तरह से विस्तारित नहीं किया गया है बस अनुच्छेद 225 में केवल इतना कहा गया है कि एक उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ वही होंगी जो संविधान के लागू होने से तुरंत पूर्व थी।
हालांकि कालांतर में इसमें कई और चीज़ें जोड़ी गई है जैसे कि राजस्व मामलों पर उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार (जो संविधान-पूर्व काल में इसके पास नहीं था)। इसके अलावा न्यायदेश, पर्यवेक्षण की शक्ति, परामर्श की शक्ति आदि भी दी गई है।
अगर संसद और राज्य विधानमंडल चाहे तो उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार या न्यायक्षेत्र में परिवर्तन ला सकती है। वर्तमान की बात करें तो उच्च न्यायालयों के पास निम्नलिखित क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ हैं:-
1. उच्च न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार –
इसका अर्थ ये है कि निम्नलिखित मामलों के विवादों में उच्च न्यायालय प्रथम दृष्टया (Prima facie) सीधे सुनवाई करेगा, न कि अपील के जरिये।
(1) अधिकारिता का मामला, वसीयत, विवाह, तलाक कंपनी कानून एवं न्यायालय की अवमानना।
(2) संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल सदस्य के निर्वाचन संबंधी विवाद।
(3) राजस्व मामले या राजस्व संग्रहण के लिए बनाए गए किसी अधिनियम अथवा आदेश के संबंध में।
(4) नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन ।
(5) संविधान की व्याख्या के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय से स्थानांतरित मामलों में।
◾यहाँ पर प्रथम दृष्टया (Prima facie) का मतलब है पहली बार देखते ही जो सत्य प्रतीत होता है, उसके आधार पर निर्णय, भले ही बाद में वो गलत ही क्यों न साबित हो जाए।
2. उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार –
संविधान का अनुच्छेद 226 एक उच्च न्यायालय की नागरिकों कि मूल अधिकारों के प्रवर्तन और अन्य किस उद्देश्य के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध एवं अधिकार प्रेच्छा रिट जारी करने का अधिकार देता है।
हम जानते है कि यही रिट जारी करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को भी है लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत।
और दूसरी बात ये उच्चतम न्यायालय सिर्फ मूल अधिकारों से संबन्धित मामलों पर ही रिट जारी कर सकती है लेकिन उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के अलावा भी अन्य विषयों पर रिट जारी कर सकता है।
कहने का मतलब ये है कि इस मामले में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय से भी ज्यादा है।
चंद्रकुमार मामले 1997 में उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार को संविधान के मूल ढांचे के अंग के रूप में माना। इसका मतलब ये है कि संविधान संशोधन के जरिये भी इसमें कुछ जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है।
3. उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार –
कानून के क्षेत्र में अपील एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत निचले अदालतों के निर्णय को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाती है। ये व्यवस्था त्रुटि सुधार की प्रक्रिया के साथ-साथ कानून को स्पष्ट और व्याख्या करने की एक प्रक्रिया के रूप में भी कार्य करती है।
उच्च न्यायालय भी मूलतः एक अपीलीय न्यायालय (Appellate Court) ही है। जहां इसके क्षेत्र के तहत आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई होती है। यहाँ दोनों तरह के सिविल एवं आपराधिक मामलों के बारे अपील होती है।
हालांकि कुछ मामलों में इसके पास प्रथम दृष्टया (Prima facie) सीधे सुनवाई करने का भी अधिकार होता है जिसे कि हमने ऊपर पढ़ा है। पर अपीलीय क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र इसके मूल न्यायिक क्षेत्र से ज्यादा विस्तृत है।
(1) दीवानी मामले (civil cases) – इस संबंध में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कुछ इस प्रकार है:
1. जिला न्यायालयों, अतिरिक्त जिला न्यायालयों एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों और निर्णयों को प्रथम अपील के लिए सीधे उच्च न्यायालय में लाया जा सकता है,
2. जिला न्यायालयों एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों और निर्णय के विरुद्ध दूसरी अपील, जिसमें कानून का प्रश्न हो तथ्यों का नहीं,
3. प्रशासनिक एवं अन्य अधिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय की खंड पीठ के सामने की जा सकती है। 1997 मे उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि ये अधिकरण उच्च न्यायालय के न्यायादेश क्षेत्राधिकार के विषयाधीन है।
परिणामस्वरूप किसी पंचायत के फैसले के खिलाफ पीड़ित व्यक्ति बिना पहले उच्च न्यायालय गए सीधे उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता।
(2) आपराधिक मामले (Criminal cases) – उच्च न्यायालय का आपराधिक मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार कुछ इस प्रकार है:
1. सत्र न्यायालय और अतिरिक्त सत्र न्यायालय के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में तब अपील की जा सकती है जब किसी को सात साल से अधिक सजा हुई हो।
यहाँ पर के बात याद रखिए कि कि सत्र न्यायालय या अतिरिक्त सत्र न्यायालय द्वारा दी गई सजा-ए-मौत पर कार्यवाही से पहल उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की जानी होती है। भले ही सजा पाने वाले व्यक्ति ने कोई अपील कि हो या न की हो।
2. आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) के कुछ मामले में सहायक सत्र न्यायाधीश, नगर दंडाधिकारी या अन्य दंडाधिकारी के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
| Compoundable and Non-Compoundable Offences | Hindi |
| Cognizable and Non- Cognizable Offences | Hindi |
| Bailable and Non-Bailable Offences | Hindi |
4. उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षक क्षेत्राधिकार –
उच्च न्यायालय को इस बात का अधिकार है कि वह अपने क्षेत्राधिकार के क्षेत्र के सभी न्यायालयों व सहायक न्यायालयों के सभी गतिविधियों पर नजर रखे। (सिवाय सैन्य न्यायालयों और अभिकरणों के)।
इसके तहत वह –
1. निचले अदालतों से मामले वहाँ से स्वयं के पास मँगवा सकता है।
2. सामान्य नियम तैयार और जारी कर सकता है, और उसने प्रयोग और कार्यवाही को नियमित करने के लिए प्रपत्र निर्धारित कर सकता है।
3. उनके द्वारा रखे जाने वाले लेखा सूची आदि के लिए प्रपत्र निर्धारित कर सकता है।
4. क्लर्क, अधिकारी एवं वकीलों के शुल्क आदि निश्चित करता है।
पर्यवेक्षण के मामले में उच्च न्यायालय की शक्तियाँ बहुत ही व्यापक है क्योंकि,
(1) यह सभी न्यायालयों एवं सहायकों पर विस्तारित होता है चाहे वे उच्च न्यायालय में अपील के क्षेत्राधिकार में हो या न हो,
(2) उसमें न केवल प्रशासनिक प्रयवेक्षण बल्कि न्यायिक पर्यवेक्षण भी शामिल है,
(3) उच्च न्यायालय स्वयं संज्ञान ले सकता है, किसी पक्ष द्वारा प्रार्थनापत्र आवश्यक नहीं है।
उच्च न्यायालय की ये शक्तियाँ असीमित नहीं होती है बल्कि सामान्यत: यह (1) क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण (2) नैसर्गिक न्याय का घोर उल्लंघन (3) विधि की त्रुटि (4) उच्चतर न्यायालयों कि विधि के प्रति असम्मान या (5) अनुचित निष्कर्ष और प्रकट अन्याय तक सीमित होती है।
5. अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण –
उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण रखती है न सिर्फ अपीलीय क्षेत्राधिकार या पर्यवेक्षक क्षेत्राधिकार के तहत बल्कि प्रशासनिक नियंत्रण भी रखती है। क्योंकि
(1) जिला न्यायाधीशों कि नियुक्ति, तैनाती और पदोन्नति एवं व्यक्ति की राज्य न्यायिक सेवा में नियक्ति के लिए राज्यपाल उच्च न्यायालय से परामर्श लेता है।
(2) यह राज्य कि न्यायिक सेवा (जिला न्यायाधीशों के अलावा) के तैनाती स्थानांतरण, सदस्यों के अनुशासन, अवकाश स्वीकृति, पदोन्नति आदि मामलों को भी देखता है।
(3) यह अधीनस्थ न्यायालय में लंबित किसी ऐसे मामले को वापस ले सकता है, जिसमें महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न या फिर संविधान की व्याख्या की आवश्यकता हो। यह या तो इस मामले को निपटा सकता है या अपने निर्णय के साथ मामले को संबन्धित न्यायालय को लौटा सकता है
(6) जैसे उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून को मानने के लिए भारत के सभी न्यायालय बाध्य होते हैं, उसी प्रकार उच्च न्यायालय के कानून को उन सभी अधीनस्थ न्यायालयों को मानने की बाध्यता होती है, जो उसके न्यायिक क्षेत्र में आते हैं।
6. अभिलेख न्यायालय (Court of record) –
अनुच्छेद 215 में इसकी चर्चा की गई है। उच्चतम न्यायालय की तरह ही उच्च न्यायालय के पास भी अभिलेख न्यायालय के रूप में दो शक्तियाँ है:
(1) उच्च न्यायालय की कार्यवाही एव उसके फैसले सार्वकालिक अभिलेख व साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं। खास बात ये है कि अन्य अदालत में चल रहे मामले के दौरान इन अभिलेखों पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। बल्कि उसका इस्तेमाल मार्गदर्शन के लिए या विधिक संदर्भों में किया जाता है।
(2) इसे न्यायालय की अवमानना पर साधारण कारावास या आर्थिक दंड या दोनों प्रकार के दंड देने का अधिकार है। इसमें 6 वर्ष के लिए सामान्य जेल या 2000 रुपए तक अर्थदण्ड या दोनों शामिल है।
न्यायालय की अवमानना किसे कहा जाएगा इसे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया था इसीलिए न्यायालय की अवहेलना अधिनियम 1971 में इसे परिभाषित किया गया है। इसके तहत अवहेलना दीवानी अथवा आपराधिक किसी भी प्रकार की हो सकती है।
सिविल अवमानना का अर्थ है एक न्यायालय के किसी भी निर्णय, आदेश, न्यायदेश अथवा अन्य प्रक्रिया का जान बूझकर पालन न करना।
वहीं आपराधिक अवहेलना का मतलब है किसी ऐसे मामले का प्रकाशन या ऐसी कार्यवाही करना जिसमें न्यायालय को कलंकित या उसके प्राधिकार को कम करने का इरादा हो, या न्यायिक कार्यवाही के प्रति दुराग्रह अथवा उसमें हस्तक्षेप की कोशिश हो, या फिर अन्य किसी प्रकार से न्यायिक प्रशासन में अवरोध अथवा हस्तक्षेप हो।
◾ हालांकि निर्दोष प्रकाशन एवं कुछ मामलों का वितरण, न्यायिक कार्यवाही की सही पत्रकारिता, उचित एवं वाजिब न्यायिक आलोचना, कार्यवाही, प्रतिक्रिया आदि न्यायालय की अवहेलना नहीं है।
अभिलेख न्यायालय के रूप में, एक उच्च न्यायालय को किसी मामले के संबंध में दिये गए अपने स्वयं के आदेश अथवा निर्णय की समीक्षा की और उसमें सुधार की शक्ति प्राप्त है।
यद्यपि इस संबंध में संविधान द्वारा इसे कोई विशिष्ट शक्ति प्रदान नहीं की गई है। दूसरी ओर, उच्चतम न्यायालय को संविधान ने विशिष्ट रूप से अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान की है।
7. न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति (The power of judicial review) –
उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता के परीक्षण के लिए है।
इसके तहत यदि कोई कानून या कोई प्रावधान संविधान का उल्लंघन करने वाले है तो उन्हे असंवैधानिक और सामान्य घोषित किया जा सकता है। परिणामस्वरूप, सरकार उन्हे लागू नहीं कर सकती। बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय की तरह।
न्यायिक समीक्षा शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है लेकिन अनुच्छेद 13 और 226 में उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा के उपबंध स्पष्ट है। अनुच्छेद 13 और 226 को न्यायिक समीक्षा (judicial review) वाले लेख में समझाया गया है।
भारत में किसी विधायी अधिनियम अथवा कार्यपालिकीय आदेश की संवैधानिक वैधता को उच्च न्यायालय में तीन आधारों पर चुनौती दी जा सकती है;
1. यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है,
2. यह उस प्राधिकारी की सक्षमता से बाहर का है जिसने इसे बनाया है, तथा
3. यह संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल है या संविधान की मूल ढांचा को क्षति पहुंचाता है।
भारत के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार
| नाम | स्थापना वर्ष | न्यायक्षेत्र |
|---|---|---|
| 1. त्रिपुरा | 2013 | त्रिपुरा |
| 2. मेघालय | 2013 | मेघालय |
| 3. मणिपुर | 2013 | मणिपुर |
| 4. उत्तराखंड | 2000 | उत्तराखंड |
| 5. झारखंड | 2000 | झारखंड |
| 6. छतीसगढ़ | 2000 | छतीसगढ़ |
| 7. सिक्किम | 1975 | सिक्किम |
| 8. हिमाचल प्रदेश | 1971 | हिमाचल प्रदेश |
| 9. दिल्ली | 1966 | दिल्ली |
| 10. गुजरात | 1960 | गुजरात |
| 11. केरल | 1958 | केरल और लक्षद्वीप |
| 12. मध्य प्रदेश | 1956 | मध्य प्रदेश |
| 13. हैदराबाद | 1954 | आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना |
| 14. राजस्थान | 1949 | राजस्थान |
| 15. उड़ीसा | 1948 | उड़ीसा |
| 16. गुवाहाटी | 1948 | असम, नागालैंड, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश |
| 17. जम्मू एवं कश्मीर | 1928 | जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख |
| 18. पटना | 1916 | बिहार |
| 19. कर्नाटक | 1884 | कर्नाटक |
| 20. पंजाब एवं हरियाणा | 1875 | पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ |
| 21. इलाहाबाद | 1966 | उत्तर प्रदेश |
| 22. बंबई | 1862 | महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नागर हवेली |
| 23. कलकत्ता | 1862 | पश्चिम बंगाल तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह |
| 24. मद्रास | 1982 | तमिलनाडुऔर पुडुचेरी |
कुल मिलाकर ये उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार या न्यायक्षेत्र (Jurisdictions of High Court) है, उम्मीद है समझ में आया होगा। इससे आगे आपको अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Courts) को समझना चाहिए।
उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार प्रैक्टिस क्विज
न्यायालय से संबन्धित अन्य लेखों का लिंक
भारत की राजव्यवस्था
मूल संविधान
https://en.wikipedia.org/wiki/High_courts_of_India

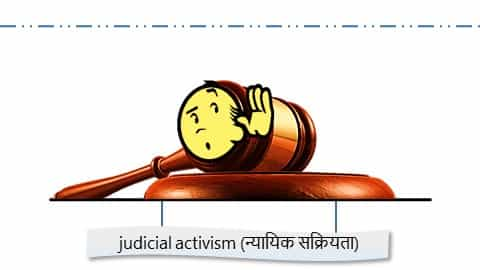
![शोषण के विरुद्ध अधिकार [Right against exploitation]](https://wonderhindi.com/wp-content/uploads/2020/05/शोषण-के-विरुद्ध-अधिकार-1.jpg)
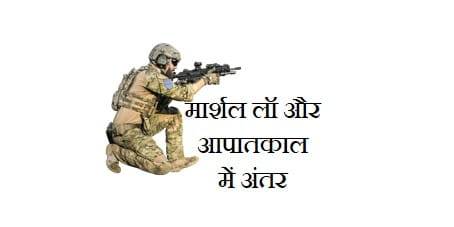
![भारत की संघीय व्यवस्था । Federal System of India [UPSC]](https://wonderhindi.com/wp-content/uploads/2020/06/भारत-की-संघीय-व्यवस्था.jpg)