इस लेख में हम उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार (Jurisdiction of Supreme Court) एवं शक्तियों पर सरल और सहज चर्चा करेंगे,
भारतीय एकीकृत न्यायिक व्यवस्था में उच्चतम न्यायालय सबसे शीर्ष पर है ऐसे में स्वाभाविक है कि इसका क्षेत्राधिकार भी सबसे ज्यादा होगा।
इस लेख को अच्छी तरह से समझने के लिए पहले उच्चतम न्यायालय (Supreme court) को अवश्य समझ लें।
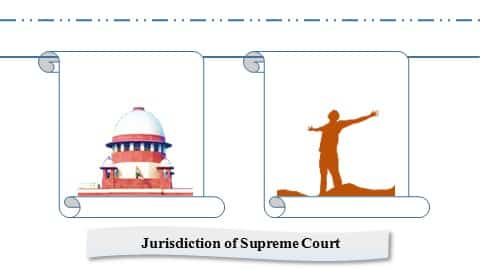
उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां
एक लोकतंत्र के हिसाब से हर जरूरी स्वतंत्रता सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। ऐसे में कोई संस्था स्वतंत्र है इसमें अपने आप में निहित है कि उसका अपना एक क्षेत्र होगा जहां वह अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करता होगा या फिर अपनी शक्तियों का अनुप्रयोग करता होगा।
चूंकि हमारी न्यायिक व्यवस्था एकीकृत व्यवस्था पर आधारित है जहां सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर चोटी पर स्थित है। यह अपील का अंतिम न्यायालय है एवं यह संविधान और भारत के नागरिकों के अधिकारों का व्याख्याता एवं गारंटर भी है।
ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार व्यापक तो होगा ही। कितना व्यापक है इसका वर्णन संविधान में मिलता है जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले है।

“भारत के उच्चतम न्यायालय को विश्व के किसी अन्य सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में ज्यादा शक्तियाँ प्राप्त है।”
— अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर
⚫ उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को निम्नलिखित तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है –
1. अपीलीय क्षेत्राधिकार (Appellate jurisdiction)
2. मूल क्षेत्राधिकार (Original jurisdiction)
3. असाधारण मूल क्षेत्राधिकार (Extraordinary original jurisdiction) या न्यायदेश क्षेत्राधिकार
4. सलाहकार क्षेत्राधिकार (Advisory jurisdiction)
5. अभिलेखों का न्यायालय (Court of records)
6. न्यायिक समीक्षा की शक्ति (Power of judicial review)
7. अन्य शक्तियाँ (Other powers)
1. अपीलीय क्षेत्राधिकार
जैसा कि ऊपर भी बताया गया है सुप्रीम कोर्ट अपील का सबसे उच्चतम न्यायालय है। होता ये है कि अगर किसी को अधीनस्थ न्यायालय का फैसला उचित नहीं लगता है तो उच्च न्यायालय में अपील कर देता है, अगर उच्च न्यायालय का फैसला भी उचित नहीं जान पड़ता है तो फिर इसे उच्चतम न्यायालय में अपील कर देता है।
अब सवाल ये है कि किस प्रकार का अपील उच्चतम न्यायालय में किया जाता है। तो इसे निम्नलिखित चार भागों में बाँट कर देखा जा सकता है।
(1) संवैधानिक मामलों में अपील,
(2) दीवानी मामलों में अपील,
(3) आपराधिक मामलों में अपील, और
(4) विशेष अनुमति द्वारा अपील। आइये इसे एक-एक करके समझते है।
(1) संवैधानिक मामलों में अपील (Appeal in constitutional matters) – अनुच्छेद 132 के तहत, संवैधानिक मामलों में उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के किसी भी फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है, भले ही वह आपराधिक मामला हो या फिर दीवानी।
लेकिन उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 134 (A) के तहत बताना होगा कि (1) ये एक ऐसा मामला है जिसका निराकरन उच्चतम न्यायालय ही कर सकता है, और (2) इसमें संवैधानिक व्याख्या की जरूरत पड़ेगी।
संवैधानिक व्याख्या का सीधा सा मतलब है कि किसी चीज़ को क्या समझा जाये। जैसे कि निजता को ही ले लें तो इस संबंध में सब की अपनी-अपनी सोच होती है, कोई इसे जरूरी मानता है तो कोई नहीं।
लेकिन अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निजता की व्याख्या करते हुए कहा कि अब से ये एक मूल अधिकार है और अगर आप जी रहे है तो निजता आपके उसी जीवन का एक हिस्सा है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता।
(2) दीवानी मामलों में अपील (Appeal in civil cases) – अनुच्छेद 133 के तहत, दीवानी मामलों को उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है।
(घर-गृहस्थी से संबन्धित जो झगड़े होते है उसे दीवानी मामला कहा जाता है जैसे कि शादी से संबन्धित, तलाक से संबन्धित, गोद लेने से संबन्धित इत्यादि मामले)
यहाँ भी वही व्यवस्था है कि उच्च न्यायालय को प्रमाणित करना पड़ेगा कि (1) ये उसके बस की बात नहीं है अब इसे आप ही संभालिए, यानी कि जिसका निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक हो और (2) वो मामला किसी तरह की व्याख्या की मांग करता हो।
(3) आपराधिक मामलों में अपील (Appeal in criminal cases) – अनुच्छेद 134 के तहत, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के आपराधिक मामलों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई करता है,
यदि उच्च न्यायालय ने,
(1) आरोपी व्यक्ति के बरी के आदेश को पलट दिया हो और उसे सजा ए मौत दी हो,
(2) किसी अधीनस्थ न्यायालय से मामला लेकर आरोपी व्यक्ति को दोषसिद्ध किया हो, और उसे सजा ए मौत दे दी हो,
(3) अगर उच्च न्यायालय इस तरह के मामले को अनुच्छेद 134 (A) के तहत प्रमाणित कर देता है कि ये मामला उच्चतम न्यायालय में ले जाने योग्य है।
1970 में संसद ने उच्चतम न्यायालय के आपराधिक अपीलीय न्यायक्षेत्र में विस्तार किया। यानी कि उसके बाद से अब उच्च न्यायालय के किसी भी फैसले पर अपील हो सकती है भले ही आरोपी को दोषमुक्त ही क्यों न कर दिया गया हो।
(4) विशेष अनुमति द्वारा अपील (Appeal by special permission) – सैन्य अदालतों के मामलों को छोड़कर अन्य किसी भी अदालतों के किसी भी प्रकार के मामलों के संबंध में उच्चतम न्यायालय को इस बात का अधिकार है कि वे किसी पीड़ित या असंतुष्ट व्यक्ति के मामले को विशेष अनुमति द्वारा सीधे अपने पास सुनवाई का मौका दे। भले ही कोई भी अदालत उस मामले में अपना जजमेंट ही क्यों न सुना दिया हो।
यह अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट को मिला एक विशेषाधिकार है जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है यदि उसे लगता है कि,
(1) मामला संवैधानिक व्याख्या की मांग करता है, या
(2) उस अमुक व्यक्ति के साथ बहुत अन्याय हुआ है। लेकिन यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है कि यह एक विवेकानुसार शक्ति है और इसीलिए किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा इसका अधिकार के रूप मे दावा नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है वे इस अधिकार का इस्तेमाल करता है कि नहीं।
इस तरह इस उपबंध का कार्यक्षेत्र काफी व्यापक है और इसकी पूर्ण सुनवाई उच्चतम न्यायालय में निहित है। इस शक्ति का उपयोग उच्चतम न्यायालय सावधानी के साथ विशेष परिस्थितियों में ही बिरले रूप में ही करता है क्योंकि इस शक्ति का प्रयोग किसी भी नियम के तहत करना मुश्किल होता है।
2. मूल क्षेत्राधिकार (Original jurisdiction)
अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है। किसी भी संघीय व्यवस्था वाले देश में केंद्र और राज्य या फिर राज्य और राज्य के बीच विवाद होना स्वाभाविक है इसी प्रकार के विवाद को निपटाने की जो शक्ति उच्चतम न्यायालय के पास है उसी को मूल क्षेत्राधिकार कहा जाता है।
इसी बात को संविधान में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि किसी भी विवाद को जो –
(1) केंद्र व एक या अधिक राज्यों के बीच हो, या
(2) केंद्र और कोई राज्य या फिर राज्यों का एक तरफ होना एवं एक या अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना, या
(3) दो या अधिक राज्यों के बीच, किसी विवाद में यदि ऐसा कोई प्रश्न अंतर्वलित है जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है तो वहाँ तक उच्चतम न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार होगी।
इस तरह के मामले में उच्चतम न्यायालय को दो बातों का ध्यान रखना होता है। पहला, विवाद से कुछ इस तरह का प्रश्न खड़ा होता हो जो किसी कानून, किसी तथ्य या संविधान की व्याख्या की मांग करता हो। दूसरा, इस तरह के विवादों के मामले किसी नागरिक के द्वारा न्यायालय में न लाया गया हो।
हालांकि उच्चतम न्यायालय के इस न्यायक्षेत्र की सीमा भी है जो कुछ इस प्रकार है-
(1) कोई ऐसी संधि या समझौता जिसमें ये लिखा हुआ हो कि इसका न्यायक्षेत्र उच्चतम न्यायालय नहीं होगा तो फिर उस संधि या समझौते के तहत जो विवाद होगा वे उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से बाहर होंगे,
(2) अंतर्राज्यीय जल विवाद के मामले भी इसके मूल क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं क्यों होते है इसके लिए आप इस लेख को पढ़ सकते हैं।
(3) वित्त आयोग के संदर्भ वाले मामले या फिर केंद्र एवं राज्यों के बीच कुछ खर्चों के समझौते वाले मामले और केंद्र व राज्यों के बीच वाणिज्यिक प्रकृति वाले साधारण विवाद भी इसके न्यायक्षेत्र से बाहर होते हैं
(4) केंद्र के खिलाफ राज्य के किसी नुकसान की भरपाई का मामला भी इसके न्यायक्षेत्र से दूर होता है।
1961 में मूल न्यायक्षेत्र के तहत पहली बार पश्चिम बंगाल द्वारा केंद्र के खिलाफ मामला लाया गया। राज्य सरकार ने संसद द्वारा पारित ‘कोयला खदान क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम 1957’ की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी।
हालांकि उच्चतम न्यायालय ने अधिनियम की वैधानिकता को मानते हुए इस मुकदमे को खारिज कर दिया था।
| Compoundable and Non-Compoundable Offences | Hindi |
| Cognizable and Non- Cognizable Offences | Hindi |
| Bailable and Non-Bailable Offences | Hindi |
3. असाधारण मूल क्षेत्राधिकार (Extraordinary original jurisdiction)
हमने अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय के रिट जारी करने की शक्ति को समझा था, ये उसी के बारे में है। इसे न्यायदेश क्षेत्राधिकार भी कहा जाता है क्योंकि उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध एवं अधिकार प्रेच्छा जैसे न्यायादेश (रिट) जारी कर सकता है।
इसमें व्यवस्था ये है कि नागरिक बिना अपील याचिका के सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जब किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन राज्य द्वारा हो रहा हो तो वह सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। (यहाँ पर ये याद रखिए कि यहीं शक्ति उच्च न्यायालय के पास भी है)
न्यायदेश क्षेत्राधिकार के मामले में उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय में एक और अंतर है। उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के संबंध में न्यायदेश जारी कर सकता है, अन्य उद्देश्य से नहीं, जबकि दूसरे तरफ उच्च न्यायालय न केवल मूल अधिकारों के न्यायदेश जारी कर सकता है बल्कि अन्य उद्देश्यों के लिए भी इसे जारी कर सकता है।
इसका अभिप्राय है कि न्यायदेश न्यायक्षेत्र के मसले पर उच्च न्यायालय का क्षेत्र ज्यादा विस्तृत है। लेकिन संसद उच्चतम न्यायालय को अन्य उद्देश्यों के लिए न्यायादेश की शक्ति प्रदान कर सकती है।
4. सलाहकार क्षेत्राधिकार (Advisory jurisdiction of Supreme Court)
अनुच्छेद 143 के तहत, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से राय लेने का अधिकार रखता है।
ये राय दो प्रकार का होता है –
(1) सार्वजनिक महत्व के किसी मसले पर विधिक प्रश्न उठने पर। यानी कि यदि किसी भी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर कानून या किसी तथ्य का प्रश्न उत्पन्न हो गया है, या उत्पन्न होने की संभावना है और इस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना जरूरी है, तो वह उस विषय को न्यायालय को विचार के लिए संदर्भित कर सकता है।
लेकिन यहाँ पर ये याद रखिए कि न्यायालय अपना विचार देने के लिए बाध्य नहीं है वो चाहे तो दे भी सकता है चाहे तो नहीं भी।
(2) किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते, आदि मामलो पर किसी विवाद के उत्पन्न होने पर। इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को अपना मत देना अनिवार्य है।
दोनों ही मामलों में उच्चतम न्यायालय का मत सिर्फ सलाह होती है। इस तरह, राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं है वह इस सलाह को माने। यद्यपि सरकार अपने द्वारा निर्णय लिए जाने के संबंध में इसके द्वारा प्राधिकृत विधिक सलाह प्राप्त करती है।
राष्ट्रपति द्वारा अपने सलाहकारी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को सौंपे गए कुछ मामले निम्नवत है:
1. रामजन्म भूमि मामला 1993 में,
2. पंजाब समझौते को समाप्त करने संबंधी अधिनियम (Punjab Termination of Agreements Act) 2004 में,
3. 2जी स्पेक्ट्रम मामले में आया निर्णय तथा प्राकृतिक संसाधनों की सभी क्षेत्रों में नीलामी को बाध्यकारी बनाया जाना, 2012 में
5. अभिलेख का न्यायालय (Court of record)
अनुच्छेद 129 के तहत अभिलेखों के न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय के पास दो शक्तियाँ है –
(1) उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही एव उसके फैसले सार्वकालिक अभिलेख व साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं। खास बात ये है कि अन्य अदालत में चल रहे मामले के दौरान इन अभिलेखों पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। बल्कि उसका इस्तेमाल मार्गदर्शन के लिए या विधिक संदर्भों में किया जाता है।
(2) इसके पास न्यायालय के अवमानना पर दंडित करने का अधिकार है। इसमें 6 वर्ष के लिए सामान्य जेल या 2000 रुपए तक अर्थदण्ड या दोनों शामिल है। 1991 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि दंड देने की यह शक्ति न केवल उच्चतम न्यायालय में निहित है बल्कि ऐसा ही अधिकार उच्च न्यायालयों अधीनस्थ न्यायालयों पंचाटों को भी प्राप्त है।
न्यायालय की अवमानना सिविल या आपराधिक दोनों प्रकार की हो सकती है। सिविल अवमानना का मतलब है स्वेछा से किसी फैसले, आदेश, न्यायादेश की अवहेलना जबकि आपराधिक अवमानना का मतलब किसी ऐसी सामाग्री का प्रकाशन और ऐसा कार्य करना, जिसमें न्यायालय की शक्ति को कमतर आंकना या उसको बदनाम करना या न्यायी प्रक्रिया में बाधा पहुंचाना,या फिर न्याय प्राप्रशासन को किसी भी तरीके से रोकना।
हालांकि किसी मामले का निर्दोष प्रकाशन और उसका वितरण न्यायिक कार्यवाही रिपोर्ट की निष्पक्ष, उचित आलोचना और प्रशासनिक दिशा से इस पर टिप्पणी को न्यायालय की अवमानना में नहीं माना जाता।
6. न्यायिक समीक्षा की शक्ति (Power of judicial review)
उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित है। इसके तहत केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर विधायी व कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जाती है।
इसमें कुछ गरबड़ी पाये जाने पर इन्हे असंवैधानिक और अवैध (बालित और शून्य घोषित किया जा सकता है) तदुपरान्त इन्हे सरकार दारा लागू नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की ये बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है इसे अच्छे से समझने के लिए इस लेख को अवश्य पढ़ें – (भारत में न्यायिक समीक्षा↗️)
इस सब के अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 137 के तहत अपने स्वयं के फैसले की समीक्षा करेने की शक्ति है, इस तरह यह पूर्व के फैसले पर अडिग रहने को बाध्य नहीं है और सामुदायिक हितों व न्याय के हित में वह इससे हटकर भी फैसले ले सकता है।
संक्षेप में उच्चतम न्यायालय स्वयं सुधार संस्था है। उदाहरण के लिए केशवानन्द भारती मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व के फैसले गोलकनाथ मामले 1967 से हटकर फैसला दिया।
7. उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार संबंधी अन्य शक्तियाँ
उपरोक्त शक्तियों के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय को कई अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त है, जैसे-
(1) यह राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में किसी प्रकार के विवाद का निपटारा करता है। इस संबंध में यह मूल, विशेष एवं अंतिम व्यवस्थापक है।
(2) यह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के व्यवहार एवं आचरण की जांच करता है, उस संदर्भ में जिसे राष्ट्रपति द्वारा निर्मित किया गया है।
यदि यह उन्हे दुर्व्यवहार का दोषी पाता है तो राष्ट्रपति से उसको हटाने की सिफ़ारिश कर सकता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई इस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है।
(3) अनुच्छेद 139 (A) के तहत सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों को यह मँगवा सकता है और उनका निपटारा कर सकता है। यह किसी लंबित मामले या अपील को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित भी कर सकता है।
(4) अनुच्छेद 141 के तहत, सुप्रीम कोर्ट की विधियाँ भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्य होंगी। इसके डिक्री या आदेश पूरे देश में लागू होते हैं। सभी प्राधिकारी उच्चतम, न्यायालय की सहायता में कार्य करते हैं।
(5) यह संविधान का इकलौता व्याख्याता है। यह संविधान की विभिन्न उपबंधों एवं उसमें निहित तत्वों को अंतिम रूप प्रदान करता है।
(6) इसे न्यायिक अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है और इसका देश के सभी न्यायालयों एवं पंचाटों के क्रियाकलापों पर नियंत्रण है।
(7) अनुच्छेद 138 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायक्षेत्र एवं शक्तियों को केन्द्रीय सूची से संबन्धित मामलों पर संसद द्वारा विस्तारित किया जा सकता है और इसके न्यायक्षेत्र एवं शक्ति अन्य मामलों में केंद्र एवं राज्यों के बीच विशेष समझौते के तहत विस्तारित किए जा सकते हैं।
(8) अनुच्छेद 139 के तहत कुछ रिट निकालने की शक्तियों को उच्चतम न्यायालय को प्रदत किया जा सकता है। संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के खंड (2) में वर्णित प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए ऐसे निदेश, आदेश या रिट, जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण रिट हैं, या उनमें से कोई निकालने की शक्ति प्रदान कर सकेगी।
(9) अनुच्छेद 140 के तहत संसद, विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को ऐसी अनुपूरक शक्तियाँ प्रदान करने के लिए उपबंध कर सकेगी जो इस संविधान के उपबंधों में से किसी से असंगत न हों और जो उस न्यायालय को इस संविधान द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त अधिकारिता का अधिक प्रभावी रूप से प्रयोग करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हों।
(10) अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में फैसला सुनाते समय संवैधानिक प्रावधानों के दायरे में रहते हुए ऐसा आदेश दे सकता है, जो किसी व्यक्ति को न्याय देने के लिए जरूरी हो। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो किसी खास मामले में न्याय की प्रक्रिया को तार्किक अंजाम तक पहुंचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कर सकता है।
(11) अनुच्छेद 144 के तहत भारत के राज्यक्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे।
(12) अनुच्छेद 145 के तहत संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उच्चतम न्यायालय समय-समय पर, राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया के, विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। जैसे कि –
(क) उस न्यायालय में विधि-व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के बारे में नियम;
(ख) अपीलें सुनने के लिए प्रक्रिया के बारे में और अपीलों संबंधी अन्य विषयों के बारे में नियम;
(ग) भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी का प्रवर्तन कराने के लिए उस न्यायालय में कार्यवाहियों के बारे में नियम; आदि।
(13) अनुच्छेद 146 के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो भारत के मुख्य न्यायमूार्ति या उस न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा, जिसे भारत के मुख्य न्यायमूार्ति ने इस प्रयोजन के लिए नियम बनाने के लिए प्राधिकॄत किया है, बनाएं गए नियमों द्वारा विहित की जाएं: परन्तु इस खंड के अधीन बनाएं गए नियमों के लिए, जहां तक वे वेतनों, भत्तों, छुट्टी या पेंशनों से संबंधित हैं, राष्ट्रपति के अनुमोदन की अपेक्षा होगी ।
दूसरी बात ये कि उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक व्यय, जिनके अतंर्गत उस न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में संदेय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे और उस न्यायालय द्वारा ली गई फीसें और अन्य धनराशियां उस निधि का भाग होंगी ।
(14) अनुच्छेद 147 भारतीय संविधान और अन्य कानूनों की व्याख्या करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति देता है। ये काफी विवादित अनुच्छेद है।
तो ये रहा सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार (Jurisdiction of Supreme Court), उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इससे आगे की लेख को नीचे दिया गया है उसे जरूर पढ़े।
उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार अभ्यास प्रश्न
उच्चतम न्यायालय से संबन्धित अन्य लेख
भारत की राजव्यवस्था↗️
मूल संविधान
supreme court of india Handbook
https://main.sci.gov.in/


![जनहित याचिका (PIL): अर्थ, उद्देश्य, लाभ आदि [UPSC]](https://wonderhindi.com/wp-content/uploads/2021/01/pil.jpg)
![राष्ट्रपति (President): बेसिक अवधारणा [UPSC]](https://wonderhindi.com/wp-content/uploads/2020/07/राष्ट्रपति.jpg)
![संवैधानिक उपचारों का अधिकार [Art 32] UPSC](https://wonderhindi.com/wp-content/uploads/2020/05/संवैधानिक-उपचारों-का-अधिकार1.jpg)