संसद की गरिमा, स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता अक्षुण्ण रहे और ये अपना काम बिना किसी अवरोध के कर सके इसके लिए संसद के सदस्यों और इसके विभिन्न निकायों को संविधान द्वारा कुछ विशेषाधिकार दिये गए हैं, इसे संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privilege) कहा जाता है।
इस लेख में हम इसी संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary privilege) पर सरल और सहज चर्चा करेंगे, एवं इसके विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे।

| 📖 Read in English |
संसदीय विशेषाधिकार का अर्थ (meaning of parliamentary privilege):
संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privilege), वे विशेषाधिकार, उन्मुक्तियाँ और छूटें हैं जो संसद के दोनों सदनों, इसके समितियों और इसके सदस्यों को प्राप्त होते हैं (राष्ट्रपति को नहीं)।
ये विशेषाधिकारें इनके कार्यों की स्वतंत्रता और प्रभाविता के लिए आवश्यक हैं। इन अधिकारों के कारण ही सदन अपनी स्वायत्तता एवं सम्मान को संभाल पाता है। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 105 में किया गया है।
दूसरे शब्दों में कहें तो संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privilege) अनुच्छेद 105 के संवैधानिक प्रावधानों पर आधारित है, जो संसद के सदस्यों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, गिरफ्तारी से स्वतंत्रता, और कानून की अदालत में गवाह के रूप में उपस्थिति से छूट सहित कुछ अधिकार और प्रतिरक्षा प्रदान करता है।
उपर्युक्त वर्णित लोगों और समूहों के अलावा संविधान ने भारत के महान्यायवादी (Attorney General) को भी संसदीय अधिकार दिये हैं। जिसके तहत वे संसद के किसी सदन या इसकी किसी समिति में बोलते और हिस्सा लेते हैं।
[यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है ये है कि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न हिस्सा होता है लेकिन संसद का भाग होते हुए भी राष्ट्रपति को संसदीय विशेषाधिकार नहीं मिलता है इसीलिए इसे सदनीय विशेषाधिकार (Privilege of Houses) भी कहा जाता है।]
संसदीय विशेषाधिकारों का वर्गीकरण (Classification of Parliamentary Privilege):
संसदीय विशेषाधिकारों (Parliamentary Privilege) को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है:
1. सामूहिक विशेषाधिकार (Collective privilege) – ये वे अधिकार हैं, जिन्हे संसद के दोनों सदन सामूहिक रूप से प्रयोग करते हैं, तथा
2. व्यक्तिगत विशेषाधिकार (Personal privilege) – ये वे अधिकार हैं, जिसका उपयोग इसके सदस्य व्यक्तिगत रूप से करते हैं।
आइये इसे विस्तार से समझते हैं –
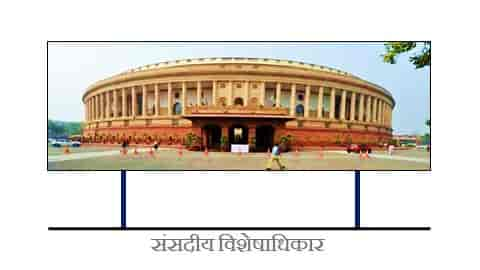
1. सामूहिक विशेषाधिकार (Collective privilege)
संसद के दोनों सदनों के संबंध में सामूहिक विशेषाधिकार कुछ इस प्रकार है:-
1. इसे अपनी रिपोर्ट, वाद-विवाद और कार्यवाही को प्रकाशित करने तथा अन्यों को इसे प्रकाशित न करने देने का अधिकार है।
हालांकि 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम के अनुसार, सदन की पूर्व अनुमति बिना प्रेस संसद की कार्यवाही की सही रिपोर्ट का प्रकाशन कर सकता है, किन्तु यह सदन की गुप्त बैठक के मामले में लागू नहीं है।
2. यह अपनी कार्यवाही से अतिथियों को बाहर कर सकती है तथा कुछ आवश्यक मामलों पर विचार-विमर्श हेतु गुप्त बैठक कर सकती है।
3. यह अपनी कार्यवाही के संचालन एवं प्रबंधन तथा इन मामलों के निर्णय हेतु नियम बना सकती है।
4. यह सदस्यों के साथ-साथ बाहरी लोगों को इसके विशेषाधिकारों के हनन या सदन की अवमानना करने पर चेतावनी या दंड दे सकती है।
5. इसे किसी सदस्य की बंदी, अपराध सिद्ध, कारावास या मुक्ति संबंधी तत्कालीन सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।
याद रखिए, सदन क्षेत्र में पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति (चाहे वो बाहरी हो या सदन का कोई सदस्य) बंदी नही बनाया जा सकता और न ही कोई कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
6. यह जांच कर सकती है तथा गवाह की उपस्थिति तथा संबन्धित पेपर तथा रिकॉर्ड के लिए आदेश दे सकती है
7. न्यायालय, सदन या इसके समिति की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता है।
2. व्यक्तिगत विशेषाधिकार (Personal privilege)
व्यक्तिगत अधिकारों से संबन्धित विशेषाधिकार कुछ इस प्रकार है:-
1. उन्हें संसद की कार्यवाही के दौरान, कार्यवाही शुरू होने से 40 दिन पूर्व तथा कार्यवाही बंद होने के 40 दिन बाद तक बंदी नहीं बनाया जा सकता है।
यहाँ याद रखने वाली बात है कि यह अधिकार केवल नागरिक (civil) मुकदमों में लागू होता है, आपराधिक (Criminal) तथा प्रतिबंधात्मक निषेध (restrictive prohibition) मामलों में नहीं।
2. उन्हें संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता है। किसी सदस्य द्वारा संसद में दिये गए भाषण या किसी मत के लिए, न्यायालय में उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।
3. वे न्यायनिर्णयन सेवा से मुक्त है। वे संसद सत्र के दौरान न्यायालय में लंबित मुक़दमे में प्रमाण प्रस्तुत करने या गवाह के रूप में उपस्थित होने के लिए मना कर सकते हैं।
संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provision):
जैसा कि हमने ऊपर भी समझा कि संविधान के अनुच्छेद 105 में इसका प्रावधान किया गया है। यहाँ संक्षिप्त में इसपर चर्चा की गई है विस्तार से समझने के लिए Article 105 पढ़ें;
संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत कुल चार खंड है, जिसे कि आप नीचे देख सकते हैं;
1. इस संविधान के उपबंधों के और संसद की प्रक्रिया का विनियमन (Regulation) करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए, संसद में बोलने की आजादी (Freedom of speech) होगी।
2. संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
और दूसरी बात ये कि सदन को अपनी रिपोर्ट, वाद-विवाद और कार्यवाही को प्रकाशित करने तथा अन्यों को इसे प्रकाशित न करने देने का अधिकार है, न्यायालय में इस बात के लिए कार्यवाही नहीं की जा सकती।
लेकिन, 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम के अनुसार, सदन की पूर्व अनुमति बिना प्रेस (मीडिया) संसद की कार्यवाही की सही रिपोर्ट का प्रकाशन कर सकता है (हालांकि यह सदन की गुप्त बैठक के मामले में लागू नहीं होता है)।
3. इस खंड में कहा गया है कि संविधान में उल्लिखित विशेषाधिकारों के अलावा अन्य विशेषाधिकारों के संबंध में, संसद के प्रत्येक सदन की, उसके सदस्यों की और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ वही होंगी जो संविधान (44वां संशोधन) अधिनियम, 1978 के प्रवृत्त होने से तुरंत पूर्व उस सदन की, उसके सदस्यों की और समितियों की थी। यानि कि अन्य जो विशेषाधिकार हैं वो वहीं हैं जो 26 जनवरी 1950 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स को प्राप्त था।
यहाँ यह समझना जरूरी है कि अनुच्छेद 105(3) संसद को इस संबंध में विधि बनाने को कहती है लेकिन संसद ने अब तक विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध (Codified) करने के संबंध में कोई विशेष विधि नहीं बनाया है। [क्यों नहीं बनाया है इसे अनुच्छेद 105 में विस्तार से समझाया गया है।]
4. इस खंड के तहत यह व्यवस्था किया गया है कि जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर संसद् के किसी सदन या उसकी किसी समिति में बोलने का और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार है, उनके संबंध में खंड (1), खंड (2) और खंड (3) के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे संसद् के सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं।
संविधान ने कुछ प्रकार के लोगों को संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार दिया है। अनुच्छेद 88 के तहत मंत्रियों और महान्यायवादी को यह अधिकार मिला है कि वह संसद के किसी भी सदन में बोल सकता है। तो इनके ऊपर भी अनुच्छेद 105(1), (2) और (3) खंड लागू होते हैं। यानि कि इनको भी अनुच्छेद 105 के तहत मिलने वाले विशेषाधिकार का लाभ मिलेगा।
| विस्तार से समझने के लिए पढ़ें – Article 105
| Lok Sabha: Role, Structure, Functions | Hindi | English |
| Rajya Sabha: Constitution, Powers | Hindi | English |
| Parliamentary Motion | Hindi | English |
विशेषाधिकारों का हनन एवं सदन की अवमानना (Breach of privilege & Contempt of the House of Parliament):
जब कोई व्यक्ति या प्राधिकारी किसी संसद सदस्य की व्यक्तिगत और संयुक्त क्षमता में इसके विशेषाधिकारों, अधिकारों और उन्मुक्तियों का अपमान या उन पर आक्रमण करता है तो इसे विशेषाधिकार हनन कहा जाता है और यह सदन द्वारा दंडनीय है।
दूसरे शब्दों में कहें तो सदनों, समितियों या संसद के सदस्यों द्वारा अपने कर्तव्यों और कृत्यों का प्रभावी और कुशल ढंग से और बिना भय या पक्षपात के निर्वहन करने में बाधा डालने वाला कोई भी कार्य विशेषाधिकार हनन करने वाला माना जाएगा।
जैसे कि, सदन की बैठक में उपस्थित होने के लिए किसी सदस्य को जाने से रोकना विशेषाधिकार का हनन होगा। इसी तरह से सदन को जानबूझकर गलत जानकारी देना भी विशेषाधिकार का हनन (Breach of Privilege) माना जा सकता है।
यहाँ यह याद रखिए कि कुछ ऐसे भी मामले हैं जिनसे विशेषाधिकार भंग नहीं होता है; जैसे कि
- ऐसी परंपरा या मान्यता है कि संसदीय सदस्यों या अन्य लोगों द्वारा सार्वजनिक समारोहों में संसद के सदस्यों के प्रति उचित शिष्टता दिखानी चाहिए; लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे विशेषाधिकार का हनन नहीं माना जाता है।
- जब सदन का अधिवेशन चल रहा हो तो नीति संबंधी वक्तव्य सदन से बाहर नहीं देने चाहिए; लेकिन कोई सदस्य अगर ऐसा करता है तो उसे विशेषाधिकार का हनन नहीं माना जाता है।
वहीं सदन की अवमानना (Contempt) की बात करें तो, किसी भी तरह का कृत्य या चूक जो सदन, इसके सदस्यों या अधिकारियों के कार्य संपादन में बाधा डाले, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसद की मर्यादा शक्ति तथा सम्मान के विपरीत परिणाम दे, संसद की अवमानना (Contempt of the House of Parliament) माना जाएगा। उदाहरण के लिए,
- कार्यवाहियों को गलत ढंग से प्रकाशित करना।
- लोक सभा अध्यक्ष या राज्य सभा सभापति द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उसके चरित्र या निष्पक्षता को चुनौती देना।
- सदस्यों को उनके संसदीय आचरण से प्रभावित करने के लिए उन्हे घूस देना या घूस ऑफर करना।
- सदस्यों के संसदीय आचरण के संबंध में उन्हे डराना।
सामान्यतः विशेषाधिकार हनन, सदन की अवमानना हो सकती है। और इसी प्रकार सदन की अवमानना में भी विशेषाधिकार हनन शामिल हो सकता है।
लेकिन यहाँ याद रखने वाली बात है कि विशेषाधिकार हनन के बिना भी सदन की अवमानना हो सकती है। उदाहरण के लिय सदन के विधायी आदेश कों न मानना विशेषाधिकार का हनन नहीं है, परंतु सदन की अवमानना जरूर है।
कुल मिलाकर यहाँ समझने वाली बात ये है कि अवमानना शब्द की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। इसीलिए इसका अर्थ व्यापक हो जाता है क्योंकि किसे सदन का अवमानना माना जाएगा और किसे नहीं यह अंततः सदन ही तय करता है।
Q. सदन विशेषाधिकार संबंधी प्रश्नों को कैसे तय करता है?
मामले उठाने की प्रक्रिया – कोई भी सदस्य विशेषाधिकार संबंधी मुद्दे संसद के पटल पर रख सकता है। लेकिन याद रखिए कि सदन में विशेषाधिकार के मुद्दे उठाने की अनुमति केवल उसी सदस्य को दी जा सकती है, जिसने विशेषाधिकार के संदर्भ में महासचिव को सूचना दी है।
यदि अध्यक्ष चाहे तो इस तरह के मुद्दे को प्रथम दृष्टया (Prima facie) देखने के बाद आगे बढ़ाने से इंकार भी कर सकता है।
लेकिन यदि अध्यक्ष द्वारा सदन में संबंधित सदस्य को विशेषाधिकार संबंधी कोई मामला उठाने के लिये कहता है, तो वह सदस्य उस विशेषाधिकार के प्रश्न से संबन्धित एक संक्षिप्त वक्तव्य देता है।
◾ यदि इसके बाद संसद के अन्य सदस्यों द्वारा अनुमति के संबंध में आपत्ति जतायी जाती है तो अध्यक्ष उन सदस्यों से अपने स्थान पर खड़े हो जाने के लिए अनुरोध करता है जो विशेषाधिकार मामले उठाने वाले सदस्य के पक्ष में हैं।
◾ यदि पच्चीस या इससे अधिक सदस्य खड़े हो जाते हैं तो यह माना जाता है कि सदन ने मामले को उठाए जाने की अनुमति दे दी है तब अध्यक्ष यह घोषणा करता है कि अनुमति दी जाती है और यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो अध्यक्ष उस सदस्य को सूचित कर देता है कि उसे सदन ने उस विशेषाधिकार मामले को उठाने की अनुमति नहीं दी है।
◾ सदन द्वारा यदि अनुमति दी जाती है तो ऐसी स्थिति में या तो सदन स्वयं उस मामले की जांच कर सकता है या फिर उसे विशेषाधिकार समिति को सौंप सकता है।
आमतौर पर यदि मामले तुच्छ प्रकृति की होती है या फिर जब अपराधी स्वयं ही माफी मांग लेता है तो इस स्थिति को सदन स्वयं ही निपटा लेता है। लेकिन अगर गंभीर किस्म का मामला हो तो उसे विशेषाधिकार समिति (Privilege Committee) को सौंप दिया जाता है।
अब सवाल यही आता है कि विशेषाधिकार समिति (Privilege Committee) क्या होता है?
विशेषाधिकार समिति (Privileges Committee) क्या है?
जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि संसद के सदस्यों और समितियों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होती हैं। जब इन विशेषाधिकारों के हनन होने का प्रश्न उत्पन्न होता है, या हनन हो जाता है तो उसे जांच करने के लिए और उस पर रिपोर्ट देने के लिए विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया जा सकता है।
दोनों सदनों का अपना-अपना विशेषाधिकार समिति होता है जो पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष गठित किया जाता है।
◾ लोकसभा द्वारा गठित इस समिति में 15 सदस्य और राज्यसभा द्वारा गठित समिति में 10 सदस्य होते हैं। समिति का कार्य अर्ध-न्यायिक प्रकृति का होता है फिर भी अगर ये कभी सिफ़ारिशें करती है तो आमतौर पर इसे नजरंदाज नहीं किया जाता है।
◾ मामले की उचित जांच-पड़ताल करने के बाद समिति एक रिपोर्ट तैयार करता है और उसे संबंधित सदन के समक्ष प्रस्तुत करता है।
◾ फिर सदन उस रिपोर्ट पर विचार करता है। सदन चाहे तो उस रिपोर्ट से सहमत हो सकता है या फिर असहमत हो सकता है फिर संशोधनों के साथ सहमत हो सकता है।
| यहाँ से समझें – संसदीय समितियां (अर्थ, प्रकार, समझ)
संसदीय विशेषाधिकार का स्रोत (Sources of Parliamentary Privilege):
मूल रूप में, संविधान के अनुच्छेद 105 में दो विशेषाधिकार बताए गए हैं:- संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता और इसकी कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार। अन्य विशेषाधिकार ब्रिटेन के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों के समान ही माना जाता है (जैसा कि हमने ऊपर भी समझा)।
यहाँ यह समझना जरूरी है कि अनुच्छेद 105(3) संसद को इस संबंध में विधि बनाने को कहती है लेकिन संसद ने अब तक विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध (Codified) करने के संबंध में कोई विशेष विधि नहीं बनाया है।
इसीलिए आमतौर पर संसदीय विशेषाधिकार 5 स्रोतों पर आधारित होता है:- 1. संवैधानिक उपबंध, 2. संसद द्वारा निर्मित अनेक विधियाँ, 3. दोनों सदनों के नियम, 4. संसदीय परंपरा, और; 5. न्यायिक व्याख्या।
संसदीय विशेषाधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता (Parliamentary Privilege and Freedom of the Press):
प्रेस को संसद का विस्तार माना जाता है क्योंकि प्रेस ही संसदीय विधान या चर्चाओं को जनता तक पहुंचाता है। अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित है।
लेकिन दिक्कत अनुच्छेद 105(2) के कारण होती है क्योंकि इस खंड के तहत संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाहियों के प्रकाशन से संबंधित सभी व्यक्तियों को किसी न्यायालय में कार्यवाही से पूर्ण उन्मुक्ति (immunity) प्रदान की गई है यदि ऐसा प्रकाशन सदन द्वारा सदन के प्राधिकार से किया जाय।
लेकिन यही उन्मुक्ति ससदीय कार्यवाहियों की रिपोर्ट समाचारपत्रों में प्रकाशित करने के मामले में प्रदान नहीं की गई है, जब तक कि किसी सदन द्वारा ऐसे प्रकाशन के लिए स्पष्टतः प्राधिकृत न किया गया हो।
ऐसी व्यवस्था इसीलिए की गई ताकि सदन अपने वाद-विवाद एवं कार्यवाहियों के प्रकाशन पर नियंत्रण रख सके और यदि आवश्यक हो तो उल्लंघन करने वाले को दंड भी दे सके।
◾ हालांकि आमतौर पर सदन की कार्यवाहियों की रिपोर्ट प्रकाशित करने पर को प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। इसकी एक वजह 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 का वो नियम है जिसके तहत, सदन की पूर्व अनुमति बिना प्रेस (मीडिया) संसद की कार्यवाही की सही रिपोर्ट का प्रकाशन कर सकता है।
◾ हालांकि यह याद रखिए कि यदि कोई रिपोर्ट दुर्भावना से की गई हो या फिर किन्ही भाषणों को जान-बूझकर गलत रूप दिया गया हो या साक्ष्य छिपाया गया हो तो इसे विशेषाधिकार भंग या सदन की अवमानना माना जा सकता है। और इसके लिए दोषी व्यक्ति को दंड भी दिया जा सकता है।
◾ यदि प्रेस द्वारा किसी समिति के रिपोर्ट को सदन में पेश होने से पहले ही मीडिया में प्रकाशित कर दिया जाता है तो इसे भी विशेषाधिकार का हनन माना जा सकता है।
◾ इसके अलावा प्रेस सदन के किसी गुप्त बैठक को भी प्रकाशित नहीं कर सकता है तब तक, जब तक सदन द्वारा उसे अगोपनीय (non confidential) करार नहीं दिया जाता है।
विशेषाधिकार भंग करने या अवमानना के लिए दंड की व्यवस्था (Punishment for breach of privilege or contempt of parliament):
जैसा कि अब तक हमने समझा अपने-अपने विशेषाधिकारों का रक्षक संसद के सदन स्वयं होते हैं। ऐसे में अगर सदन को कभी ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति ने उसके विशेषाधिकारों का हनन किया है या अवमानना किया है तो सदन उसे दंड भी दे सकता है।
◾ अगर विशेषाधिकारों का हनन करने वाला स्वयं सदन का सदस्य हो तो उसे या तो सदन की सेवा से निलंबित (Suspend) किया जा सकता है या फिर सेवा से निष्कासित (Expelled) किया जा सकता है।
◾ वहीं अगर विशेषाधिकारों का हनन करने वाला सदन का सदस्य न हो तो दंड के रूप में सदन द्वारा उसकी भर्त्सना (Condemn) की जा सकती है या फिर निर्धारित अवधि के लिए कारावास की सजा दी जा सकती है।
यहाँ यह याद रखिए कि यदि किसी व्यक्ति को कारावास की सजा दी जाती है तो कारावास की अवधि अधिवेशन की अवधि से अधिक नहीं हो सकता है। यानि कि सदन का जैसे कि सत्रावसान (Prorogation) होगा वैसे ही बंदी को रिहा कर दिया जाएगा।
◾ सदन की दंड देने की यह जो शक्ति है उसका क्षेत्राधिकार सदन के बाहर तक होता है। यानि कि यह सदन अपने सदस्यों को तो दंडित कर ही सकता है साथ ही ऐसे व्यक्तियों को भी दंडित कर सकता है तो जो कि सदन का सदस्य नहीं है।
◾ और दूसरी बात ये कि सदन को इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता है कि अवमानना सदन के परिसर के भीतर किया गया है कि परिसर के बाहर।
◾ जुर्माना लगाना – यदि सदन के दृष्टिकोण से किया गया उल्लंघन या अवमानना आर्थिक दुष्कर्म का है और उस उल्लंघन से कोई आर्थिक लाभ हुआ है, तो संसद उस व्यक्ति पर जुर्माना लगा सकती है।
सदन का विशेषाधिकार हनन करने या उसकी अवमानना के आधार पर किन्ही व्यक्तियों को दंड देने की सदन की इसी शक्ति को संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privilege) की नींव मानी जाती है।
उत्तर प्रदेश के विधान सभा द्वारा विशेषाधिकार हनन पर दंड देने का ताजा मामला

उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 3 मार्च 2023 को एक सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी और पांच पुलिसकर्मियों को विशेषाधिकार हनन के लिए दंडित किया। दंड के रूप में एक दिन की कैद की सजा सुनाई गई।
इसके लिए विधानसभा को अनुच्छेद 194(3) के तहत एक न्यायालय में बदल दिया गया। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के मुताबिक, यूपी विधानसभा के इतिहास में यह दूसरा उदाहरण है, जहां उसने अदालत के तौर पर काम किया और सजा का आदेश दिया. इससे पहले ऐसी घटना साल 1964 में हुई थी।
इसके लिए हमें अनुच्छेद 194 देखना होगा। क्योंकि जो विशेषाधिकार से संबन्धित अधिकार संसद को अनुच्छेद 105 के तहत मिलता है वही अधिकार राज्य विधान मंडल को अनुच्छेद 194 के तहत मिलता है।
अनुच्छेद 194, राज्यों के विधान मण्डल और उसके सदस्यों की शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार के बारे में है।
- अनुच्छेद 194(1) के तहत यह बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के विधानमंडल में फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा।
- अनुच्छेद 194(2) में पहले वाले को ही और विस्तारित करके बताया गया है कि राज्य विधानमंडल में विधायकों द्वारा कही गई किसी बात को लेकर उस विधायक के विरुद्ध किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
तो ये जो दो बातें है वो संविधान में लिख दिया गया है लेकिन इसके अलावा अन्य बातों के लिए क्या नियम होंगे इसके लिए अनुच्छेद 194(3) में बताया गया है कि विधान-मंडल के किसी सदन के सदस्य और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ ऐसी होंगी जो वह विधान-मंडल, समय-समय पर, विधि द्वारा परिनिश्चित करें।
यानि कि विधानमंडल के किसी समिति की शक्तियों एवं विशेषाधिकार को स्वयं विधानमंडल तय कर सकता है। और अनुच्छेद के इसी प्रावधान का इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश के विधानमंडल को एक न्यायालय में बदल दिया गया।
पूरी घटनाक्रम
दरअसल हुआ ये था कि 15 सितंबर 2004 को तत्कालीन विधायक और अब एमएलसी सलिल विश्नोई ने कानपुर में बिजली आपूर्ति को लेकर धरना-प्रदर्शन किया था.
जब विश्नोई एक जुलूस में जिलाधिकारी को ज्ञापन देने जा रहे थे तो पुलिस द्वारा उनका अपमान किया गया, गाली दी गई और लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज में विश्नोई के दाहिने पैर में फ्रैक्चर हो गया।
चूंकि विश्नोई का विरोध शांतिपूर्ण था और साथ ही वह विधायक (MLA) भी था। तथा उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए उसे पीटा जाए इसीलिए इस घटना को सदन का विशेषाधिकार भंग होना समझा गया।
चूंकि इसे एक गंभीर किस्म का मामला समझा गया इसीलिए सदन ने खुद इसपर निर्णय लेने के बजाय एक विशेषाधिकार समिति का गठन कर दिया।
28 जुलाई 2005 को सदन की विशेषाधिकार समिति ने सभी पुलिसकर्मियों को दोषी पाया और उन्होंने सिफारिश की कि उन्हें दंडित किया जाना चाहिए।
इस संबंध में महाधिवक्ता (Advocate General) से भी सलाह ली गई जिन्होंने सिफारिश की कि दोषियों को जेल भेजा जाना चाहिए।
उन्होंने प्रस्ताव दिया कि संविधान के अनुच्छेद 194 के तहत राज्य विधानमंडल को दोषियों को दंडित करने का अधिकार है और सदन को अदालत में बदलने का प्रस्ताव रखा जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।
विशेषाधिकार समिति ने 27 फरवरी 2023 को हुई अपनी बैठक में भी दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की थी और उसी के अनुरूप सदन की कार्यवाही को अदालत में बदला गया और पांचों व्यक्तियों को 1 दिन के लिए कैद की सजा सुनाई गई।
ये अपने आप में एक दिलचस्प घटना बन गई क्योंकि विधानमंडल एक न्यायालय में परिवर्तित हो गया था। द हिन्दू के अनुसार विधान सभा में ऐसी ही कवायद मार्च 1989 में हुई थी, जब राज्य के तराई विकास जनजाति निगम के एक अधिकारी शंकर दत्त ओझा को एक विधायक के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में विधान सभा में बुलाया गया था।
Facts Related to Parliamentary Privilege
- संसद के सदस्यों को केवल उसी समय और उसी सीमा तक विशेषाधिकार उपलब्ध है जिस समय और सीमा तक वे संसद के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। इसके अलावा संसद का सदस्य भी सभी नागरिकों की तरह ही कानून की नजरों में बराबर होते हैं।
- संसद के सदस्यों के लिए विशेषाधिकार तभी उपलब्ध होता है जब वह संसदीय सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो और तब किसी ने उसके काम में बाधा पहुंचायी हो या उस पर आक्रमण किया हो।
- यदि किसी सदस्य द्वारा सदन में दिये गए किसी भाषण से न्यायालय की अवमानना होती हो फिर भी किसी न्यायालय में उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।
- अनुच्छेद 122 के तहत संसद की कार्यवाहियों की न्यायालयों द्वारा जांच नहीं की जा सकती है।
- अनुच्छेद 121 के तहत उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण पर सदन में तभी चर्चा की जा सकती है जब उस पर महाभियोग (Impeachment) चल रहा हो।
- अध्यक्ष या सभापति की अनुमति के बिना संसद भवन के अंदर किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
- धारा 144 भी संसद के परिसरों में लागू नहीं की जा सकती। यदि सक्षम प्राधिकारी ऐसा करने की सोचें तो वह विशेषाधिकार हनन का मुद्दा बन सकता है।
समापन टिप्पणी (Closing Remarks):
संसदीय विशेषाधिकार भारत की संसदीय प्रणाली का एक अनिवार्य घटक है। यह सुनिश्चित करता है कि संसद के सदस्य प्रतिशोध या बाहरी प्रभाव के डर के बिना अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं, जिससे एक संस्था के रूप में संसद की स्वतंत्रता और अखंडता को बढ़ावा मिलता है।
एक संस्था के रूप में संसद की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखने के लिए संसदीय विशेषाधिकार की अवधारणा आवश्यक है। यह संसद के सदस्यों को बिना किसी कानूनी कार्रवाई या दायित्व के किसी भी मुद्दे के बारे में स्वतंत्र रूप से और खुले तौर पर बोलने की अनुमति देता है।
हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये विशेषाधिकार पूर्ण नहीं हैं और दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ सीमाओं और प्रतिबंधों के अधीन हैं। संसद के सदस्यों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को संतुलित करके, संसदीय विशेषाधिकार भारत में लोकतंत्र और कानून के शासन को बनाए रखने में मदद करता है।
उदाहरण के लिए, संसद का कोई सदस्य संसदीय विशेषाधिकार का उपयोग किसी को बदनाम करने या गोपनीय जानकारी का खुलासा करने के लिए नहीं कर सकता है। संविधान किसी भी सदस्य की सजा का भी प्रावधान करता है जो अपने विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करता है या दूसरों के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है।
कुल मिलाकर, भारत में संसदीय विशेषाधिकार संसद के सदस्यों को दिए गए विशेष अधिकारों और उन्मुक्तियों को संदर्भित करता है, जो उन्हें किसी भी तरह के प्रभाव या हस्तक्षेप के डर के बिना अपने कार्यों और कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम बनाता है।
तो ये रहा संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary privilege) और उससे संबंधित कुछ मुख्य बातें। संसद से संबंधित अन्य लेख नीचे दिये जा रहें है, उसे भी अवश्य पढ़ें।
Parliamentary Privilege Practice Quiz
Read Related Articles Also
मूल संविधान
हमारी संसद – सुभाष कश्यप
डी डी बसु की व्याख्या
https://www.thehindu.com/news/national/other-states/uttar-pradesh-vidhan-sabha-punishes-six-policemen-for-one-day-custody-in-2004-case/article66578165.ece
https://economictimes.indiatimes.com/news/india/uttar-pradesh-assembly-converted-into-a-court-and-then-a-jail-for-six-cops-for-a-day/articleshow/98398112.cms
एम लक्ष्मीकान्त – भारत की राजव्यवस्था
Polity pramod agrawal
https://mpa.gov.in/sites/default/files/Manual2018_0_0.pdf
https://blog.ipleaders.in/parliamentary-priviledges/#Freedom_of_Speech


![भारत पर आज़ादी पूर्व के घटनाओं का प्रभाव [यूपीएससी]](https://wonderhindi.com/wp-content/uploads/2022/12/artistic-vintage-world-map-draw-concept_52683-26378-440x264.webp)

![केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध [Concept] #UPSC](https://wonderhindi.com/wp-content/uploads/2020/07/Center-State-Financial-Relations1.jpg)